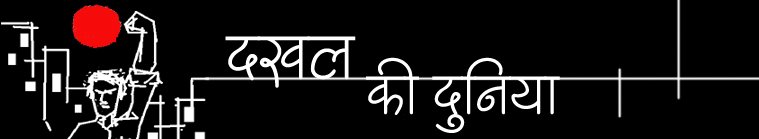मधेपुरा से सिंहेश्र्वर की ओर जानेवाली सडक पर पथराहा गांव में मिलते हैं जोगेंदर यादव। सडक किनारे एक पान की दुकान के सामने मचान पर बैठे वे पानी को अपनी 'खर छपरी' में घुसते हुए देखते हैं। पानी ने सुबह ही पथराहा में प्रवेश किया है। कोसी का लाल पानी. कल दोपहर में गांववालों ने उसकी रेख देखी थी, गांव के पूरब. आज वह उनके घरों से, आंगन से, बांस-फूस की दीवारों से होता हुआ बह रहा है. कौवे उसकी फेन में जाने क्या ढूंढ रहे हैं. कुत्ते उसे सूंघते हैं और भडक कर भागते हैं. गोरू उसमें खुर रोपने से डरते हैं. एक-एक सीढी डुबोते हुए, एक-एक घर पार करते हुए, एक-एक गली से राह बनाते हुए सडक पर आकर वह अपनी थूथन पटकता है. कहीं-कहीं कमर भर पानी है गांव में. ७० साल के बूढे जोगेंदर ने सामान तो मचान पर चढा दिया है, लेकिन गेहूं-मकई नहीं चढा पाये. अकेले हैं. दोनों बेटे बहुओं-बच्चों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाने गये हैं. खैनी ठोंकते हुए वे हंसते हैं- उदास हंसी-यही तेजी रही तो कल तक सडक पार कर जायेगा पानी. ६५-७० साल की जिदंगी में पहली बार देखा है अपने घर में पानी भरते हुए. घर गया. अनाज गया. उनके खेत उन्हें खाने लायक अनाज दे देते हैं- गेहूं, धान, मकई. इस बार सब खत्म. खेत में खडी धान की फसल को बाढ लील गयी, घर में रखा अनाज पानी में डूब गया.
... लोग जुट आये हैं. वे सुनाते हैं- सौ साल पहले यहां कोसी बहती थी. अब लगता है, वह फिर लौट आयी है. बेचन यादव, कारी, तेजनारायण, रामदेव, संजय व शैलेंद्र ... दर्जनों लोग, सबके पास कई-कई कहानियां. किसी के आंगन में पोरसा भर पानी है, तो किसी के घर में सांप घुस आया है. अभी लेकिन सब शांत हैं-चिंता की एक रेख तक नहीं है. कहते हैं अभी सडक तो है ही सोने के लिए. ज्यादा डूबने लगेगा तो प्लान करेंगे निकलने का.
...लेकिन बूढे जोगेंदर को यह भी चिंता नहीं. वे अपनी खैनी होठों के नीचे दाब चुके हैं-'हम अकेले आदमी, मर जायेंगे तो क्या होगा ङ्क्ष सांप भी कांट लेगा, तो क्या होगा ङ्क्ष
१० साल के कुंदन का घर सडक की दूसरी ओर है- सूखे में. वह आधे गांव को डूबते हुए देखता है-अपलक. डर ङ्क्ष 'डरेंगे क्यों ङ्क्ष सब मरेगा कि हमीं मरेंगे ङ्क्ष... सब न मरतय.
लेकिन उससे दो साल छोटा मन्नू जिदंगी को उससे ज्यादा संजीदगी से लेता है-' डरना क्या है ङ्क्ष पानी बढेगा तो जहां सब जायेंगे, वहीं हम भी जायेंगे.'
पानी बढ रहा है. अपने गांव, घर, चूल्हे, खिडकी-दरवाजों को इंच-इंच डूबते हुए देखना-एक त्रासदी है. पानी अपने एक नये रूप में मिल रहा है - इनमें से अनेक पीढियों को. वे अपने तरीकों से इसकी तैयारी में जुटे हैं.
जोगेंदर की निर्लिप्तता, कुंदन की सहजता और मन्नू की जीवटता-सुनने लायक चीजें हैं, लेकिन उन्हें सुनने को कोई तैयार नहीं... लगभग एक सदी बाढ लौटी कोसी भी नहीं.
... पानी बढ रहा है.
***
सिंहेश्र्वर मंदिर धर्मशाला से निकलती दलित औरतों के मुंह से कुछ अस्फुट से बोल फूटते हैं-सगरे समैया हे कोसी माई, सावन-भादो दहेला... पूजा गीत. औरतों के चेहरों पर उदासी मिश्रित भय है... हर मंगल को दीप जलाने-संझा दिखाने के बाद भी नहीं मानीं कोसी माई.
...परसा, हरिराहा, कवियाही, रामपुर लाही... शंकरपुर व कुमारखंड प्रखंडों के दर्जनों जलमग्न गांवों से उजडे हजारों लोग पिछले चार दिनों से धर्मशाला में डेरा डाले हुए हैं. यहां रहने के लिए पक्के कमरे हैं. मूढी, चूडा, चीनी, खिचडी व बिस्कुट सबका इंतजाम है. बच्चे चूडा-गुुड पाकर खुश हैं...बेवजह शोर मचा रहे हैं. बूढे-बुजुर्ग माथे पर जोर देकर याद करने की कोशिश करते हैं कोई पुरानी बात... बाप-दादों की स्मृतियों को भी खंगाल रहे हैं-'उंहू . ऐसी बाढ मेरे देखे में तो कभी नहीं आयी. बाप-दादे भी कुछ नहीं बता गये. ३० साल पहले पानी भरा था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ कि पाट की पूरी फसल डूब जाये फुनगी तक.'
...ऐसा नहीं हुआ कभी. ६० साल के परमेसरी साह हतप्रभ हैं. जिले में बाढ ने सबसे अधिक कुमारखंड और शंकरपुर प्रखंडों में नुकसान पहुंचाया है. यदुनंदन मेहता कुमारखंड की हरिराहा पंचायत के हैं. २० अगस्त की शाम को वे अपने गांव में चौक पर घूम रहे थे कि एकाएक साइफन में देखा कि पानी बढ गया है. गांववालों को पहले से अंदेशा नहीं था. जैसे-तैसे भागे सब. २३ तारीख तक यदुनंदन लोगों को अपनी मोटरसाइकिल पर बैठा कर सिंहेश्र्वर लाते रहे. फिर रास्ता बंद हो गया. गांव के तीन हजार से ज्यादा लोग या तो वहीं फंसे हुए हैं या अन्य जगहों पर चले गये हैं. शंकरपुर प्रखंड के परसा गांववालों के लिए भी बाढ अचानक आयी.
२१ अगस्त की सुबह तीन बजे पानी गांव में घुस आया. गांव की पांच हजार आबादी में से अधिक वहीं फंसी हुई है. करीब सौ लोग निकल पाये हैं. गांव में चार फुट से ज्यादा पानी है अभी. रामचंद्र दास उदास हैं. वे अपनी दो बीघे में लगी धान की फसल, एक बीघे पाट और पांच मवेशियों को याद करते हैं-'सब बह गये. धान इस बार अच्छा लगा था. पांच किलो खाद हर कट्ठे में दिया था. सब खत्म.
जयकुमार साह के लिए भी यह कम नुकसानदेह नहीं रही. उनके १०० सदस्योंवाले परिवार की ५० भैंसें पानी में बह गयीं. अभी भी उनके मां-पिताजी गांव (परसा) में फंसे हुए हैं. उनकी चार बीघे में लगी धान की फसल भी डूब गयी.
...गांव में से इक्के-दुक्के लोग किसी तरह सुरक्षित जगहों पर अब भी पहुंच रहे हैं. नये आनेवाले ये लोग गांव की नयी खबरें भी साथ लाते हैं-प्रायः दुखद खबरें. ... हुकुम राम की मां मर गयीं-डूब कर. मचान पर थी, उसी पर से गिर गयीं. पानी का 'अदक' (आतंक) नहीं सह पायी ७० साल की बूढी. उसके घरवाले अभी मचान पर हैं. परसा में कल पानी घटने लगा था... आज फिर बढ गया.
...लोग चुप हो जाते हैं कुछ क्षण. उधर कोने में कोई सिसक उठता है... कारी कोसी जाने क्या लेकर मानेगी.
१८ किलोमीटर है सिंहेश्र्वर से परसा. कल तक सडक चालू थी, आज जिरवा पुल टूट गया-सो रास्ता बंद. लालपुर रोड पर भी भर घुटना भर पानी है. मतलब कि नाव के बिना अब गांववाले निकल नहीं सकते.
सबके घर का कोई -न -कोई गांव में फंसा हुआ है. सब उदास हैं. १२ साल का एक लडका धीरे से आकर बैठ जाता है-मिथुन कुमार दास. कहता है 'लिख लीजिए, मैं अकेले हूं यहां. मम्मी-पापा सहित सारे घरवाले गांव में हैं.' वह दो-तीन दिन पहले किसी काम से कवियाही आया था. इस बीच बाढ आ गयी और वह यहां रह गया. सभी अपना नाम लिखाना चाहते हैैंं. दीनबंधु साह आठ आदमी. रवींद्र कुमार दास-तीन आदमी. सत्यनारायण साह-पांच आदमी. परमेसरी साह-पांच आदमी. संतोष शर्मा-पांच आदमी. बेचन, शिबू, कमलेश्र्वरी ...नामों की अंतहीन सूची है. जो निकल आये हैं, वे चाहते हैं कि फंसे हुए लोग भी निकल आयें. देर हो रही है, तो वे धैर्य खोते जा रहे हैं. चूडा-गुुड मिल रहा है तो क्या, जब परिवार ही साथ नहीं तो...
परिवारों को फिर से साथ आने में समय लगेगा. उजडे घरों को फिर से बसने में भी और पानी को उतरने में भी.
...वह तो अभी बढ ही रहा है.
कटैया बाजार पर पंडा नगर से भैंसे हांक कर ला रहे किसानों ने बताया-वीरपुर बाजार में कमर भर पानी है. भीमनगर बाजार में सरकारी राहत शिविर के सामने आधे घंटे से रोटियों के लिए खडे विकास कुमार राम ने आग्रह करते हुए लिखाया-'वीरपुर के कुमार चौक में ५० आदमी फंसे हुए हैं.' विकास आज ही वीरपुर से निकला है किसी तरह.
कोसी ने लगभग पूरी तरह लील लिया है वीरपुर को. क्या बचा है वहां अब. जो दशा है वहां की ... एक-एक कर नयी सूचनाएं मिल रही हैं वीरपुर से-मानो एक अंधकार से परदा उठ रहा हो.
वीरपुर से कुसहा की दूरी महज छह किलोमीटर है और सोमवार को बांध टूटने के बाद भारत में पहला बडा आघात वीरपुर को झेलना पडा.
सोमवार की सुबह से ही वीरपुर बाजार में अफवाहें थीं कि बांध को खतरा है, लेकिन अधिकारिक तौर पर कोई सूचना नहीं थी. इससे लोगों ने निकलने की तैयारी भी नहीं की. बूढ-पुरनियों ने इन अफवाहों को चुटकी में उडा दिया-पानी तो आता ही रहता है. इस बार भी आया है, तो पहले की तरह ही निकल जायेगा. ...खतरे की गंभीरता का अंदेशा किसी को नहीं था.
लेकिन शाम साढे छह बजे पानी शहर में घुसा और घंटे भर में पूरा शहर तीन से चार फुट पानी से भर गया. किसी को निकलने का मौका नहीं मिला. पूरा हफ्ता निकल जाने पर भी वीरपुर में आधा से अधिक लोग फंसे हुए हैं. राहत अब कुछ जाने भी लगी है, तो वह सिर्फ वीरपुर तक सीमित है. आसपास के गांव अब भी अछूते हैं. भीमनगर में मिले परमानंदपुर के एक निवासी ने बताया कि उधर अब तक कोई पहुंचा ही नहीं. रानीपट्टी से आ रहे रंजीत पासवान ने सूचना दी-सारे आदमी फंसे हुए हैं गांव में. बसमतिया रोड पर ३०-४० फुट जगह बची है. उसी पर डेढ-दो हजार आदमी रह रहे हैं. खाने-पीने का कोई सामान नहीं. दो-तीन आदमी मर भी गये हैं. कटैया से वीरपुर आठ किलोमीटर है और भीमनगर से पांच. अब नावें वीरपुर तक पहुंचने लगी हैं, लेकिन वे बहुत महंगी हैं. एक नाव एक बार वीरपुर जाने के लिए पांच से छह हजार रुपये लेती है. उसमें भी पानी की धार देखते हुए इन छोटी नांवों से वहां जाना जोखिम भरा है.
कटैया में एक चाय दुकान पर मिलते हैं, दिलीप कुमार गुप्ता. उनके पास वीरपुर से आज सुबह तक की सूचनाएं हैं-अब भी हरेक कॉलोनी में सात फुट पानी है. वीरपुर कोसी पुल के हॉस्टल की छत पर तीन सौ आदमी हैं. फतेहपुर स्कूल पर ५०-६० आदमी हैं. कहीं कोई मदद नहीं मिल पायी है .
वे सुनाते हैं-पूरा गांव भंस गया है फतेपुर का. वीरपुर बाजार में अरबों की संपत्ति का नुकसान है. क्वार्टरों में चोरियां बढ गयी हैं. जो नाववाला दिन में वीरपुर से कटैया पहुंचाता है, वही रात में जा कर खाली घरों पर हाथ साफ करता है. तीन महला मकान गिर रहे हैं. दिलीप कटैया में वीरपुरवालों को सूचना देते हैं चिल्ला कर : चानो मिस्त्री, रमेश कुमार, अख्तर बैंड, दुक्खी बैंड, मनोज पाठक के मकान टूट गये हैं.
कुछ दूसरी सूचनाएं भी मिली हैं- वीरपुर जेल में ८७ कैदी थे. असुरक्षित. चार दिनों से उनका खाना बंद था. जेल के कर्मचारी भाग चुके थे. अंत में कैदियों ने धोतियां-चादरें जोडीं और भाग गये. उनमें से कितने बचे-कितने डूब गये, अभी कौन बता सकता हैङ्क्ष सिविल कोर्ट, अनुमंडल ऑफिस के हजारों रेकॉर्ड पानी में खत्म. धान और पाट की खेती डूब गयी. बीसियों हजार लोग बरबाद हो गये.
भीमनगर से कटैया आनेवाली सडक राहगीरों से भरी है. उजडे-बरबाद हुए परिवार छोटे ठेलों पर, कंधे पर सामान लिये जानवर हांकते आ रहे हैं. थके-हारे चेहरे-उदास आंखें. लोग हंसना भूल गये हैं. गलती से कोई बाहरी आदमी हंस दे, तो लोग चौंक उठते हैं. जानवर तक डकरना भूल गये हैं. बूढी, कमर झुकी औरतें भी, बच्चे भी गठरियां उठाये तेजी से चल रहे हैं. कहां पहुुंचना है, पता नहीं. कोसी ने उन्हें कहीं का नहीं छोडा.
... सडक के किनारे बाढ का पानी तेजी से थांप मारता है. कभी-कभी कोई गाडी भीड के बीच से गुजर जाती है सीटी बजाती हुई... एक औरत रास्ते की दूसरी ओर अपने किसी परिचित से कह रही है-वीरपुर तो अब सपना हो गया.
... कुछ बातें ऐसी होती हैं, जिन्हें भुलाया नहीं जा सकता.
***
हफ्ते भर से वीरपुर में फंसे लोग अब निकलने लगे हैंं-लेकिन उनमें से भी वही लोग निकल पा रहे हैं, जो नाव के लिए दो से छह हजार रुपये खर्च कर पाने में सक्षम हैं.
स्वीटी फ्रांसिस उनमें से एक हैं, जो अपनी मां, दादी और बहनों के साथ मंगलवार को वीरपुर को पीछे छोड आयीं. बाहर निकल आने की आश्वस्ति उनके चेहरे पर है, लेकिन अब भी वीरपुर में उनके दो भाइयों समेत पांच परिजन फंसे हुए हैं. ये सात दिन स्वीटी के लिए किसी यातना से कम नहीं रहे. वह याद करती है-नमक तक कोई नहीं दे रहा है. एयरड्रॉपिंग का कोई खास फायदा नहीं है. पैकेट पानी में गिर जाते हैं.
वीरपुर में राशन और दवाइयों की कुछ दुकानें खुली हुई हैं, लेकिन राशन दोगुने-तिगुने दाम पर मिल रहा है. इसके अलावा उसे बनाने का संकट भी है. स्वीटी बताती है कि उसके वार्ड नंबर चार के वार्ड मेंबर की गोल चौक पर सरकारी राशन की दुकान है. उन्होंने कुछ भी देने से मना कर दिया. चावल ३० से ४० रुपये किलो तक बिक रहा है. चूडा सौ रुपये तक.
स्वीटी को याद है, सोमवार की सुबह से ही ऐसी अपुष्ट खबरें आने के बाद कि बांध टूटनेवाला है, बाजार में चीजों के दाम बढ गये थे. सोमवार के दिन मूढी ४० रुपये किलो तक बिकी. दिन में दो बजे के करीब कुछ युवकों ने खबर दी कि बांध टूट गया. लेकिन तब भी लोगों को यकीन था कि सरकारी तौर पर कोई सूचना जरूर मिलेगी. उन्होंने अफवाहों को बहुत गंभीरता से नहीं लिया. उधर मधुबन जंगल में पानी भरने लगा था. शाम को राजमार्ग तोड दिया गया और इसके बाद वीरपुर में पानी भर गया.
फ्रांसिस परिवार ने जैसे-तैसे खाने का कुछ सामान बचाया और छत की शरण ली. लेकिन शहर की सारी आबादी को छतें उपलब्ध नहीं थीं, जहां वह शरण ले सकती. गरीबों के बांस-फूस के झोंपडे थे. वे डूबे भी-बहे भी. कइयों ने दूसरों की छतों पर शरण ली.
पहले तो वीरपुर के निवासियों ने सोचा कि पानी दो-तीन दिनों में निकल जायेगा, जैसा कि पहले भी हो चुका था. लेकिन उनकी उम्मीदें सही साबित नहीं हुईं. वीरपुर और टूटे हुए कुसहा बांध के बीच में पडते हैं नेपाल के गांव-लाही, हरिपुर, शिवगंज और दूधगंज. उन गांवों में तो अब घर भी नहीं दिखते. सिर्फ पेड खडे दिख रहे हैं. वीरपुर के अलावा भवानीपुर, सीतापुर, हृदयनगर और प्रखंड मुख्यालय बसंतपुर भी पूरी तरह तबाह हो चुके हैं.
बाढ से घिरे इलाकों में भूख से मौतें शुरू हो चुकी हैं. फ्रांसिस परिवार ही नहीं, वीरपुर से निकले कई अन्य लोगों ने भी सूचना दी-परमानंदपुर मदरसा में फंसे १२ लडके भूख से मर गये २३ अगस्त को. २५ को बसमतिया में २० लोग डूब गये हैं....आठ साल का एक बच्चा एयरड्रॉपिंग का पैकेट लपकने में छत से गिर कर मर गया. वीरपुर अस्पताल के प्रभारी डॉक्टर वीरेंद्र प्रसाद की इलाज के अभाव में शनिवार को मौत हो गयी.
...नक्शा फैला कर देखिए-पश्चिम में भीमनगर से पूरब बसमतिया तक का पूरा इलाका कोसी में समा चुका है. लोग जिंदा तो हैं, लेकिन हर पल जीवन उनसे दूर होता जा रहा है.
...मुसलिम टोले में २०० लोग फंसे हुए हैं. सेंट्रल बैंक कॉलोनी (वार्ड चार) में सौ से अधिक लोग फंसे हुए हैं. वीरपुर से दो किमी पूरब पटेरवा में दो हजार लोग फंसे हुए हैं. उनमें बच्चे हैं, महिलाएं हैं, बूढे हैं.
...और ऐसे में वीरपुर लहरी टोल की ज्योति पराया ने २० तारीख को एक बच्चे को जन्म दिया. चारों ओर से पानी से घिरे एक काठ के घर की छत पर शरण ली हुईं चार बहनों को भाई मिला...लेकिन वह बचेगा कैसेङ्क्ष मकान धंसा तो क्या होगाङ्क्ष कौन जानता है कि मकान धंस नहीं गया होगाङ्क्ष रोज ही शहर (!) में घर गिर रहे हैं. छतें टूट रही हैं. दीवारें धंस रही हैं.
स्वीटी को इन सात दिनों में अपने पापा की बहुत याद आयी. सिंचाई विभाग में इंजीनियर रहे और कुसहा बांध के इंच-इंच से परिचित स्वीटी के पापा कहते थे-कुसहा बांध टूटे तो कभी वीरपुर में मत रहना. कोसी इसे बरबाद कर देगी.
पापा के निधन के कई वर्षों बाद स्वीटी पाती है कि उसके पापा कितने सही थे.
***
कटैया जैसे छोटे बाजार के लिए इतनी भीड बहुत अनहोनी बात है. साल में सिर्फ विश्वकर्मा पूजा के मेले में ऐसी भीड जमा होती है. लेकिन वह तो मेला होता है. बिहार स्टेट हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर कारपोरेशन में कार्यरत राकेश कुमार इसके लिए एक दूसरा नाम सुझाते हैं : आफत मेला.
वास्तव में यह आफत मेला है. कटैया हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर प्लांट से दक्षिण से लेकर भंटाबाडी (नेपाल) तक चले जाइए-अस्थायी तंबुओं (इन्हें अगर आप तंबू कह सकते हों) में रह रही हजारों की आबादी आफत में फंसी हुई है. कटैया की हर इंच पर उजडे परिवार बसे हुए हैं. हर तरफ, बांस-फूस से बनी दुकानों से बची खाली जगह से लेकर मंदिर परिसर, धर्मशाला और दूसरी सभी जगहों पर विस्थापितों के तंबू गिरे हुए हैं-छोटे से घेरे में घर का बचा-खुचा सामान और बहने से बच गये लोग. वीरपुर, बैजनाथपुर, लालपुर खंटाहा, भवानीपुर, बलुआ, भारदह से आये हुए लोग अपने जानवरों के साथ बोरे और चादरें आदि टांग कर रह रहे हैं. हर समय कुछ नये परिवार आ रहे हैं और खाली जगहों पर कुछ नये तंबूनुमा डेरे खडे हो जाते हैं. राज्य के आपदा प्रबंधन मंत्री नीतीश मिश्रा बलुआ के निवासी हैं. बलुआ से आये लोग बताते हैं कि वहां न कोई नाव है, न राहत. बलुआ हाइ स्कूल पर २०० लोगों ने शरण ली थी. शुक्रवार २२ अगस्त को छत गिर गयी. उनमें से कम ही होंगे, जो बच पाये होंगे.
लेकिन जो जीवित हैं, वे भी हताश हो रहे हैं. एक टेंट में सूखा चूडा फांक रहे उपेंद्र प्रसाद कहते हैं-'और दो चार दिन कुछ नहीं मिला तो लोग भूखे मर जायेंगे. अभी तो जिंदा देख रहे हैं न, चार दिन बाद लाश देखियेगा लोगों की.'
भीमनगर के पुराना बाजार चौराहे पर बाढ राहत शिविर में कुछ लोग जमा हो गये हैं-दवा काउंटर के पास. शिविर में बैठा एक नेतानुमा व्यक्ति स्थानीय लोगों और अधिकारियों को बता रहा है-'मेरा तो एक बयान ऐसा आया है कि उसे हिंदुस्तान टाइम्स तक को छापना पडा है.'...ऐसी आफत में भी इतना हृदयहीन हो सकता है कोईङ्क्ष
हाथ में नोटबुक देख कर पास ही में बैठे पुलिस के एक अधिकारी ने अखबारों पर टिप्पणी की-'कुछ छाप नहीं रहे हो तुमलोग जी. जनता मर रही है यहां.' लेकिन वहीं बैठे बाढ राहत के एक प्रभारी अधिकारी कोई रिस्क लेना नहीं चाहते. उतने बोल्ड नहीं हैं. राहत कार्यों के बारे में पूछने भर से वे खडे हो जाते हैं-'जो पूछना है, डीएम से पूछिए जाकर. हमारी नौकरी मत लीजिए भाई.'
सडक की दूसरी ओर एक चाय दुकान पर चाय 'सर्व' करनेवाला बच्चा पानी का गिलास रखते हुए लगभग इशारे में बताता है-'यहां लोग पांच दिन बिना खाये रहा है. तीन दिन से पूडी बन रहा है, तब जिंदा देख रहे हैं इनको.' वह अपने दोनों हाथों की अंगुलियां फैलाता है-दस हजार लोग मरा है.
शिविर के सामने पंक्तियों में बैठे कुछ बच्चे और महिलाएं भोजन का पौन घंटे तक इंतजार करने के बाद उठने लगे हैं. हालांकि इस पूरी अवधि में तेजी से पूडियां तली जाती रही हैं. वे बंटेंगी, लेकिन कब, पता नहीं.
उन्हीं के बीच से गुजरती हुई, अपने मल्लाह पति को खाना ले जाती हुई और बाढ के प्रकोप से बची हुई एक नेपाली महिला कोसी को गोहारती है, अपनी भाषा में :
कौने नइया डूबेइगो कोसी माई
कौने नइया उगइबो कोसी माई,
मईया गो उतरइबी पार...
पापे नइया डूबेइगो कोसी माई,
धरमे नइया उगइबो कोसी माई,
मईया गो उतरइबी पार...