-दिलीप ख़ान
[ये लेख हंस के सोशल मीडिया विशेषांक के लिए नवंबर
2017 में लिखा गया था। यहां हम उसी लेख को हूबहू प्रकाशित कर रहे हैं। लिहाजा ‘इस साल’ का मतलब 2017 और ‘बीते साल’ का मतलब 2016 समझा जाए। इस लेख के बाद कम से कम दो बेहद
महत्वपूर्ण घटनाक्रम हुए, जिनकी चर्चा इसमें नहीं की गई है। ये दोनों घटनाएं हैं- कैम्ब्रिज
एनालिटिका और भारत में सोशल मीडिया पर
क़ानून का प्रस्ताव।- लेखक]
“फ़र्जी
मुख्यधारा का मीडिया शिद्दत से मेहनत कर रहा है कि मैं सोशल मीडिया से दूर रहूं।
उसे इस बात से तकलीफ़ है कि मैं यहां ईमानदारी से अनफिल्टर्ड संदेश आप तक पहुंचा
सकता हूं।”-
डोनल्ड ट्रंप, राष्ट्रपति, अमेरिका[i]
दुनिया के सबसे ताक़तवर मुल्क के राष्ट्रपति का
वहां के कुछ मीडिया समूहों के साथ तकरार महीनों से जारी है। वो अपनी तरफ़ उठने
वाले हर सवाल को इस तरह चुनौती देते हैं कि समूचे मीडिया की विश्वसनीयता उन
मुद्दों पर सवालों के घेरे में आ जाती है, जो सत्ता को असहज करने वाले हों। अमेरिका में
राष्ट्रपति चुनाव के दौरान से ही डोनल्ड
ट्रंप और मीडिया
के बीच
बयानों का सिलसिला लगातार निचले स्तर तक पहुंचता गया। समय-समय
पर ट्रंप की तरफ़
से टीवी चैनलों
और अख़बारों को धमकाया भी गया। इसमें
सोशल मीडिया के ज़रिए लोगों तक उनकी
पहुंच का भाव
इस तरह गुंथा
रहता है, जैसे
डोनल्ड ट्रंप स्थापित
टीवी चैनलों और अख़बारों को ट्वीटर और फेसबुक के ज़रिए चुनौती
दे रहे हों।
 |
| डोनल्ड ट्रंप और अमेरिकी मीडिया के बीच तल्ख़ रिश्ते रहते हैं |
इसके
दर्जनों उदाहरण डोनल्ड
ट्रंप के ट्वीटर
हैंडल पर देखने
को मिल जाएंगे।
फ़र्जी, बेईमान, देशविरोधी
ये तीन ऐसे
शब्द हैं जो डोनल्ड ट्रंप मीडिया
के साथ इस तरह
इस्तेमाल करते हैं
जैसे मीडिया को श्रेणीबद्ध करने में लोग
प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक या सोशल
मीडिया का ज़िक्र
करते हों। ट्रंप
ने इन तमाम
वर्गीकरण को अपने
तरीके से फर्जी,
बेईमान और देशविरोधी
नाम के एक तंबू
में बंद कर दिया
है।[iii]
अगर
ट्रंप के ट्वीटर
आर्काइव का विश्लेषण
किया जाए तो उनके
हर 10 में से एक
ट्वीट में मीडिया,
फेक न्यूज़, एमएसएम
(यानी मेनस्ट्रीम मीडिया),
फेक मीडिया और मेनस्ट्रीम मीडिया नामक
शब्द जरूर होता
है।[iv] डोनल्ड
ट्रंप ने मीडिया
और पत्रकारों को लेकर
जो चर्चित बयान
दिया है, उनमें
दो-तीन बेहद
दिलचस्प है। उन्होंने
कहा-
1.
प्रेस
अमेरिका से ज़रा भी प्यार नहीं करता
2.
पत्रकार
सबसे बेईमान लोग होते हैं
3.
मीडिया
अमेरिकी लोगों का दुश्मन है।[v]
अंतरराष्ट्रीय सूचना प्रवाह
में अमेरिका और मीडिया के तालमेल की पड़ताल करने पर एकबारगी
ये सारे बयान
इस आधार पर अविश्वसनीय नज़र आते हैं
कि पश्चिमी मीडिया
दशकों से अमेरिकी
सत्ता के प्रचारक
की भूमिका में
दुनिया भर में
नज़र आया है।
अमेरिका के विदेश मंत्री
जॉन फोस्टर ड्यूल्स
ने शीत यु्द्ध
के दौरान कहा
था कि अगर
अमेरिकी विदेश नीति
में सिर्फ़ और सिर्फ़ एक चीज़ चुनने
का विकल्प हो तो
वो मुक्त सूचना
प्रवाह को चुनेंगे।
वजह साफ़ थी कि
उस वक़्त का ‘मुक्त
सूचना प्रवाह’ अमेरिकी
मीडिया के कंधे
पर सवार होकर
अमेरिकी साम्राज्यवादी नीति
का सबसे ‘शांतिपूर्ण’ वाहक
था। अमेरिका ने न
सिर्फ़ टीवी और प्रिंट मीडिया बल्कि
हॉलीवुड की फ़िल्मों
के ज़रिए भी वियतनाम समेत कई मुल्कों
पर अपने हमले
को न्यायसंगत बताने
का काम किया।[vi]
फिर, डोनल्ड ट्रंप
की ताज़ा नाराजगी
की वजह क्या
है? क्या
उन्हें अपनी बात मीडिया के ज़रिए बड़ी आबादी तक पहुंचाने में रुचि नहीं है? क्या कुछ मीडिया समूह डोनल्ड ट्रंप और उनकी नीतियों का आलोचक है
इसलिए ट्रंप मीडिया की विश्वसनीयता को गिराकर अपनी आलोचनाओं को इस आधार पर निरस्त
कर देना चाहते है? या फिर डोनल्ड ट्रंप ये जानते
हैं कि जिसे मुख्यधारा का मीडिया कहा जाता है, उसकी बजाए वो निजी प्लेटफॉर्म से उन
लोगों के बीच ज़्यादा सटीक और सीधी सूचना पहुंचा सकते हैं जिन्हें दुनिया सोशल
मीडिया के नाम से जानती है।
डोनल्ड ट्रंप ने इस साल फ़रवरी में एक प्रेस
ब्रीफिंग में कई मीडिया समूहों को आने की इजाज़त नहीं दी। इनमें न्यूयॉर्क टाइम्स,
सीएनएन, पोलिटिको, एनबीसी, एबीसी, फॉक्स न्यूज़ और बज़ फीड जैसे कई अख़बार और टीवी
चैनल्स शामिल थे, जो अमेरिका समेत दुनिया में चर्चित हैं और जिनपर अमेरिकी नीतियों
का वाहक होने का कई बार इल्ज़ाम लग चुका है। जब इन मीडिया समूहों को प्रेस
ब्रीफिंग से दूर किया गया तो वॉशिंगटन टाइम्स और वन अमेरिका न्यूज़ जैसे कई मीडिया
संस्थानों ने ब्रीफिंग का बहिष्कार कर दिया।[vii]
आख़िरकार ट्रंप को ये
आत्मविश्वास किस ज़मीन
से हासिल हो रहा
है कि वो अपने
मुल्क के सबसे
बड़े मीडिया संस्थानों
से खुल्लम-खुला
नारजगी मोल ले रहे
हैं और एनबीसी
का लाइसेंस रद्द
करने की धमकी
ट्वीट कर
सार्वजनिक करते हैं।[viii]
अमेरिका में
लोगों के मीडिया
चुनाव को देखें
तो बीते कई साल
से ये रुझान
साफ तौर पर दिख
रहा है कि वहां
अख़बारों का सर्कुलेशन
घट रहा है,
केबल टीवी मीडिया
के प्रति युवाओं
का रुचि कम हो
रही है और इंटरनेट तेज़ी से लोकप्रियता के सारे आयामों
को तोड़ रहा
है।[ix]
ये चलन सिर्फ अमेरिका में नहीं है बल्कि दुनिया के
कई देशों की यही कहानी चल है। भारत जैसे मुल्कों में अख़बारों का सर्कुलेशन अभी
सकारात्मक है, टीवी देखने वालों की तादाद भी पहले के मुकाबले बढ़ी है, लेकिन इसके
पीछे अमेरिका से अलग दूसरी वजहें हैं। अगर सोशल मीडिया के प्रसार को देखें तो
प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक के मुकाबले इसके प्रसार में अभूतपूर्व वृद्धि हो रही है।[x]
जनवरी 2017 में दुनिया में 187 करोड़ लोग फेसबुक का इस्तेमाल कर रहे थे, 100-100
करोड़ लोग व्हाट्सएप और फेसबुक मैसेंजर का, जबकि 32 करोड़ लोग ट्वीटर पर सक्रिय
थे। [xi]
ये संख्या विशाल है। सोशल मीडिया पर सक्रिय लोग
टीवी और प्रिंट के इस्तेमाल करने वाले से बिल्कुल अलग मिज़ाज के होते हैं। ये
शिथिल उपभोक्ता नहीं हैं। एल्विन टॉफलर ने अपनी प्रसिद्ध किताब द थर्ड वेब में जिस
प्रोज्यूमर शब्द का इस्तेमाल किया था, उसे इंटरनेट दौर के अगले चरण में सोशल मीडिया
ने सही साबित किया। टॉफलर ने इंटरनेट के बढ़ते चलन को देखते हुए भविष्य के इस
बदलाव को 1980 के दशक में ही भांप लिया था। मार्शल मैकलुहान ने भी मीडियम में हो
रहे बदलाव को महसूस करते हुए आने वाले दिनों में उपभोक्ताओं के मिज़ाज में बदलाव
को चिह्नित किया था।
डोनल्ड ट्रंप या कोई भी व्यक्ति जब ‘मुख्यधारा मीडिया’ को सोशल मीडिया
के बल पर चुनौती देते हैं तो उनके
जेहन में ये साफ़
रहता है कि उनके
फॉलोअर्स सीधे तौर
पर उनके दावे
पर भरोसा करेंगे
और जो उनके
दावों से असहमति
रखते हैं उनके
बीच भी ट्रंप
की तरफ़ से उठाए
गए मुद्दे ही बहस
के केंद्र में
होंगे। जिस ‘मुख्यधारा
के मीडिया’ पर
वो तीखे सवाल
उठा रहे हैं,
उन पर भी ट्रंप के बयान के इर्द-गिर्द ही बहसें होंगी। यानी
सूचना तंत्र का एजेंडा तय करने के लिए
उनकी तरफ़
से किया
गया एक ट्वीट
ही पर्याप्त साबित
हो सकता है।
न तो सोशल
मीडिया यूजर्स उस संदेश को नज़रअंदाज़ कर सकते
हैं और न ही
वो मीडिया जिनपर
सवाल उठाए गए हैं।
इस तरह ट्रंप
वो राजनीतिक बढ़त
हासिल करने की होड़
में दिखते हैं
जिसमें उनकी तरफ़
से फ़र्जी तथ्य,
झूठ और ग़लतबयानी
इस आधार पर न्यायसंगत नज़र आने लगेगा
कि झूठ अगर
ट्रंप बोल रहे
हैं तो मीडिया
भी शर्तिया झूठ
बोल ही रहा
होगा क्योंकि सवाल
दोनों तरफ़ से उठ
रहे हैं।
वस्तुनिष्ठ तरीके से अगर
इस चलन को देखने की कोशिश की जाए
तो तस्वीर ऐसी
बनेगी कि सैद्धांतिक
तौर पर एक पक्ष
आरोप लगा रहा
है और ठीक
उसी वक़्त दूसरा
पक्ष भी वही
आरोप दोहरा रहा
है जो पहले
ने लगाया है।
यानी स्कोर बराबर
है। अब अगला चरण इस
बात की पड़ताल
है कि दोनों
में से किनके
आरोपों में तथ्य
सच्चाई के क़रीब
है और किनमें
ये झूठ के क़रीब। लेकिन जब तक
ये पड़ताल पूरी
नहीं न हो,
तब तक दोनों
पक्षों के आरोपों
का वजन बराबर
है। वाशिंगटन पोस्ट
ने डोनल्ड ट्रंप
के बयानों को आधार
बनाकर एक विश्लेषण
छापा जिसमें ये बताया गया कि राष्ट्रपति
बनने के 263 दिनों
के दरम्यान डोनल्ड
ट्रंप ने 1318 फर्जी
और भ्रामक बयान
और दावे किए।[xii]
ज़ाहिर है डोनल्ड ट्रंप
पर मीडिया की तरफ़
से उठ रहे
सवालों के बाद
ख़ुद को साबित
करने का दबाव
लगातार बढ़ता गया
क्योंकि उनपर ये आरोप
नियमित अंतराल पर लगते
रहे हैं कि वो
अपने बयानों में
फर्जी तथ्यों का इस्तेमाल करते हैं। रिपोर्टर्स
विदाउट बॉर्डर्स ने प्रेस फ्रीडम इंडैक्स
2017 में अमेरिका की रैंकिंग गिरने के पीछे
सबसे बड़ी वजह
डोनल्ड ट्रंप के प्रचार अभियान में
फर्जी और भ्रामक
तथ्यों की बरसात
को बताया जिसे
आज हम पोस्ट-ट्रूथ परिघटना के तौर
पर जानते हैं।[xiii]
*************
21वीं सदी का निरक्षर वो नहीं होगा जो पढ़-लिख न सके, बल्कि वो
होगा जो सीखने, भूलने और फिर से सीखने की चेष्टा न कर सके- एल्विन टॉफलर
सोशल मीडिया यूजर्स के बारे में आम तौर पर ये धारणा
है कि वो बाक़ी मीडिया उपभोक्ताओं की तुलना में ज़्यादा चतुर, ज़्यादा समझदार और
ज़्यादा सक्रिय है। ये धारणा इसलिए बनी है क्योंकि ये ऐसा माध्यम है जिसमें यूजर
एक ही वक्त में उपभोक्ता होने के साथ-साथ उत्पादक भी होता है। यानी वो प्रोज्यूमर
है। वो एक जगह पर कुछ चीजों का उपभोग कर रहा होता है तो उसी क्षण दूसरे उपभोक्ताओं
के लिए वो कंटेंट का उत्पादन भी कर रहा होता है।
लेकिन बात जब राजनीतिक संदेश की जाए तो ये चलन साफ़ तौर पर देखा जा सकता है कि सोशल मीडिया पर अपने राजनीतिक रुझान के हिसाब से ही कंटेंट का उत्पादन हो रहा है। इसमें दो तरह के यूजर्स को वर्गीकृत किया जा सकता है। एक वो जिसकी राजनीतिक विचारधारा पहले से तय है और दूसरा वो जो सोशल मीडिया के प्रभाव में आकर अपनी राजनीति तय करता है। जिनकी राजनीतिक विचारधारा पहले से तय है वो अपनी पार्टी या विचारधारा के प्रचार और दूसरे को ख़ारिज करने के अंदाज़ में इस मंच पर सक्रिय नज़र आता है, जबकि जो सोशल मीडिया के कंटेंट के हिसाब से अपनी समझदारी विकसित करता है, वो भी आख़िरकार पहली श्रेणी के लोगों के बीच ही कुछ समय बाद खड़ा हो जाता है। भारतीय चुनाव प्रचारों में सोशल मीडिया के बढ़ते प्रभावों पर हुए अध्ययन इस बात की तरफ़ इशारा करते हैं कि जिस पार्टी की ऑन लाइन मौजूदगी जितनी ज़्यादा थी, युवाओं के बीच उसकी लोकप्रियता भी उसी अनुपात में नज़र आई।[xiv]
अगर
एल्विन टॉफलर की निगाह से पूरी परिघटना को देखा जाए तो ऐसा लगता है कि सोशल मीडिया कंटेंट को शक की निगाह से देखे और प्रामाणिक तथ्यों तक पहुंचे बग़ैर जो व्यक्ति सोशल मीडिया पर मौजूद कंटेंट को ही तथ्य मान ले वही ‘निरक्षर’ है। कैथरीन विनर का मानना है कि तथ्य, प्रति-तथ्य और समानांतर तथ्य का उत्पादन पोस्ट ट्रूथ के दौर में जिस तेज़ी से हो रहा है उसमें इन तीनों तथ्यों को बराबर वजन के साथ यूजर अपने बचाव में और दूसरों को ध्वस्त करने के इरादे से इस्तेमाल करता है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि कौन सा तथ्य सही है और कौन सा ग़लत।[xv]
डोनल्ड ट्रंप के बारे में
जो बातें ऊपर कही गई है अगर उसको भारत के परिप्रेक्ष्य में देखा जाए तो कई सारी
समानताएं देखने को मिल जाएंगी। जिस तरह आलोचनाओं को डोनल्ड ट्रंप ने खारिज करते
हुए तमाम मीडिया संस्थानों को देशविरोधी करार दिया, उस तरह का चलन भारतीय सत्ताधारी
पार्टी के मिज़ाज में भी देखने को मिलता है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कभी
सीधे तौर पर भारतीय मीडिया पर इस तरह के हमले नहीं किए, लेकिन कई बार आलोचनाओं के
चलते मीडिया पर तंज ज़रूर कसा।[xvi]
 |
| फ़ेसबुक और ट्वीटर पर नरेन्द्र मोदी को फॉलो करने वालों की तादाद करोड़ों में हैं। फोटो में मार्क ज़करबर्ग के साथ नरेन्द्र मोदी। |
नरेन्द्र मोदी ने टीवी और
अख़बारों को लेकर दूसरा रास्ता अख़्तियार किया। उन्होंने इन मीडिया संस्थानों में
गिने-चुने साक्षात्कार दिए, लेकिन प्रेस कांफ्रेंस एक भी नहीं किया। डोनल्ड ट्रंप
ने तमाम आलोचनाओं के बावजूद, मीडिया पर सबसे तीखे प्रहार और किरकिरी के बावजूद पत्रकारों
के सवालों का सामना किया, वहीं नरेन्द्र मोदी ने इसकी जहमत तक नहीं उठाई।[xvii]
टीवी चैनलों के कंटेंट पर
अगर विस्तृत शोध हो तो ये साफ़ नज़र आएगा कि ज़्यादातर चैनल्स सत्ताधारी पार्टी और
सरकार के नज़रिए को लेकर नरम रुख अपना रहे हैं। कड़े सवालों का अभाव स्पष्ट रूप से
दिखता है। ज़्यादातर चैनलों पर विपक्ष से ही सबसे ज़्यादा सवाल पूछे जा रहे हैं या
फिर उन बातों पर ज़ोर दिया जा रहा है जो बीजेपी के लिए मुफ़ीद हो।[xviii]
इस तरह टीवी चैनलों और
अख़बारों के साथ भारतीय प्रधानमंत्री के दो तरह के रिश्ते उभरकर सामने आते हैं। एक
रिश्ता बेहद गर्मजोशी भरा है जिसमें दोनों के सुर समान राग में एकमेक होते हैं,
वहीं दूसरा रिश्ता ऐसा है जिसमें दोनों की एक-दूसरे तक पहुंच सार्वजनिक मंचों पर
बेहद कम नज़र आता है। अब सवाल ये है कि अगर नरेन्द्र मोदी मीडिया के सवालों का
जवाब देने से बचते हैं तो फिर अपनी नीतियों को किस तरह समर्थकों और जनता तक
पहुंचाने का काम करते हैं और आलोचनाओं का जवाब देने के लिए किस प्लेटफॉर्म का
इस्तेमाल करते हैं? इस साल
के फ़रवरी महीने में नरेन्द्र मोदी फेसबुक पर दुनिया में सबसे ज़्यादा फॉलो किए
जाने वाले व्यक्ति बन गए। दूसरे नंबर पर कौन हैं? डोनल्ड ट्रंप।[xix]
ज़ाहिर है इन दोनों
राजनेताओं के लिए फ़ेसबुक और ट्वीटर बड़ा मंच है जहां ये एक साथ करोड़ों लोगों से
सीधे संवाद स्थापित करने में सक्षम हैं। सोशल मीडिया पर आलोचनाओं का जवाब न देने
के पीछे आसान सा तर्क दिया जा सकता है कि लाखों लोगों के सवालों और आरोपों का मिनट
भर के भीतर जवाब देना आसान काम नहीं है। लेकिन सवाल ये है कि क्या ट्रंप या मोदी
सोशल मीडिया यूजर्स को नोटिस नहीं करते? क्या उनके प्रति यूजर्स के रुझान से वो वाकिफ़ नहीं हैं
या फिर प्रशंसा करने वालों को वे प्रोत्साहित करते हैं?
नरेन्द्र मोदी के ट्वीटर
हैंडल को लेकर कई बार सवाल उठे कि वे ट्रोल्स को क्यों फॉलो करते हैं? नरेन्द्र मोदी ट्वीटर पर
जिन 2000 से कम लोगों को फॉलो करते हैं उनमें दर्जनों लोग ऐसे हैं जिनका सोशल
मीडिया पर व्यवहार बेहद आपत्तिजनक, अश्लील और बदमाशों वाला है।[xx]
एक समय ऐसा था जब नरेन्द्र मोदी विपक्ष के एक भी नेता को ट्वीटर पर फॉलो नहीं करते
थे, सवाल उठने के बाद उन्होंने गिनती के कुछ नेताओं को फॉलो करना शुरू किया।[xxi]
लेकिन ट्वीटर पर खुलेआम गालियां देने वाले लोगों को फॉलो करना उन्होंने आज तक बंद नहीं किया।[xxii]
यानी ये साफ़ है कि प्रधानमंत्री उन लोगों को प्रोत्साहन दे रहे हैं जो उनके समर्थक हैं, भले ही उनकी भाषा और उनका व्यवहार कितना ही आपत्तिजनक क्यों न हो? ये ऐसे लोग हैं जो
प्रधानमंत्री की नीतियों के प्रचार के लिए दूसरे यूजर्स को धमकी तक दे डालते हैं।
ट्वीटर पर लगातार ऐसी भाषा का इस्तेमाल करने वाले तजिंदर बग्गा को बीजेपी ने
प्रवक्ता बना दिया। तजिंदर बग्गा न सिर्फ़ ट्वीटर पर इस तरह की हरकत करने के लिए
कुख्यात हैं, बल्कि वो एक बार वरिष्ठ अधिवक्ता और राजनीतिक कार्यकर्ता प्रशांत
भूषण पर शारीरिक हमला भी कर चुके हैं। तजिंदर बग्गा की सबसे बड़ी ख़ासियत उनकी
ट्वीटर जैसे मंचों पर सक्रियता और सोशल मीडिया की समझदारी है और शायद इसी आधार पर
बीजेपी ने उन्हें नई ज़िम्मेदारी सौंपी।[xxiii]
दिलचस्प ये है कि प्रशांत भूषण पर हमला करने के ज़ुर्म में तजिंदर बग्गा के साथ जिस विष्णु गुप्त को गिरफ़्तार किया गया था, वो हर साल डोनल्ड ट्रंप का जन्मदिन मनाते हैं और प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के कट्टर समर्थक हैं। [xxiv]
नरेन्द्र मोदी सीधे तौर पर
समूचे मीडिया पर डोनल्ड ट्रंप की तरह जो सवाल नहीं उठाते, उसकी भरपाई ट्वीटर पर
प्रधानमंत्री और सत्ताधारी बीजेपी के समर्थक करते हैं। मसलन सोशल मीडिया पर प्रिंट
और टीवी मीडिया के लिए प्रेस्टीट्यूट और एनडीटीवी के लिए रंडीटीवी जैसे शब्दों का
इस्तेमाल आम है। साथ ही व्हाट्सएप जैसे मंचों पर किसी भी मैसेज के अंत में “बिकाऊ मीडिया आपको ये नहीं दिखाएगा” जैसे वाक्यों का रोज़ाना इस्तेमाल हो रहा है और इनमें से ज़्यादातर प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के समर्थक नज़र आते हैं। जब ये लोग प्रेस्टीट्यूट शब्द का इस्तेमाल करते हैं तो इसमें वो तमाम मीडिया संस्थान शामिल होते हैं जो सरकार की आलोचना का साहस करते हों। यानी भारत में भी मीडिया नाम की समूची संस्था की विश्वसनीयता को प्रेस्टीट्यूट जैसे शब्दों के ज़रिए एक झटके में ख़ारिज करने की कोशिश उस दिशा से हो रही है, जिन्हें इस मीडिया ने सर्वाधिक स्पेस दिया है और जिनके पक्ष में वो सबसे ज़्यादा खड़ा नज़र आता है। रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स की सालाना रिपोर्ट में प्रेस की आज़ादी इंडेक्स में जब भारत को तीन स्थानों का नुकसान हुआ तो इसके पीछे हिंदू राष्ट्रवाद की अतिरंजित बहस को मुख्य वजह माना गया। लेकिन सोशल मीडिया पर प्रेस्टीट्यूट जैसे शब्दों का इस्तेमाल वही लोग कर रहे हैं जो हिंदू राष्ट्रवाद के सबसे बड़े समर्थक हैं।[xxv]
भड़काऊ संदेश फैलाने, पत्रकारों को धमकी देने, पत्रकारों की हत्या का जश्न मनाने और उन्हें गाली देने वाले लोगों को ट्वीटर पर प्रधानमंत्री अगर फॉलो करते हैं तो इसका साफ़ मतलब है कि डोनल्ड ट्रंप की तरह वो भी खुलकर अपने आलोचकों से फटकार की मुद्रा में मुखातिब होना चाहते हैं।[xxvi]
पत्रकारों की हत्या और
पत्रकारों को धमकी के मामले में भारत का हाल बेहद ख़राब है। मीडिया में ये बात
प्रमुखता से उठी कि 2017 में रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स की प्रेस फ्रीडम इंडेक्स
में भारत तीन स्थान पिछड़कर 136वें नंबर पर पहुंच गया, लेकिन इस बात पर ध्यान नहीं
दिया गया कि ‘एब्यूज़ स्कोर’ यानी ख़तरों और धमकियों के मामले में भारत दुनिया का 19वां सबसे बदतर देश है। पाकिस्तान, नाइजीरिया, बांग्लादेश और कैमरून से भी बदतर।[xxvii]
देश में कई पत्रकार इस बात
को लेकर खुली नाराजगी जता चुके हैं कि राजनीतिक पार्टियों के लोग और समर्थक
असहमतियों के चलते सोशल मीडिया पर ट्रोलिंग करने लगते हैं। भारत में पत्रकारों के
मामले में धमकियों, गिरफ़्तारियों और हत्याओं के आंकड़ों पर ग़ौर करें तो बेहद ख़ौफ़नाक
तस्वीर सामने आती है। यूनेस्को के मुताबिक़ 21वीं सदी में भारत में जितने
पत्रकारों की हत्या हुई है उनमें सिर्फ़ एक केस में हत्यारे को सज़ा सुनाई गई और
उसमें भी ऊपरी अदालत में अभी अपील दर्ज है। मीडिया राज के संपादक राजेश मिश्रा की
हत्या में अदालत ने एक व्यक्ति को सज़ा सुनाई, दो बरी हुए। मामला अपील में है।
इनको छोड़ दें तो अब तक एक भी मामला ऐसा नहीं है जिसमें पत्रकार के हत्यारों को
सज़ा मिली हो।[xxviii]
ऐसे में सोशल मीडिया पर अगर किसी पत्रकार को धमकी मिलती है और धमकी देने वाले व्यक्ति को अगर प्रधानमंत्री फॉलो कर रहा हो तो डर का भाव स्वाभाविक है। सोशल मीडिया ने उन सभी लोगों को ये ताक़त दी है कि वो किसी भी स्थापित पत्रकार से कई तल्ख़ सवाल कर सके और इस प्लेटफॉर्म पर अपने भीतर की उस भड़ास को भी निकाल सके, जिसे ‘मुख्याधारा के मीडिया’ में पत्रकारों द्वारा पेश किए गए कार्यक्रम या फिर रिपोर्ट को लेकर उन्होंने दिमाग़ में दर्ज़ कर रखा हो। लेकिन सवाल और धमकी के बीच का जो रेशा भर का फर्क है उसी को लांघना ट्रोल हो जाना है।
वापस डोनल्ड ट्रंप और प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के बीच मौजूद समानताओं की बात करते हैं। डोनल्ड ट्रंप की ग़लतयानी को अमेरिकी मीडिया ने तालिका बनाकर पेश किया। भारत में ऐसा कोई डेटाबेस अब तक नहीं बना है, जिसमें नरेन्द्र मोदी द्वारा पेश किए गए ग़लत आंकड़ों और तथ्यों की सूची बनाई गई हो, लेकिन वक़्त-वक़्त पर उनके दावों पर सवाल ज़रूर उठाए गए। कई मौक़ों पर प्रधानमंत्री ने फर्जी तथ्य, ग़लत आंकड़ों और झूठ का सार्वजनिक पाठ किया है।[xxix] सोशल मीडिया पर लाखों लोग
इन्हीं फर्जी तथ्यों और आंकड़ों का पुनर्उत्पादन करते हैं और लाखों रिट्वीट और
हज़ारों बार मीडिया कवरेज पाने के बाद एकबारगी तथ्य का नकलीपन इतना कमज़ोर हो जाता
है कि अगली बार ऐसे ‘तथ्य’ आने पर ‘सामान्य’ रहने का एहसास होता है। मीडिया अध्ययन में तथ्यों के
पुनर्उत्पादन को लेकर हुए शोध में ये माना गया है कि दोहराव यानी रिडंडेंसी पाठकों
के दिमाग़ पर असर करता है और एक ख़ास तरह की तस्वीर का निर्माण करता है।[xxx]
सहमति के निर्माण की बात जिस तरह नोम चोम्स्की ने कही है, उसी पैटर्न पर दशकों से
मीडिया अध्ययन में बातें उठती रही हैं। वाल्टर लिपमैन ने 1920 के दशक में पब्लिक
ओपिनियन में इसी बात पर ज़ोर दिया था कि मीडिया किस तरह लोगों के दिमाग़ में एक
काल्पनिक तस्वीर का निर्माण करता है, जिसका वास्तविकता से लेना-देना नहीं भी हो
सकता है।
दोहराव के मामले में रेडियो, प्रिंट और
इलेक्ट्रॉनिक तीनों माध्यमों के मुकाबले सोशल मीडिया कहीं ज़्यादा शक्तिशाली है।
एक ही संदेश लाखों लोग कॉपी-पेस्ट कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। वही संदेश एक
साथ कई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर नमूदार हो सकते हैं। उसी बात को वो मीडिया भी
अपने मंच पर जगह दे सकता है, जिसे आम तौर पर सोशल मीडिया के मुकाबले ज़्यादा
संजीदा और पारंपरिक माना जाता है। 2000 रुपए के नए नोट में चिप होने की अफ़वाह ने
टाइम्स ऑफ़ इंडिया से लेकर ज़ी न्यूज़ जैसे संस्थानों में ख़बर के तौर पर जगह पाई।[xxxi]
इस लिहाज से किसी भी राजनेता और राजनीतिक पार्टी के
पास अपनी प्रचार सामग्रियों को लोगों के जेहन में उतार देने का ऐसा ज़रिया मौजूद
है कि वो रोज़ाना ‘सूचनाओं’ की बमबारी कर लोगों की
चेतना पर कब्ज़ा कर सकता है। जिस तरह किसी को प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया जैसे
पारंपरिक सूचना तंत्र को वैचारिक तरीके से अपने पाले में करने का विकल्प उपलब्ध
है, वही विकल्प सोशल मीडिया मंच पर भी उपलब्ध है। दूसरे माध्यम से ये सिर्फ़ इस
बिनाह पर अलग है कि इसमें हर यूजर के पास अपनी बात कहने का सैद्धांतिक तौर पर
बराबर जगह और अधिकार है। लेकिन तकनीक पर नियंत्रण का जो समाजशास्त्र है उसे हरबर्ट
आई शिलर ने विस्तार से समझाया है। तकनीक का इस्तेमाल और अपनी वैचारिकी को उसके
ज़रिए पुनर्उत्पादित करने की क्षमता सबके पास बराबर नहीं हो सकती। टीवी मीडिया
कल्चर में एकरूपता की एक वजह के तौर पर इसको भी चिह्नित किया गया है कि इसकी तकनीक
सबके लिए सुलभ नहीं थी। मामला मीडिया कल्चर तक ही सीमित नहीं है, बल्कि टीवी ने
दुनिया की संस्कृति को एकमेक करने की कोशिश की है और काफी हद तक इसमें सफल भी रहा
है।[xxxii]
संस्कृति उद्योग का ये मामला उतने ही संगठित तौर पर सोशल मीडिया पर भी दिख रहा है,
लेकिन उसमें काउंटर आवाज़ भी मुखर है। इसी फर्क के चलते कई लोग सोशल मीडिया को
वैकल्पिक मीडिया के तौर पर पेश करने की कोशिश करते रहते हैं। सोशल मीडिया और
टीवी-प्रिंट मीडिया में सिर्फ़ माध्यम का फर्क है। मीडिया कोई भी वैक्लिपक नहीं हो
सकता, वैकल्पिक नैरेटिव यानी कथ्य और राजनीतिक विचारधारा होती है।[xxxiii]
प्रिंट और टीवी पर जब इसी वैकल्पिक कथ्य का दबाव
बनता है तो कई दफ़ा वो उन ख़बरों को भी उठाने पर मजबूर हो जाते हैं जो सोशल मीडिया
पर ज़ोर-शोर से उठाए जा रहे हों। ऊना से लेकर बीएचयू तक दर्जनों ऐसी घटना है
जिसमें सोशल मीडिया और टीवी-प्रिंट का तुलनात्मक अध्ययन करने पर परस्परविरोधी
नैरेटिव बनता नज़र आएगा। इनमें से कई ख़बरें ऐसी हैं जिन्हें सोशल मीडिया के दबाव
में टीवी पर जगह मिली। असल में टीवी चैनल और अख़बार भी सोशल मीडिया पर उतना ही
सक्रिय है जितना कोई आम यूजर, बल्कि आम यूजर से कहीं ज़्यादा संगठित तौर पर ये
मीडिया संस्थान सोशल मीडिया का इस्तेमाल करते हैं। लिहाजा सोशल मीडिया उनके लिए
पुनर्उत्पादन का मज़बूत मंच बन जाता है। भारत में नरेन्द्र मोदी के लिए सोशल
मीडिया प्राथमिक मंच भी है और ‘मुख्यधारा के मीडिया’
के रास्ते पुनर्उत्पादन का मंच भी। डोनल्ड ट्रंप और नरेन्द्र मोदी में सिर्फ़ यही
बारीक फ़र्क है।
[i] 6 जून 2017, 5.28 PM (https://www.vox.com/policy-and-politics/2017/6/7/15749218/donald-trump-problem-with-twitter-is-not-mainstream-media)
[iv] (http://www.trumptwitterarchive.com/archive/%22media%20%22%7C%7C%20fake%20news%20%7C%7C%20MSM%20%7C%7C%20fake%20media%20%7C%7C%20mainstream%20media/tfff/1-20-2017_6-30-2017)
[vi] विकास
संचार और मुक्त सूचना प्रवाह के अंतर्संबंध के राजनीतिक पहलू, दिलीप ख़ान, जन
मीडिया, वॉल्यूम-1, अंक-4
[vii] (https://www.vox.com/policy-and-politics/2017/2/24/14729078/white-house-banned-media-outlets-press-briefing)
[viii] (https://www.theguardian.com/us-news/2017/oct/11/donald-trump-tweet-nbc-news-challenge-license)
[ix] (http://www.adweek.com/digital/kurt-abrahamson-sharethis-guest-post-social-media-is-the-new-television/)
[xi] https://www.smartinsights.com/social-media-marketing/social-media-strategy/new-global-social-media-research/
[xii] (https://www.washingtonpost.com/graphics/politics/trump-claims-database/?tid=a_inl&utm_term=.92f47fabebb5)
[xiv] https://www.omicsonline.org/open-access/social-media-for-political-mobilization-in-india-a-study-2165-7912-1000275.pdf
[xv] तकनीक ने कैसे सच का गला घोंटा, कैथरीन विनर
(अनुवाद- दिलीप ख़ान) http://dakhalkiduniya.blogspot.in/2017/01/blog-post.html
[xix] http://www.huffingtonpost.in/2017/02/21/pm-modi-becomes-the-most-followed-leader-on-facebook-donald-tru_a_21718457/
[xxii] https://satyagrah.scroll.in/article/109492/why-pm-modi-follows-those-on-twitter-who-are-crossing-every-limit-while-commenting-on-gauri-lankesh
[xxiii] http://www.news18.com/news/politics/delhi-bjp-appoints-twitter-savvy-tajinder-singh-bagga-as-spokesman-1360007.html
[xxiv] https://scroll.in/latest/840625/delhi-hindu-sena-hosts-celebrations-for-donald-trumps-71st-birthday
[xxvi] https://www.altnews.in/alt-news-investigation-people-behind-targeted-harassment-ravish-kumar-via-whatsapp/
[xxix] https://scroll.in/article/829999/fact-checking-modi-in-uttar-pradesh-some-claims-partially-true-others-exaggerated-or-false
[xxx] The Role of the Press
in the Reproduction of Racism, Teun A. van Dijk
[xxxi] अफ़वाह,
सोशल मीडिया और पोस्ट ट्रूथ का दौर, दिलीप ख़ान http://dakhalkiduniya.blogspot.in/2016/12/blog-post_29.html
[xxxii]
Globalization of Culture Through the media, Marwan M Kraidy, page-7
[xxxiii] वैक्लपिक
मीडिया की भ्रामक अवधारणा, दिलीप खान, दैनिक जागरण, 18 मई 2017, http://dakhalkiduniya.blogspot.in/2017/05/blog-post.html
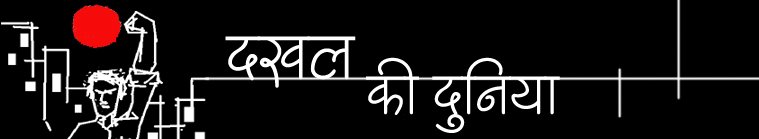





lifestyle matters
जवाब देंहटाएंtechnology solutions
शानदार
जवाब देंहटाएंOver the last 6 weeks I've actually got serious with reference to Weight Loss. That is heavy handed. I believe there will be a big price to pay anyhow. Consequently, maybe I am seeing this with Weight Loss and I could do a lot better. In that way, one can have pleasant feelings for their Dietary Supplements. It can be straightforward to do. This is how to end worrying relative to what others think.
जवाब देंहटाएंhttps://www.nutraket.com/excel-keto-gummies/
https://www.nutraket.com/lets-keto-gummies/
https://www.nutraket.com/rejuvenate-cbd-gummies/
https://www.offerplox.com/weight-loss/lets-keto-gummies/
https://www.offerplox.com/weight-loss/keto-extreme-fat-burner/
https://www.claimhealthy.com/lifetime-keto-gummies/
https://www.claimhealthy.com/sweet-relief-cbd-gummies/
https://usanewsindependent.com/2023/01/animale-male-enhancement-animal-cbd-gummies-for-men-reviews-2023/
Remember to stay calm and confident during the exam. Trust in your preparation, and
जवाब देंहटाएंLastly but certainly not least important - customer support! Should you encounter any issues or have questions during your preparation journey, DumpsArena has an excellent support team ready to assist you promptly and effectively.
In conclusion (as per instructions), these are just a few highlights among many other remarkable features offered by DumpsArena's DP-203 exam dumps. With their accurate content, user-friendly interface, detailed explanations
Upto 70% Discount ON THIS https://dumpsarena.com/microsoft-dumps/dp-203/
Latest Updates Await! >>>>> DP-203 Exam Dumps
100 percent Unconditional promise - An Assurance For Your Test
जवाब देंहटाएंWe unequivocally trust in our program and know as a matter of fact that our CRCM practice test questions works. We feel somewhat doubtful. In any case, in the event that you go through the materials, yet bomb the test, we'll give you a full discount. crcm pass rate maintain that every one of our clients should be blissful and fulfilled and accept the 100 percent Unconditional promise pursues the buy choice an easy decision for any individual who doesn't as a rule joke around about finishing the test.
We Offer Substantial CRCM Test Questions
As an expert site, crcm exam pass rate offers you the most recent and most legitimate ABA CRCM Practice Test and ABA CRCM test questions, assessed by our accomplished and profoundly gifted IT commentators. You can be certain beyond a shadow of a doubt that our material is precise and refreshed.
Our Site Strategy
You can access on-line to the free preliminary of ABA CRCM Practice Test before you purchase. After you make the buy, you will be permitted to get free updates with the most recent CRCM practice test questions. There is an every minute of every day client care helping you on the off chance that you find any issues while making the buy or examining. Exam-Labs Note that you likewise reserve the privilege to a full discounted or change to other ABA Practice Test for nothing on the off chance that you don't breeze through the test with our CRCM Testing Motor.