अभिषेक श्रीवास्तव के द्वारा प्रस्तुत यह रिपोर्ट तहलका मे प्रकाशित हुई जिसे हम यहां प्रस्तुत कर रहे है :-

राजेंद्र रवि एक राजनीतिक कार्यकर्ता हैं। गाहे-बगाहे उन्हें लेखक भी कहा जा सकता है और उनकी पहचान सामाजिक-राजनीतिक आंदोलनों में असंसदीय गलियारे में नारे लगाने वाले हजारों आम चेहरों में एक के रूप में भी की जा सकती है। आम तौर पर वे परिवहन क्षेत्र के विशेषज्ञ माने जाते हैं और दिल्ली के चांदनी चौक में रिक्शों को बंद करवाने के सरकार के फैसले के दौरान 'रिक्शा: एक महागाथा' नामक पुस्तक से वे चर्चा में आए। उनकी एक अन्य पुस्तक हाल ही के दिनों में बाजार में आई है जिसका नाम है 'यथार्थ की धरती और सपना'।
यह पुस्तक किसी विशेष उद्देश्य से नहीं लिखी गई है। यह राजेंद्र रवि द्वारा समय-समय पर लिखे आलेखों और अनुभवों का एक संकलन है जो उन्हें सार्वजनिक राजनीति में आने के बाद हुए और जिनके प्रति उनकी लेखनी सक्रिय रही। चूंकि लंबे समय से रवि दिल्ली में ही रह रहे हैं, इसलिए जाहिर तौर पर उनका कार्यक्षेत्र दिल्ली ही है और यहीं के शहरी नियोजन पर उन्होंने काफी काम किया है।
पुस्तक चार खंडों में है। पहला खंड परिवहन व्यवस्था पर है, दूसरा पर्यावरण पर, तीसरा महिलाओं की समस्याओं से जुड़ा है और आखिरी खंड में वंचित-शोषित दुनिया के जो पक्ष छूट गए हैं, अधिकतम को समाहित कर लिया गया है। सार्वजनिक जीवन या राजनीतिक दायरे में पहले-पहल उतर रहे किसी भी व्यक्ति के लिए यह पुस्तक आंदोलनों के प्रति आस्था और निगरानी का एक स्रोत है, विश्व दृष्टिकोण का एक खाका निर्मित करने की जंत्री है और समाज विज्ञान में एक प्रवेशिका है।
लेखक पुस्तक की भूमिका में जो स्वीकार करते हैं, दरअसल वही इस पुस्तक को पढ़ने के बाद जेहन में पहला ख्याल भी आता है, 'मुझे इस बात का गहरा एहसास है कि यह पुस्तक अलग-अलग मुद्दों पर केंद्रित अपनी विशिष्ट सामग्री के चलते किसी विषय का गंभीर विवेचन प्रस्तुत नहीं करती। इस तरह के किसी संग्रह से ऐसी अपेक्षा करना बहुत उपयुक्त भी नहीं है।' दरअसल, यही स्वीकारोक्ति इस पुस्तक की जान है।
सामाजिक जीवन में उतरने वाले किसी भी व्यक्ति के लिए दुनिया के तमाम मसलों पर कोई एक राय बनाना बहुत मुश्किल होता है क्योंकि तमाम किस्म के पक्ष उसे अपनी ओर खींचने में लगे होते हैं।
कह सकते हैं कि आम तौर पर ऐसे छात्रोपयोगी विषयों पर पुस्तकें बहुत कम हैं और हैं भी, तो विषयों पर काफी बोरियत पैदा करती हैं। इस लिहाज से भी प्रस्तुत पुस्तक पढ़ने लायक कही जा सकती है। इसमें आपको दिल्ली के मजदूरों और रिक्शा खींचने वालों की दिक्कतों से लेकर ब्राजीली शहरों के नियोजन के मॉडल सम्बन्धी उदाहरण मिल जाएंगे। एक ओर जहां आदिवासियों की कीमत पर आधुनिक विकास की बात मिलेगी, वहीं भोपाल गैस कांड या संभावित परमाणु युद्ध के चलते धरती के बदले हुए नक्शे की तस्वीर दिखाई देगी। जल, जंगल और जमीन के सवालों पर लोगों के लुटने-पिटने के उदाहरण शामिल हैं, तो घरेलू हिंसा और विस्थापन की मार झेल रही महिलाओं का दर्द भी बयां है।
तमाम सवालों के बीच दिल्ली के मालियों पर एक आलेख विशेष तौर पर ध्यान खींचता है क्योंकि इनके बारे में आम तौर पर कहीं पढ़ने को नहीं मिलता। हमें यह जान कर आश्चर्य होता है कि मालियों को अपने ही घर से बाल्टी और औजार लाने के आदेश भी इसी दिल्ली में जारी किए जा चुके हैं। यह भी पढ़ने को मिलेगा कि दिल्ली के छिटपुट जंगलों से लकड़ी की अवैध कटाई भी होती है और इसका विरोध करने पर मालियों को खतरे भी उठाने पड़ते हैं।
इसके अलावा रवि आपको ब्राजीली शहर क्यूरीटीबा ले जाते हैं जहां के शहरी नियोजन को मानक के तौर पर बताया गया है। एक बहुत बढ़िया और बुनियादी बात आप देखेंगे जो इस शहर के बारे में कही गई है- क्यूरीटीबा के 99 फीसदी बाशिंदों का कहना था कि उन्हें अपने शहर में रहना अच्छा लगता है। यह बात देखने में चाहे जितनी भी सहज लगे, लेकिन यदि यही सवाल हमारे देश के सिर्फ चार महानगरों के बाशिंदों से पूछा जाए, तो आप ऐसे जवाब की कितने लोगों से उम्मीद करेंगे। एक ऐसा शहर जहां के 99 फीसदी लोगों को वहां रहना भाता हो, अपने आप में एक अद्भुत परिघटना है।
ऐसे तमाम चौंकाने वाले उदाहरणों से मिलकर बनी है यह पुस्तक। यकीन मानिए जैसा कि पहले मैंने कहा- सार्वजनिक जीवन या राजनीतिक दायरे में पहले-पहल उतर रहे किसी भी व्यक्ति के लिए यह पुस्तक आंदोलनों के प्रति आस्था और निगरानी का एक स्रोत है, विश्व दृष्टिकोण का एक खाका निर्मित करने की जंत्री है और समाज विज्ञान में एक प्रवेशिका है।
अकादमिक जटिलता से बचते हुए यदि जनता के जमीनी मसलों से साबका बैठाना हो, समय कम हो और भाषा बोलचाल वाली समझ में आती हो- तो इस पुस्तक को एक बार जरूर देखें। कहीं-कहीं लेखक के आत्मवृतान्त के संदर्भ में दुहराव दिख सकता है, लेकिन उसे नजरअंदाज कर दें। जाहिर तौर पर जनता के बीच काफी दिनों तक काम करने के बाद नागरिक समाज का हिस्सा बन जाने पर एक आत्ममुग्धता जैसी चीज घर कर ही जाती है। मूल बात उन अनुभवों, संस्मरणों और तथ्यों में छुपी है जो पुस्तक की जान है। पूरी पुस्तक पढ़ने के बाद ही आपको पुस्तक के नाम का औचित्य समझ में आएगा, शुरू में नहीं।
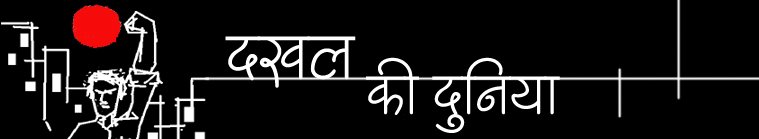
दखल का मुद्रित अंक यहा देने का धन्यवाद !
जवाब देंहटाएंकृपया इसे भी देखें और अपने ब्लॉग रोल में जगह दें sandoftheeye.blogspot.com
धन्यवाद !