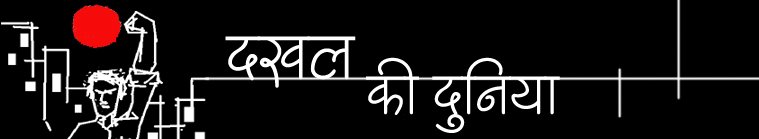गांव और गरीबी मुम्बई से नहीं दिखती न ही काला हांडी, न बस्तर, न विदर्भ, और न मुम्बई की बम्बई कुछ भी तो नहीं दिखता आज की मुम्बईया फिल्मों में जो सत्यजीत रे की निगांहों ने देखा और पर्दे पर उतारा . हाशिये के रेयाज भाई का सत्यजीत रे की फिल्मों पर लिखा एक आलेख हम प्रकाशित कर रहे हैं.
एक बार फिर दुर्गा और अपु को याद करें, उस समय जब वे कास के पौधों के बीच भाग रहे थे. याद करें उनका टेलीफोन के बजते तारों को सुनना. उनकी चकित-विस्मित भंगिमा. उनकी आपसी नाराजगी और उसके बीच घुली ईख की मिठास. और तभी कास के फूलों के उस पार धुआं छोडती, धडधडाती रेलगाडी गुजरती है. दोनों पहली बार ट्रेन देखते हैं. हवा में एक तीखी सीटी गूंजती है. कैमरा अपु और दुर्गा के पीछे से हट कर पटरी की दूसरी तरफ चला जाता है और भागती हुई ट्रेन के पहियों के अंतराल में से दिखते हैं अपु और दुर्गा. यह दृश्य विश्व सिनेमा के इतिहास में कभी न भुलाये जा सकनेवाले दृश्यों में से एक है.
जब भी पाथेर पांचाली देखा है, लिंडसे एंडरसन की तरह घुटनों तक भर आयी धूल को महसूस किया है. आधी सदी से अधिक समय गुजरने के बाद यह धूल और गाढी हुई है.
सत्यजीत राय को गरीबी का कलाकार कहा गया. उन्होंने अपनी फिल्मों में भारतीय समाज के रेशे-रेश में पैठी गरीबी और विपन्नता को जिस तरह, जिस दौर में, जिन अभावों के बीच प्रस्तुत किया, वह कल्पना से परे की बात लगती है.
स्कूली दिनों से ही सत्यजीत राय के भीतर फिल्मों ने अपनी जगह बना ली थी. वे जब प्रेसीडेंसी कॉलेज से ग्रेजुएशन करने के बाद शांतिनिकेतन में रह कर पेंटिंग की शिक्षा ले रहे थे, इस बात पर अफसोस कर रहे थे कि वहां उन्हें हॉलीवुड की फिल्में देखने को नहीं मिल रही हैं और सिटीजन केन जैसी फिल्म कलकत्ता में लग कर निकल चुकी और वे उसे नहीं देख पाये. हालांकि शांतिनिकेतन में उनके गुरु नंदलाल बोस और विनोद बिहारी मुखोपाध्याय जैसे प्रख्यात चित्रकार थे, उनका मन पश्चिमी संगीत सुनने में अधिक लगता और वे अंगरेजी के एक अध्यापक के यहां संगीत सुनते हुए शामें गुजारना अधिक पसंद करते.
१९४२ में सत्यजीत राय ने शांतिनिकेतन छोडने का फैसला कर लिया और वे उस दिन शांतिनिकेतन से निकल आये, जिस दिन कलकत्ता पर जापान ने पहली बार बमबारी की थी. इसके बाद सत्यजीत राय ने एक विज्ञापन एजेंसी में ग्राफिक्स डिजाइनर के रूप में नौकरी पायी. इस ब्रिटिश कंपनी में काम करने के अलावा वे किताबों के लिए रेखांकन और उनके आवरण बनाने का काम भी करते. यहीं पाथेर पांचली पहली बार उनके कलाकर्म में दाखिल हुई, जब उन्होंने उसके एक संक्षिप्त संस्करण के लिए आवरण बनाया.
सत्यजीत राय ने फिल्मों पर किताबें पढना भी शुरू कर दिया था. वे बांग्ला में पारसी थिएटर के तर्ज पर बन रही मेलोड्रामा फिल्मों से खीझे हुए रहते. १९४४ में उन्होंने रोजर मानवेल की किताब 'फिल्म' पढ ली थी और उन्हें हॉलीवुड तथा दूसरे देशों की फिल्मों को देखे-दिखाये जाने की जरूरत महसूस हो रही थी. अपने कुछ मित्रों के साथ उन्होंने एक फिल्म सोसायटी बनाने की बात सोची और १९४७ में कलकत्ता फिल्म सोसायटी की स्थापना की गयी. इस सोसायटी ने कलकत्ता में गंभीर सिने प्रेमियों का पहली बार विश्व के श्रेष्ठतम कहे जानेवाले सिनेमा से परिचय कराया. उन दिनों सोसायटी में सेर्गेइ आइजेंस्टाइन, पुदोव्स्की, रॉबर्ट फ्लेहार्टी, जॉन ग्रियरसन, मार्शल कार्न, ज्यूलियन दुविविअर की फिल्में दिखायी जातीं. विश्व की सर्वकालिक सर्वश्रेष्ठ मानी जानीवाली आइजेंस्टाइन की बैटलशिप पोटेमकिन, स्ट्राइक, जनरल लाइन और अलेक्जेंडर नेव्स्की तथा पुदोव्स्की की स्टार्म ओवर एशिया जैसी फिल्मों का प्रदर्शन हुआ. सोसायटी में आनेवालों में ज्यां रेनोइर, पुदोव्किन, निकोलाई चेरकासोव और जॉन हस्टन जैसी महत्वपूर्ण हस्तियां थीं.
१९४८-४९ के आसपास ज्यां रेनोइर अपनी फिल्म द रिवर की शूटिंग के लिए कलकत्ता आये. सत्यजित राय उनसे मिले और इसी फिल्म के सेट पर राय की मुलाकात एक २१ वर्षीय फोटोग्राफर सुब्रत मित्रा से हुई. सुब्रत एक स्टिल फोटोग्राफर थे और उनकी खींची कुछ तसवीरें देखने के बाद सत्यजीत राय ने उन्हें एक अजीब-सा प्रस्ताव दिया. उन्होंने मित्रा से कहा कि वे राय की फिल्म में -जिसे वे भविष्य में बनायेंगे- सिनेमेटोग्राफर बन जायें.
और इस तरह अब तक एक फुट भी फिल्म शूट नहीं करनेवाले मित्रा उस फिल्म के सिनेमेटोग्राफर बन गये, जो विश्व सिनेमा में मील का पत्थर बननेवाली थी, जो फिल्म निर्देशन और फिल्मांकन का अपने आप में एक स्कूल है.
लेकिन अभी पाथेर पांचाली की शुरुआत नहीं हुई थी.
राय जिस कंपनी में काम करते थे, १९५० में उसने उनका तबादला लंदन स्थित अपने मुख्यालय में कर दिया. लंदन में अपने छह महीनों के प्रवास के दौरान राय ने ९९ फिल्में देखीं. इनमें रेनोइर की लॉ रीगल डू जिया और प्रख्यात इतालवी निर्देशक वेट्टेरियो डिसिका की मशहूर फिल्म बाइसिकल थीव्स शामिल थी.
लंदन से लौटते वक्त उन्होंने जहाज पर ही पाथेर पांचाली की पटकथा लिखनी शुरू कर दी.
राय ने अपनी पहली लंदन यात्रा से बहुत कुछ सीखा. फिल्मों में दृश्यों को प्रभावशाली बनाने के लिए रेनोइर की तरह अभिव्यिक्ति का अर्थशास्त्र और उसकी कला, समय का उपयोग और कथ्य को ऊंचाई देने के लिए विवरणों की जरूरत सीखी. उन्होंने यह सीखा कि छोटी-सी लगनेवाली कहानी को डिसिका की तरह समृद्ध कथा संदर्भों और सांस्कृतिक अनुपूरकों के जरिये किस तरह सफलतापूर्वक प्रस्तुत किया जा सकता है.
१९५२ में उन्होंने अपनी कंपनी से कुछ महीनों की छुट्टी ली और पाथेर पांचाली पर काम शुरू किया.
जब फिल्म की पटकथा पूरी हो चुकी थी, संवाद लिख लिये गये थे और पटकथा से लेकर संगीत और कैमरे की पोजीशन तक की बातें तय कर ली गयी थीं, राय के मित्रों ने उनसे यह फिल्म नहीं बनाने को कहा. उन्हें विश्वास नहीं था कि राय जिस तरह की फिल्म चाहते हैं उसे बनाना संभव है, खास तौर पर उसे बनाने के लिए जितने संसाधन उनके पास हैं, उनमें तो और भी नहीं. लेकिन राय उनसे सहमत नहीं थे.
पाथेर पांचाली की शूटिंग शुरू हुई, एक ऐसी फिल्म, जिसका अधिकतर हिस्सा आउटडोर में शूट होना था, बिना अनुभवी कलाकारों के, बिना मेकअप के. पाथेर पांचाली की पूरी यूनिट अनुभवहीन लोगों की थी. किसी को भी सिनेमा का अनुभव नहीं था. खुद सिनेमेटोग्राफर वास्तव में एक फोटोग्राफर था. संपादक ने इसके पूर्व सिर्फ एक फिल्म कट की थी. मुख्य नारी पात्र सर्वजया (करुणा बनर्जी) वास्तव में राय के एक एक्जीक्यूटिव मित्र की पत्नी थी. अपु और दुर्गा की भूमिकाओंवाले बच्चों को भी अभिनय का अनुभव नहीं था. सिर्फ इंदिर ठाकरुन की भूमिका निभा रहीं ८० साल की चुनीबाला देवी ही ऐसी कलाकार थीं, जो दशकों पूर्व कभी अभिनय कर चुकी थीं और अब रेड लाइट एरिया से आती थीं. यहां तक कि खुद निर्देशक की यह पहली फिल्म थी और ग्राम्य जीवन पर आधारित इस फिल्म के इस निर्देशक को गांवों के बारे में सिर्फ उतना ही पता था, जितना इस फिल्म की पटकथा बताती थी. इसे सत्यजीत राय ने स्वीकारा है कि उनकी पूरी यूनिट ने फिल्में देख कर और पाथेर पांचाली की शूटिंग के दौरान फिल्म निर्माण के बारे में सीखा.
फिल्म की शूटिंग पूरी होने में ढाई साल लग गये. शूटिंग सप्ताहांत में और आउटडोर लोकेशन पर होती. इस पूरी अवधि में यूनिट को दो बातों का डर लगा रहा. एक तो यह कि अपु और दुर्गा की भूमिकाएं निभा रहे बच्चे बडे न दिखने लग जायें और दूसरा यह कि चुनीबाला देवी की मृत्यु न हो जाये. हालांकि ऐसा हुआ नहीं.

फिल्म का संपादन १० दिनों में हुआ, इनमें रातें भी शामिल हैं. जल्दबाजी की एक वजह थी. अमेरिका के मुनरो ह्वील ने न्यूयार्क म्यूजियम ऑफ माडर्न आर्ट में भारतीय संस्कृति पर एक आयोजन किया था और उस दौरान इस फिल्म का विशेष प्रदर्शन भी होना था. जैसे-तैसे कट किया गया और बिना सबटाइटल के यह बांग्ला फिल्म मई, १९५५ में अमेरिका भेजी गयी. कहने की जरूरत नहीं कि इस फिल्म ने वहां के लोगों को इस विद्रूपताओं से भरे भारतीय यथार्थ पर उद्वेलित किया.
पाथेर पांचाली भारतीय विपन्नता की पहली वैश्विक चीख थी. यह आलोकधन्वा की कविता पंक्तियों की मदद से कहा जाये तो विलासिता और मनोरंजन की दुनिया में अचानक आ घुसे करोडों विपन्न लोगों के अश्लील उत्पात की तरह थी. यह उनकी मुक्ति के लिए आर्तनाद थी. इसकी मौजूदगी का अहसास उतना कहीं और नहीं होता जितना पलायन कर रहे परिवार के साथ पार्श्व में बजते संगीत को सुनते हुए होता है.
पाथेर पांचाली के पहले भारत की गरीबी को इतनी विश्वसनीयता और अंतरंगता से कभी नहीं देखा गया था. यह फिल्म अपने दर्शकों को-जो प्रायः उच्च वर्ग और मध्यवर्ग से आते थे-बताती थी कि दुनिया में दूसरी तरह के लोग भी रहते हैं और यह कि वे किस तरह जीते हैं. पाथेर पांचाली अपने उेश्य में इतनी सफल रही कि अमेरिका में इसके एक प्रदर्शन के दौरान कुछ लोग यह कहते हुए उठ कर चले गये कि वे लोगों को हाथ से खाते नहीं देख सकते.
पाथेर पांचाली ने नयी सिने भाषा और नयी सिने संभावना दी-जिसमें गीत, नृत्य और रोमांस के बिना भी फिल्में बनायी जा सकती थीं. पाथेर पांचाली ने इसी के साथ एक और बडा काम किया-उसने दूसरी भारतीय कलाओं जितनी ऊंचाई और उत्कृष्टता सिनेमा को दी.
किसी ने ऐसा पहले कभी नहीं देखा था-धान के खेत, नरकुल के जंगल, कास के दूर-दूर तक फैले पौधे, पास आती ट्रेन की सीटी, काई से ढंके तालाब का धब्बेदार शीशे जैसा दृश्य, पोपले मुंह और झुकी कमरवाली एक वृद्धा का अभिनय और गरीबी से त्रस्त एक नारी की कटुता और अपने बच्चों का जीवन बचाने की उसकी कोशिशें. यह सब सिनेमा के क्षेत्र में पहली बार घट रहा था और कलकत्ता इसके लिए संभवतः अभी तैयार नहीं था.
पाथेर पांचाली को शुरू के दो-तीन हफ्तों तक दर्शक ही नहीं मिले और तब तक नहीं मिले जब तक कलकत्तावासियों को विदेशों से आ रही फिल्म को लेकर प्रशंसात्मक खबरें नहीं मिलने लगीं. इसके बाद तो यह फिल्म कलकत्ता में १३ हफ्तों तक चली. इसने पहली बार बंगाली सिनेमा को पारसी थिएटर के प्रभाव से, जात्रा से और मेलोड्रामा से मुक्त किया.
बाद के दिनों में फेलिनी और बर्गमेन से अपनी तुलना किये जाने और लगातार उनकी ही तरह उच्च सौंदर्यशास्त्रीय मानकों को बनाये रखने में अक्षम रहने के बारे में एक सवाल का जवाब देते हुए राय ने कहा था कि फेलिनी और बर्गमेन को जैसे दर्शक मिले थे, वैसे मुझे नहीं. उनका कहना था-मैं जब फिल्म बना रहा होता हूं, तो पश्चिमी दर्शकों के बारे में नहीं सोचता. मैं अपने बंगाली दर्शकों को ध्यान में रखता हूं. मैं उन्हें अपने साथ लाने की कोशिश कर रहा हूं और इसे करने में मैं सफल रहा हूं....आपको उन्हें धीरे-धीरे अपने साथ लाना होगा. अगर कभी आप कंचनजंघा या अरण्येर दिन रात्रि की तरह छलांग लगायेंगे तो उन्हें खो देंगे....मैं उस तरह नहीं कर सकता जिस तरह बर्गमेन और फेलिनी ने किया. आप पायेंगे कि (बंगाल में) निर्देशक कितने पिछडे, कितने मूर्ख हैं, घटिया हैं और आप इस पर मुश्किल से भरोसा करेंगे कि उनकी फिल्में मेरी फिल्मों के साथ रख दी जाती हैं.'
सच में, राय की यह दिक्कत थी और इसका उन्होंने हमेशा ध्यान रखा.
राय की फिल्मों का विस्तार और उनका कैचमेंट एरिया कितना व्यापक है, इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि उन्होंने अपने समय के लगभग हर संभव विषय पर फिल्म बनायी. गांवों के जीवन पर उन्होंने पाथेर पांचाली, सद्गति और अशनि संकेत बनायी. मध्यवर्गीय जीवन पर महानगर और अरण्येर दिन रात्रि, उच्च वर्ग पर कंचनजंघा और घरे-बाइरे बनायी. अशिक्षित मजदूर वर्ग पर वे पोस्टमास्टर और सद्गति के साथ आये. अभियान और गणशत्रु, कलकत्ता के जीवन पर प्रतिद्वंद्वी और जन अरण्य, सुदूर अतीत पर देवी और चारूलता, जीवन में अतीत की स्मृतियों पर अपुर संसार और जलसाघर, तात्कालिक वर्तमान पर शाखा प्रशाखा और आगंतुक छोटे शहरी जीवन पर उनकी फिल्में हैं. उन्होंने एक ओर जहां पाथेर पांचाली और चारूलता जैसी करुण कथाओं को परदे पर प्रस्तुत किया तो पारस पत्थर और कापुरुष ओ महापुरुष जैसी शुद्ध कॉमेडी भी बनायी. इसी के साथ गोपी गाइन बाघा बाइन और हीरक राजार देशे जैसी फैेंटेसी भी रची. उन्होंने सोनार केल्ला और जय बाबा फेलूनाथ जैसी जासूसी कहानियों पर भी फिल्में बनायीं.
सत्यजीत राय में फिल्म निर्माण को लेकर उन्माद की हद तक उत्कृष्टता का आग्रह था. एक ही फिल्म में वे कला, बौद्धिकता, कारोबार, राजनीति, धर्म को इस तरह प्रस्तुत करते हैं और जटिल से जटिल दृश्यों की रचना करते हैं, त्रासदी से लेकर हास्य तक की स्थितियां पैदा करते हैं कि फिल्म अपने कथ्य का एक जीवंत संदर्भ ग्रंथ लगने लगती है. हर बार लगता है कि वे पूरी दुनिया के लिए और खुद अपने लिए भी लंबी और फिर एक और लंबी लकीर खींचते चले जा रहे हों. उनके समय के सभी महान फिल्मकार जल्दी ही चुक गये. डिसिका, रेने क्लेयर, विलिस, कुरासोवा, इसिकावा, कोबामाशी-सभी कुछेक फिल्में बनाने के बाद ही सिने परिदृश्य से ओझल होते गये. लेकिन सत्यजीत राय ने लंबे समय तक-लगभग चार दशकों तक-फिल्में बनायीं और उन्हें अंत तक नजरअंदाज नहीं किया जा सका. राय अपनी फिल्मों में बंगाली संस्कृति के इस कदर घुले-मिले होने के बावजूद एक सार्वभौमिक अपील लेकर प्रस्तुत होते हैं.
राय ने कभी विदेशी दर्शकों को ध्यान में रख कर कोई फिल्म नहीं बनायी बल्कि वे इस मानसिकता की आलोचना ही करते रहे कि भारतीय फिल्मकार पूरब के प्रति पश्चिम के आकर्षण की दलाली करने में लग जायें. और इसीलिए वे इतनी बेहतरीन फिल्में बना पाये, जो भारत की और खास कर बंगाली समाज की एक ही साथ जडता को और उसके टूटन को, उसकी आकांक्षा को और उसके अंतद्वंद्व को प्रदर्शित कर पाये.
राय पूरी दुनिया में स्वीकारे गये और राय ने पूरी दुनिया को स्वीकार किया. उन्होंने नव यथार्थवादी सिनेमा की वैश्विक परंपरा में खुद शामिल किया और उसकी जमीन पर बंगाली संस्कृति को रूपायित किया. जब पहली बार उन्होंने बाइसिकल थीव्स देखी थी, उन्होंने तय किया कि जब वे पाथेर पांचाली बनायेंगे तो उसे ठीक इसी तरह बनायेंगे. लेकिन राय की संश्लेषणात्मक क्षमता कितनी समृद्ध थी, इसका अंदाजा लगाने के लिए बाइसिकल थीव्स और पाथेर पांचाली को एक बार फिर एक साथ देखा जा सकता है. उनमें क्या समानता हैङ्क्ष
एक भी समानता नहीं, सिवाय इसके कि दोनों वास्तविक लोकेशनों पर बनायी गयी हैं और दोनों के कलाकार एकदम अनजान लोग हैं.
सत्यजीत राय ने फिल्म निर्माण का क्रमशः पूरा काम खुद अपने ऊपर ले लिया. पटकथाएं तो वे लिखते ही थे, कॉस्टूम और सेट निर्माण में भी उनकी मुख्य भूमिका रहती. वे छोटे विवरणों तक पर बारीकी से ध्यान देते. शूटिंग के दौरान कैमरा भी खुद ही चलाते और खुद हरेक फ्रेम को संपादित करते. उन्होंने अपनी अधिकतर फिल्मों का संगीत भी खुद ही कंपोज और रिकार्ड किया है. ऐसा वे न सिर्फ अपना बजट कम रखने के लिए करते, बल्कि वे यह चाहते थे कि उनकी फिल्म पूरी तरह उनकी हो.

राय ने अपने प्रस्तुति कौशल में बहुत ज्यादा परिवर्तन नहीं किये. इसलिए उनकी फिल्में चौंकाती नहीं हैं, बल्कि वे परिवेश के स्तर पर बहुत जानी-पहचानी लगती हैं. लेकिन प्रस्तुति के स्तर पर वे एकदम नयापन लिये हुए होती हैं. उनका काम हमेशा परिपूर्ण होता. उनकी फिल्में प्रायः एक कसे हुए उपन्यास या कविता की तरह हैं, बहुत कुछ महाकाव्यात्मक उपन्यास की तरह. उनकी फिल्में देखते हुए फणीश्वरनाथ रेणु, शोलोखोव या गोपीनाथ महांती के उपन्यास याद आ जाते हैं. ताराशंकर वंद्योपाध्याय भी उनमें से एक हैं और सत्यजीत राय ने उनकी कहानी जलसाघर पर फिल्म भी बनायी.
प्रायः सत्यजीत राय में दर्शकों को किसी युक्ति या घटना से चकित करने की प्रवृत्ति नहीं मिलती. घटनाएं उनके यहां एक प्रक्रिया के बतौर आती हैं और इसलिए दर्शक प्रायः यह समझ लेता है कि आगे क्या होनेवाला है. पाथेर पांचाली में जब इंदिर ठाकरुन सर्वजया से अंतिम बार सुलह की कोशिश करती है और नाकाम रहती है तथा बेहद हताश कदमों से फ्रेम से बाहर जाती हुई दिखती है, दर्शक के लिए यह यकीन कर पाना बेहद मुश्किल होता है कि अब इंदिर ठाकरुन किसी फ्रेम में दोबारा बोलती हुई दिखेगी.
इसी तरह घरे बाइरे के अंतिम हिस्से में, जब विमला के मना करने के बावजूद निखिलेश्वर घोडे पर बैठ दंगाग्रस्त गांवों की ओर चला जाता है और विमला खिडकी के पास खडी दिखती है, हम यह सोचने के लिए कोई आधार नहीं पाते कि निखिलेश्वर अब लौट भी पायेगा. यहां तक कि इसी फिल्म में जब संदीप पहली बार विमला का चुंबन लेता है, तब भी दर्शक नहीं चौंकते. वह अपने प्रवाह में बेहद स्वाभाविक लगता है.
ऐसा करना सत्यजीत राय को नाटकीय और अतार्किक होने से दूर ले जाता है. वे घटना को विकसित होने और स्थापित होने के लिए उसे पूरा समय देते हैं. हर बार वे प्रक्रिया को पूरी होने देते हैं, उसे बीच से काटते नहीं. पाथेर पांचाली के अंत में जब अपु दुर्गा की पुरानी चीजों में वह माला पाता है, जिसकी चोरी के आरोप में कभी दुर्गा ने बहुत मार खायी थी, लेकिन दुर्गा ने चोरी को कभी स्वीकार नहीं किया था. अपु अपनी मृत बहन का सम्मान बचाये रखने के लिए उसे तालाब में फेंक देता है. माला डूबने के बहुत देर बाद तक कैमरा वहां स्थिर रहता है जहां से माला पानी के भीतर गयी है. दर्शक (और अपु भी) कई सेकेंडों तक पानी को स्थिर होती काई को फिर से आपस में मिलते देखते हैं.
हालांकि घरे बाइरे के तीनों चुंबन दृश्य भी कुल मिला कर चौंकानेवाले ही हैं, इस अर्थ में कि सत्यजीत राय के यहां वे पहली बार घटित होते हैं. सत्यजीत राय प्रायः अंतरंग दृश्यों से बचते रहे हैं. इसलिए घरे बाइरे के ये दृश्य वास्तव में थोडी देर के लिए चकित कर देते हैं. लेकिन दुर्भाग्य से ये सत्यजीत राय की किसी भी फिल्म के सबसे कमजोर दृश्य भी हैं. ये न सिर्फ फिल्म की गति से मेल नहीं खाते, बल्कि सत्यजीत राय की अपनी स्वाभाविक गति और वर्णनशैली से मेल नहीं खाते और असहज लगते हैं.
सत्यजीत राय ने कभी अकेले संवादों को उतनी अहमियत नहीं दी, जितनी दूसरे फिल्मकार देते हैं. उनके संवाद पूरे दृश्यबंध के साथ जुडे होते हैं-उन्हें अभिनय, वातावरण, संगीत और प्रकाश के साथ संगत करनी होती है. इस क्रम में कई बार वे अधूरे भी छोड दिये जाते और कहने की जरूरत नहीं कि वे तब और अधिक प्रभावशाली हो जाते है. पाथेर पांचाली और अभियान से दो दृश्य. हरिहर लौटने पर एक साडी सर्वजया को देने की कोशिश करता है और बताता है कि यह दुर्गा के लिए है, सर्वजया की पीडा का मानो विस्फोट हो जाता है. इसके बाद कोई संवाद नहीं है. होंठ हिलते हैं, लेकिन सुनाई सिर्फ संगीत पडता है. हरिहर के लिए यह स्पष्ट हो जाता है कि दुर्गा नहीं रही. उस दृश्य को बार-बार देखा जा सकता है, जब हरिहर दुर्गा की मृत्यु की खबर की पीडा से परिचित हो रहा है. वह आधी ऊंचाई तक उठता है और फिर बैठ जाता है. लगभग आधी गति से चलती फिल्म के दौरान यह यह दृश्य इतना प्रभावकारी है कि यह आपको बिना विचलित किये नहीं रह सकता. राय अपनी आगे की किसी भी फिल्म में ऐसा दृश्य नहीं रच पाये.
इसी तरह अपराजितो का युवा नायक जब अपनी मां को देहात में छोड कर पढाई के लिए कलकत्ता जाने लगता है तो भावनाएं इतनी सघन हो जाती हैं कि दर्शक सत्यजीत राय की भावनाओं की नदी में खुद को डूबता हुआ महसूस करते हैं. हम राय से उदास होना सीखते हैं और खुश होना भी. वे हमें संस्कारित करते हैं.
दूसरा उदाहरण अभियान से. टैक्सी चालक नरसिंह एक ईसाई युवती नीली से प्यार करता है, लेकिन नीली एक ईसाई पादरी से प्यार करती है और यह बात नरसिंह नहीं जानता. जब नीली पढाई जारी रखने और शादी के लिए उस पादरी युवक के साथ कलकत्ता भागने में नरसिंह से मदद मांगती है, तो वह अवाक रह जाता है. उसके अंदर बहुत कुछ टूटता है, जो उतने अंधेरे में किसी दूसरे फिल्मकार के यहां दिखायी नहीं भी दे सकता था, लेकिन सत्यजीत राय इसे इस तरह दिखाते हैं कि कुछ भी नही बचता. नीली के संवादों को ओवरलैप करता हुआ और उन्हें अधूरा छोडता हुआ सत्यजीत राय का संगीत दृश्य पर छा जाता है और उसमें हम उस टैक्सी ड्राइवर की वेदना को महसूस करते हैं, जो उस ईसाई युवती से अंगरेजी सीखना चाहता था और चाहता था कि नीली उसका और अपना नाम एक दीवार पर लिख जाये.
सत्यजीत राय की सिनेयुक्तियां जितनी संप्रेषणीय हैं, उतनी ही जटिल भी. बल्कि जहां वे जटिल हैं, वहीं बहुत सहज हो पायी हैं. वे बहुत अनूठी-अनोखी नहीं हैं, फिर भी हर बार वे नयी लगती हैं.
एक उदाहरण फिर से अभियान के उसी प्रसंग से. भागनेवाली रात से पहले दिन में नीली नरसिंह को रात में दस बजे एक जगह आने को कहती है. समय पर नरसिंह पहुंच जाता है. परदे पर अंधेरा है और एकदम धुंधली छाया है नरसिंह के सिर की. अंधेरे में उसकी व्यग्रता दिखाती है बार-बार घडी पर पडती उसके टार्च की रोशनी और उसके सिगरेट की आग. इसी दृश्य में आगे जब नरसिंह दोनों को लेकर गाडी से जाने लगता है तो हेडलाइट की रोशनी बडी होते-होते पूरे दृश्यक्षेत्र पर छा जाती है और अंधेरे के बरअक्स पूरा परदा रोशनी में नहा जाता है.
एक दूसरा दृश्य. पाथेर पांचाली के अंतिम हिस्से में जब हरिहर के घर में एक सांप घुसता हुआ दिखता है. यह दृश्य देर तक परदे पर चलता है. इसके बाद अगला दृश्य दिखता है-बैलगाडी पर हरिहर सर्वजया और अपु के साथ गांव छोड कर जा रहा है. घर उजडने को प्रतिबिंबित करता हुआ खाली घर में घुसते हुए सांप का प्रतीक भारतीय दर्शकों के लिए उतना नया नहीं है फिर भी सत्यजीत राय का कैमरा इसे ऐसे प्रस्तुत करता है कि यह पहले देखा-सुना नहीं लगता.
सत्यजीत राय के फिल्मों में पार्श्व दृश्य ऐसे नहीं हैं, जो फिल्मांकन करते वक्त पात्रों के पीछे विवशता में आ गये हैं. वे जीवंतता से भरे हैं. पानी से भरे धान के खेत, तालाबों की लहरें, लंबे पेड और खेतों में चलते हुए हल...सब कुछ जीवन से भरपूर लगते हैं.
राय की फिल्म में रेलगाडियां एक अलग महत्व रखती हैं. वे प्रायः उनकी हर दूसरी फिल्म में किसी ने किसी रूप में मौजूद हैं. पाथेर पांचाली से लेकर अपराजित, अरण्येर दिन रात्रि, नायक, जय बाबा फेलुनाथ, अभियान, रवींद्रनाथ टैगोर...सारी फिल्मों में रेलगाडियां आती हैं. और वे किसी क्रॉसिंग पर खडे सवारियों से परिचय जैसा परिचय नहीं करतीं, वे पूरे समारोहपूर्वक दाखिल होती हैं, आत्मीयता से उनसे मिलती हैं और होड तक करती हैं. सत्यजीत राय अपनी अधिकतर फिल्मों में कहानियों की अंतर्धारा को जोडने के लिए भी रेलगाडियों या उनकी आवाज का इस्तेमाल करते हैं.
सत्यजीत राय जब-जब जटिल दृश्यों का निर्माण करते हैं, अत्यधिक सफल नजर आते हैं. जहां-जहां उन्होंने सामान्य होने की कोशिश की है, वहां वे प्रभावहीन लगते हैं.
उनका दृश्य, संगीत, प्रकाश समायोजन इतना व्यवस्थित और सब कुछ पहले से, फिल्म निर्माण शुरू होने से भी पहले से, इस तरह तय किया हुआ और आपस में गुंथा हुआ होता था कि उनमें से एक दृश्य, एक संवाद, एक धुन, प्रकाश की एक रेखा तक नहीं कम कर सकते. फिर तो पूरी फिल्म भरभरा कर गिर पडेगी.
सत्यजीत राय की फिल्मों की गति की तुलना सिर्फ महान इतालवी फिल्मकार माइकेलएंजेलो एंटोनियोनी से की जा सकती है, लेकिन एंटोनियोनी जहां एक बुर्जुआ जीवन की यांत्रिकता, एकांतिकता, त्रास, स्वार्थपरता और भटकाव को रूपायित करते हैं, सत्यजीत राय सामूहिक पिछडेपन, सामंती गतिहीनता को (एक गहरे व्यंग्य और अवहेलना के साथ) चित्रित करते हैं. दोनों के यहां समय बहुत धीरे गुजरता है, साधारण जीवन की गति की हद तक आकर, लेकिन फिर भी दोनों में बुनियादी अंतर मौजूद हैं. राय अपने साथ अपनी संस्कृति की ऊष्मा लेकर चलते हैं. वह एंटोनियोनी की तरह अपने समाज के नीरस जीवन को चित्रित करने के लिए अभी अभिशप्त नहीं हुए हैं.
राय की फिल्मों के दृश्य और चरित्र कभी वास्तविक जीवन से अधिक भव्य नहीं लगे. इसके लिए कथा वस्तु एवं दृश्य समायोजन के अलावा राय ने तकनीकी सावधानियां भी बरतीं. उनके कैमरों-पुराना मिशेल, आइमो और वाल कैमरा-के लेंस ४० एमएम के रहते. यह मानवीय दृष्टि के सबसे नजदीक पडता है. इसके अलावा राय को क्लोजअप और वाइडएंगेल से लगभग नफरत थी. वे बेहद सुंदर लगनेवाले शॉट्स को भी नकार देते थे, अगर वह पूरी फिल्म की दृश्ययोजना में न आये. राय ने अर्थाभाव के कारण फिल्में कम खर्च कीं. उनके साथ कई फिल्मों में काम कर चुकीं वहीदा रहमान ने उन्हें याद करते हुए यह रेखांकित किया है कि राजकपूर और के आसिफ जैसे फिल्मकारों की तरह-जो १२-१८ हजार फुट की फिल्म के लिए ३५ हजार फुट फिल्म तक की शूटिंग करतेथे- सत्यजीत राय ऐसा सोच भी नहीं सकते थे.
अपनी सभी फिल्मों में चिडियाखाना राय को सर्वाधिक अप्रिय थी. यह वास्तव में उनके एक सहकर्मी को बनानी थी, जो वक्त आने पर उसे न बना सका और जिसे बिना तैयारी के राय को बनाना पडा. राय कहते थे कि अगर उन्हें अपनी कोई फिल्म दोबारा उसी तरह बनानी हो तो वे चारूलता को चुनेंगे. वे उससे पूरी तरह संतुष्ट थे.
राय पर प्रायः रवींद्रनाथ टैगोर का प्रभाव माना जाता है. वे इसके अलावा वे विभूतिभूषण वंद्योपाध्याय से भी प्रभावित रहे. लेकिन एक फर्क स्पष्ट दिखता है, जब वे विभूतिभूषण की रचनाओं पर फिल्में बना रहे होते हैं. ऐसा करते वक्त वे टैगोर के प्रभाव से थोडा बाहर निकलने में सफल रहते हैं. टैगोर का प्रभाव उन पर सबसे अधिक घरे बाइरे बनाते वक्त रहा है क्योंकि इसमें निखिलेश्वर के रूप में खुद टैगोर मौजूद हैं.
लेकिन ट्रीटमेंट के लिहाज से सत्यजीत राय दोस्तोयव्स्की के अधिक नजदीक दिखते हैं. उनकी फिल्मों में खलनायक या नकारात्मक पात्र नहीं हैं. एकदम पवित्र और मासूम से दिखनेवाले चरित्रों की शुरुआत पाथेर पांचाली से होती है और कमोबेश उनकी अंतिम फिल्म आगंतुक तक चलती है. लंबे समय तक उनकी फिल्मों के पात्र अपु की छवि का एक अंश लिये होते हैं-दोस्तोयव्स्की के रस्कोल्निकोव या गोपीनाथ महांती के रवि (माटी मटाल) की तरह. हालांकि घरे बाइरे में संदीप की सकारात्मकता फिल्म के उत्तरार्ध में जरूर भंग हुई है और अंत आते-आते, विमला के मोहभंग होने से पहले ही वह अपने प्रति दर्शक की सहानुभूति खो बैठता है, फिर भी वह न तो नकारात्मक चरित्र है और न खलनायक. संदीप प्रकटतः हिंदू-मुसलिम दंगों के लिए दोषी लगता सकता था, लेकिन इसके बावजूद राय का ट्रीटमेंट उसे ऐसा होने से बचा लेते हैं. हालांकि थोडा सचेत रहें, तो हम संदीप और उसकी राजनीति में आज के नरेंद्र मोदी मार्का संघी राजनीति को बीज रूप में पा सकते हैं.
राय की फिल्मों में त्रासदी है और इस त्रासदी को अपनी झुकी हुई पीठों पर ढोते हुए लोग हैं. राय के यहां कोई एक आदमी या एक संस्था दोषी नहीं दिखता. वे स्थितियों और परिघटनाओं का इतना सरलीकरण नहीं करते और न समाधानों को इतना सामान्यीकृत करते हैं कि सारा दोष एक व्यक्ति में दिखा कर उसे दंडित करके मध्यवर्गीय चेतना को आत्मतुष्ट किया जा सके और उसे अपराधबोध से मुक्त कर दिया जाये. इसके बरअक्स राय एक के बाद एक त्रासदियों का प्रवाह सामने लेकर आते हैं और इसके लिए विवश करते हैं कि दर्शक अपनी तार्किक दृष्टि से कारणों की पडताल करे और समाधान तक पहुंचे.
राय में काफी हद तक समकालीन सवालों पर उनका कैमरा मौन रहा है. १९४६-४७ के दंगे, जिन्होंने उस बंगाल को सर्वाधिक प्रभाविक किया, जिसमें राय रह रहे थे और १९६७ का नक्सलबाडी आंदोलन जिसने चलते ट्रामोंवाले शहर कलकत्ता को क्रांतिकारी हलचलों से भर दिया था, राय के यहां अनुपस्थित है. राय पर उनके समकालीन और उनके बाद उभरे ऋत्विक घटक और मृणाल सेन की फिल्मों के जरिये अप्रत्यक्ष दबाव बढ रहा था कि वे समकालीन प्रश्नों पर अपनी सिनेमाई चुप्पी तोडें. राय पर इसका प्रभाव पडा भी पडा और उन्होंने समकालीन मुों पर भी फिल्में बनायीं, लेकिन यहां भी लय उनकी अपनी ही थी. प्रतिद्वंद्वी और सीमाबद्ध जैसी फिल्में समकालीन राजनीतिक प्रश्नों से रू-ब-रू होती हैं. प्रतिद्वंद्वी में वे नक्सलवादी आंदोलन को दृश्यक्षेत्र में लाते हैं, लेकिन सिर्फ एक सीमा तक. इसके बावजूद फिल्म बेहद प्रभावशाली है. इसे राय ने अपनी सबसे उकसावेवाली फिल्म कहा है. फिल्म में सीधे आंदोलन को चित्रित भले न किया गया हो, लेकिन दूसरे पात्रों के जरिये स्थितियों का जिस तरह निरूपण किया गया है और चरित्रों को घटनाओं के प्रवाह से गुजारा गया है, वह इस आंदोलन के प्रति राय के दृष्टिकोण को रेखांकित करता है. राय ने उन शुरुआती दिनों में ही इस आंदोलन की जडों और कारणों के संकेत देते दिखते हैं.
समकालीन राजनीतिक प्रश्नों पर फिल्में बनाने को लेकर सत्यजीत राय ने सतर्कता बरती. उनका कहना था कि उन्हें फिल्मों के सेंसर से पास नहीं होने का डर था, इसलिए उन्होंने सीधे चित्रण से परहेज किया. इसके बावजूद उन्होंने इस सवालों के अक्षुण्ण रहने दिया हो ऐसा नहीं है. वे हीरक राजार देशे का नाम लेते हैं. वे कहते हैं कि इसके एक दृश्य में जिस तरह गरीबों को भगाया गया है, वह दरअसल आपातकाल के दौरान दिल्ली और दूसरे शहरों में गरीबों के साथ हुए व्यवहार को दिखाने का उनका तरीका था. वे कहते थे कि आप सीधे सत्ताधारी पार्टी पर हमला नहीं कर सकते. ऐसा करने पर फिल्म 'किस्सा कुरसी का' की तरह नष्ट कर दी जा सकती है. इसलिए अपनी सीमा में रहते हुए भी आप उन सवालों को उठा सकते हैं.
उनका मानना था कि सत्ता को टारगेट करना तो आसान है, लेकिन ऐसा करके आप ऐसे लोगों पर हमला कर रहे होते हैं, जिन्हें इससे बहुत फर्क नहीं पडता. आपके कहने के बाद भी सत्ता का कुछ नहीं बिगडता. सत्यजीत राय का मानना था कि फिल्में समाज को बदल नहीं सकतीं. वे कहते हैं-'क्रांति के दरमियान फिल्मकार एक सकारात्मक भूमिका रखता है, वह क्रांति के लिए कुछ कर सकता है. लेकिन यदि क्रांति हो ही नहीं रही हो तो वह कुछ नहीं कर सकता.'
राय का मानना था कि नक्सलवादी आंदोलन की तरह क्रांतिकारी गतिविधियों पर सेर्गेई आइजेंस्टाइन की तरह फिल्म बनायी तो जा सकती है, लेकिन भारत की वर्तमान परिस्थितियों में यह संभव नहीं है.
राय की फिल्मों में आलोचकों को हताशा, गरीबी और उजाड ही दिखता है. राय के पास इसके लिए अपनी तरह का जवाब था-'जब आप समस्याओं के बारे में फिल्म बना रहे हों और आपके पास समाधान न हो तो फिल्म निश्चित तौर पर हताशाभरी होगी.' वे कहते हैं-'आप हर समय खुशियों भरी फिल्में नहीं बना सकते.'
राय का निधन २३ अप्रैल, १९९२ को हुआ. यह वही दिन था, जब १६१६ में शेक्सपीयर का निधन हुआ था. कई मायनों में सत्यजीत राय शेक्सपीयर जैसे लगते हैं. उनकी फिल्मों में भावनाओं की सघनता शेक्सपीयर की ही तरह थी. परिवेश, काल, शैली और मूड की खास व्यापकता, उनका विस्तार और असाधारणता, सब कुछ उन्हें रूपहले परदे का शेक्सपीयर बनाती है.
आधी सदी से अधिक समय गुजरने के बाद भी राय का एक-एक फ्रेम हमारे परिवेश को, आज के परिवेश को एक बेचैन कर देनेवाली जडता के साथ प्रस्तुत करता है. पाथेर पांचली में सर्वजया एक जगह कहती है-'अपु पढ लिख जाये, दुर्गा के लिए एक अच्छा वर मिल जाये और हमें दो वक्त का भोजन...'
सर्वजया भारत की सौ करोड आबादी में से बहुमत का प्रतिनिधित्व करती है, आज भी. आज भी उसके लिए ये सपने पूरे नहीं हो सके हैं. टूटते, बिखरते और सामंतवाद की चक्की में पिसते उनके गांव आज भी एक यथार्थ हैं. हम पाते हैं कि समय गुजरने के साथ पूरा भारत ही राय के फ्रेमों में दाखिल हो गया है. और इसीलिए आज भी, राय भारत की गरीबी और निर्मम विपन्नता के सबसे बडे सिनेप्रवक्ता हैं.
अंत में, अरुंधति राय के शब्दों का इस्तेमाल करते हुए कहें तो कहा जा सकता है कि सत्यजीत राय एक ऐसे निर्देशक थे, जिन्हें दुनिया की श्रेष्ठतम फिल्मों में से कुछ ने अपने लिए चुन लिया था.