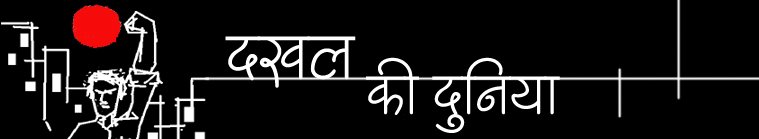कैद में अधिकार:-
डॉक्टर और असाधारण मानवाधिकारकर्ता डॉ बिनायक सेन को छत्तीसगढ़ सरकार ने पिछले नौ महीनों से अमानवीय कानूनों की आड़ में सलाखों के पीछे रखा हुआ है. उनकी कहानी दरअसल उस दरकती हुई जमीन की कहानी है जिसपर हमारे लोकतांत्रिक अधिकारों की इमारत टिकी है. शोमा चौधरी की रिपोर्ट साभार तहलका.
दिल्ली और मुंबई की भव्यता से परे, चमचमाते मॉल्स और हिचकोले खाते शेयर बाजार की सुर्खियों से कहीं दूर एक भला इंसान जेल में अपनी रिहाई का इंतजार कर रहा है. उसके बारे में थोड़ी-बहुत खबरें आई हैं. कुछ अखबारों में, कुछ टीवी चैनलों पर. फिर भी जादू-टोने, तंत्र-मंत्र, चमत्कार, बाजार, फिल्मस्टार, एसएमएस पोल आदि से अभिभूत मीडिया में अगर डॉ बिनायक सेन का जिक्र हुआ भी होगा तो इस बात के आसार कम ही हैं कि उसने आपका ध्यान खींचा हो.
बिनायक सेन की कहानी दरअसल उस दरकती हुई जमीन की कहानी है जिस पर हमारे लोकतांत्रिक अधिकारों की इमारत खड़ी है. ये कहानी है भारत के लोक और तंत्र, शहर और गांव, विकास और इंसानी जरूरतों, अंधे कानून और प्राकृतिक न्याय के बीच आ चुकी और बढ़ रही दरार की. ये उस भारत की कहानी है जिसे जोड़ने वाली डोरी धीरे-धीरे कमजोर होती जा रही है. ये उस अन्याय की दास्तान भी है जो हजारों निर्दोष लोगों के साथ होता है और जिसकी खबर किसी को नहीं लगती. ये उस बेइंसाफी का सच भी है जो कल आपके और मेरे साथ होने का इंतजार कर रही है. और सबसे ज्यादा ये उस डरावनी हकीकत का पर्दाफाश करने वाली दास्तान है कि जब सरकार खुद को ही खतरे में बताने लगे तो साधारण लोगों के साथ क्या हो सकता है. पढ़ाई पूरी करने के बाद इस प्रतिभाशाली नौजवान के सामने करिअर के शानदार विकल्प थे. वो विदेश जा सकता था या फिर यहीं ऊंची तनख्वाह वाली कोई नौकरी कर बढ़िया जिंदगी गुजार सकता था. मगर उसने एक ऐसी मुश्किल राह चुनी जिस पर चलने की हिम्मत कम ही लोग करते हैं.
मगर सबसे पहले कहानी के तथ्य.
पेशे से बच्चों के डॉक्टर और जाने-माने क्रिश्चियन मेडिकल कॉलेज (सीएमसी), वेल्लोर से गोल्ड मेडेलिस्ट, 56 वर्षीय बिनायक सेन वो शख्स हैं जिन्होंने छत्तीसगढ़ के गरीब आदिवासियों के बीच में कुपोषण, टीबी और घातक मलेरिया से लड़ते हुए लगभग तीन दशक बिताए हैं. पढ़ाई पूरी करने के बाद इस प्रतिभाशाली नौजवान के सामने करिअर के शानदार विकल्प थे. वो विदेश जा सकता था या फिर यहीं ऊंची तनख्वाह वाली कोई नौकरी कर बढ़िया जिंदगी गुजार सकता था. मगर उसने एक ऐसी मुश्किल राह चुनी जिस पर चलने की हिम्मत कम ही लोग करते हैं. सेन ने छत्तीसगढ़ के होशंगाबाद में एक ईसाई संस्था द्वारा चलाए जा रहे ग्रामीण चिकित्सा केंद्र में अपनी सेवाएं देने का फैसला किया. यहां वो महात्मा गांधी के जीवनी लेखक मारजोरी साइकस से काफी प्रभावित हुए. उनके दिल में जनस्वास्थ्य, पर्यावरण के अनुकूल विकास और न्यायमूलक समाज का सपना पलने लगा. पढ़ाई के दौरान वेल्लोर की झुग्गियों में भ्रमण करते हुए सेन को ये अहसास हो गया था कि आजीविका, रहन-सहन और स्वास्थ्य में एक अहम संबंध है. इसका और गहराई से अध्ययन करने के लिए उन्होंने जवाहर लाल नेहरू विश्वविद्यालय से सोशल मेडिसिन में डिग्री ली और 1981 में होशंगाबाद में खान मजदूर संघ के मशहूर नेता शंकर गुहा नियोगी के साथ काम करने चले आए. यहां उन्होंने दालिराजहारा में शहीद अस्पताल की स्थापना में मदद की जिसे मजूदरों ने अपने पैसे से बनाया था. बाद में वो तिल्दा के मिशन हॉस्पिटल से जुड़ गए. 1990 में सेन ने अपनी पत्नी इलिना सेन के साथ रायपुर में रूपांतर नाम के एक एनजीओ की स्थापना की. पिछले 18 सालों से ये संगठन ग्रामीण स्वास्थ्यकर्मियों को प्रशिक्षण देने और सुदूर इलाकों में मोबाइल क्लीनिक चलाने का काम कर रहा है. वो पीपुल्स यूनियन फॉर सिविल लिबर्टीज(पीयूसीएल) नाम के मानवाधिकार संगठन से भी जुड़े जिसकी स्थापना जयप्रकाश नारायण ने की थी.
बिनायक सेन का काम कितना असाधारण है इसका अंदाजा आपको तब होता है जब आप रायपुर से डेढ़ सौ किलोमीटर दूर धमतरी जिले में जंगलों से घिरे बागरुमाला और साहेलबेरिया इलाकों में जाते हैं. यहां आकर आपको ये अहसास होता है कि एक रिटायर कर्नल के होनहार बेटे को असाधारण जुनून ही ऐसी जगह पर ला सकता था. इस इलाके में बसे छोटे-छोटे गांवों में कमार और दूसरी जनजातियों के वो लोग बसते हैं जिनका शुमार भारत के सबसे उपेक्षित लोगों में किया जा सकता है. यहां सेन अपना मंगलवार क्लीनिक चलाते थे. स्कूल, पीने के पानी, बिजली, स्वास्थ्य सुविधाओं से महरूम और अपने जंगल के परंपरागत संसाधनों से लगातार वंचित किए जा रहे इन लोगों की जुबान पर बिनायक सेन की कई कहानियां हैं. उदाहरण के लिए लोग बताते हैं कि कैसे सेन ने लग्नी की जान बचाई जिसका गर्भपात हो गया था और उसका खून रुकने का नाम नहीं ले रहा था. या किस तरह उन्होंने वन अतिक्रमण के आरोप में सामूहिक रूप से जेल में डाल दिए गए पिपरही भारही गांव के लोगों को बचाया. या फिर कैसे उन्होंने अनाज बैंकों की स्थापना में मदद की. कमार बस्ती में एक वृद्ध हमसे कहते हैं, “कुछ कीजिए. डॉक्टर को बचाइये. अब कोई ऐसा नहीं है जिसके पास हम जा सकें.”
सीएमसी वेल्लोर के निदेशक डॉ. सुरंजन भट्टाचार्य कहते हैं, “बिनायक ने एक अलग राह बनाई. वो डॉक्टरों की कई पीढ़ियों के लिए प्रेरणास्रोत हैं. उन्होंने हमारी अंतरात्मा को झिंझोड़ा. उन्होंने हमें याद दिलाया कि एक स्वस्थ समाज बनाने के लिए आजादी, खाद्य सुरक्षा, आश्रय, समानता और न्याय जैसी कई चीजों की जरूरत होती है.” 2004 में सीएमसी वेल्लोर ने सेन को अपने प्रतिष्ठित पॉल हैरीसन अवार्ड से सम्मानित किया. इसमें सेन की प्रशंसा में ये शब्द कहे गए थे, “डॉ. बिनायक सेन सत्य और सेवा के प्रति अपने समर्पण को लड़ाई के अग्रिम मोर्चे तक ले गए हैं. उन्होंने सांचों को तोड़ा है और अपने मकसद को अपनी सुरक्षा से ऊपर रखकर एक बिखरे और अन्यायपूर्ण समाज में एक डॉक्टर की संभावित भूमिका को फिर से परिभाषित किया है. सीएमसी को बिनायक सेन से जुड़े होने पर गर्व है.”
इसके बावजूद, तीन साल बाद 14 मई 2007 को राज्य सरकार ने एक मानवाधिकारकर्ता और डॉक्टर के रूप में किए गए बिनायक सेन के लंबे और समर्पित कार्य को अनदेखा कर दिया. पुलिस ने पहले तो उन्हें नक्सली नेता घोषित कर दिया और बाद में गिरफ्तार कर लिया. उन पर आपराधिक षडयंत्र, राष्ट्रदोह और आतंक के ज़रिए मिले पैसे का इस्तेमाल करने के आरोप लगाए गए. सेन की गिरफ्तारी के बाद से तीन अदालतें उन्हें जमानत देने से इनकार कर चुकी हैं. सुप्रीम कोर्ट ने 10 दिसंबर 2007 को सेन को जमानत देने से इनकार कर दिया. ये भी विडंबना ही है कि इस दिन अंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस था. अदालत में जिरह के दौरान अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल गोपाल सुब्रमण्यम और छत्तीसगढ़ सरकार के वकील का तर्क था कि भारत सरकार, बिहार, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र में उग्रवाद की जांच कर रही है और बिनायक सेन इस नेटवर्क का एक अहम हिस्सा हैं. उनका कहना था कि सेन को ज़मानत देने से देश की सुरक्षा खतरे में पड़ सकती है. इस दावे के पक्ष में हास्यास्पद सबूत पेश किए गए. लोग बताते हैं कि कैसे सेन ने लग्नी की जान बचाई जिसका गर्भपात हो गया था और उसका खून रुकने का नाम नहीं ले रहा था. या किस तरह उन्होंने वन अतिक्रमण के आरोप में सामूहिक रूप से जेल में डाल दिए गए पिपरही भारही गांव के लोगों को बचाया. या फिर कैसे उन्होंने अनाज बैंकों की स्थापना में मदद की. कमार बस्ती में एक वृद्ध हमसे कहते हैं, “कुछ कीजिए. डॉक्टर को बचाइये. अब कोई ऐसा नहीं है जिसके पास हम जा सकें.”.
बिनायक सेन के व्यक्तित्व और चरित्र का अंदाजा उनके बारे में लोगों के विचारों से भी लगाया जा सकता है. जब सुप्रीम कोर्ट ने सेन को जमानत देने से इनकार कर दिया तो उनके समर्थन में उमड़ी एक रैली में मौजूद एक वृद्ध का कहना था, “अगर अदालत ने हमारे डॉक्टर को नहीं छोड़ा तो हम जेल तोड़ देंगे. मगर क्या फायदा? सारे कैदी भाग जाएंगे और डॉ बिनायक फिर भी वहीं रहेंगे.”
इसके बावजूद सेन के शुभचिंतकों की तमाम कवायदें भी उन्हें जमानत नहीं दिला सकीं. न एम्स और सीएमसी के उन डॉक्टरों के शपथपत्र जो सेन से प्रेरणा लेकर उनकी राह चल निकले हैं और न ही दुनिया भर के 2000 डॉक्टरों के हस्ताक्षर. ये भी गौरतलब है कि सेन जनस्वास्थ्य पर सरकार द्वारा बनाई गई सलाहकार समिति के भी सदस्य रह चुके हैं. विडंबना देखिये कि सेन के गिरफ्तार होने के सात महीने बाद 31 दिसंबर 2007 को इंडियन अकेडमी ऑफ सोशल साइंसेज ने उन्हें आर आर खेतान गोल्ड मेडल से सम्मानित किया गया. अकेडमी ने डॉ बिनायक सेन के काम की तुलना राष्ट्रपिता महात्मा गांधी द्वारा प्रचारित मूल्यों से की.
क्या ऐसे आदमी को जेल में ठूंसना अन्याय नहीं है. छत्तीसगढ़ पुलिस के डीजीपी विश्व रंजन जवाब देते हैं, “तो क्या हुआ? क्या कोई मानवतावादी और आदर्शवादी, माओवादी नहीं हो सकता.” समझा जा सकता है कि राज्य सरकार के काम करने का तरीका क्या है.
सबसे ज्वलंत सवाल ये है कि बिनायक सेन को गिरफ्तार क्यों किया गया? ऐसा क्या हुआ कि सरकार के लिए उनकी पहचान बदल गई और उन्हें सलाखों के पीछे ठूंस दिया गया? एक नजर डालते हैं.
दो साल पहले जनवरी 2006 में आंध्र प्रदेश के भद्राचलम में नारायण सान्याल नाम के एक माओवादी नेता को गिरफ्तार किया गया. 67 साल के सान्याल हाथ में गंभीर दर्द की एक बीमारी से पीड़ित थे जिसे चिकित्सा विज्ञान की भाषा में पामर्स कांट्रेक्चर कहा जाता है. जब सान्याल को वारंगल जेल से जमानत मिल गई तो जेल अधिकारियों ने उन्हें इस बीमारी का इलाज कराने की इजाजत दे दी. इसके तुरंत बाद छत्तीसगढ़ पुलिस ने उन्हें दंतेवाड़ा में हुए एक कत्ल के आरोप में गिरफ्तार कर लिया और रायपुर जेल में डाल दिया. मई 2006 में कोलकाता में रह रहे सान्याल के बड़े भाई राधामाधव ने पीयूसीएल, छत्तीसगढ़ के महासचिव बिनायक सेन को एक पत्र लिखा और उनसे सान्याल के लिए वकील और चिकित्सा का इंतजाम करवाने की अपील की. इस पत्र की प्रतियां उन्होंने कई मानवाधिकार संगठनों को भी भेजीं. क्षेत्र के सबसे सक्रिय मानवाधिकार कार्यकर्ताओं में से एक बिनायक ने इस मामले में हस्तक्षेप किया. उन्होंने अपने फ्लैट के सामने रह रहे एक वकील भीष्म किंजर को सान्याल का केस लेने को राजी किया. साथ ही उन्होंने सान्याल की शल्यक्रिया के लिए जेल अधिकारियों को पत्र लिखना भी शुरू किया. बूढ़े और खुद भी बीमार राधामाधव का कोलकाता से रायपुर आना और भी कम होता गया. वो निश्चिंत थे कि सेन उनके भाई का ख्याल रखेंगे.
छह मई 2007 को रायपुर पुलिस ने अचानक पीयुष गुहा नामक कोलकाता के एक व्यापारी को गिरफ्तार किया. गुहा राधामाधव का परिचित था जो किंजर की फीस के 49,000 रुपये राधामाधव से लेकर सेन को देने जा रहा था. पुलिस ने दावा किया कि उन्हें गुहा से तीन अहस्ताक्षरित पत्र भी मिले हैं जिन्हें मिस्टर पी, दोस्त वी और दोस्त को संबोधित किया गया था और जिनमें जेल की परिस्थितियों,
उम्र, जोड़ों के दर्द आदि जैसी चीजों की शिकायत की गई थी. पुलिस को यकीन था कि ये पत्र सान्याल के लिखे हुए हैं और इनके मुताबिक इनमें किसानों और शहरी केंद्रों में काम का विस्तार करने की सलाह दी गई थी. साथ ही इसमें नवीं कांग्रेस के सफलतापूर्ण आयोजन पर बधाई भी दी गई थी. हास्यास्पद रूप से पुलिस ने इन पत्रों को विस्फोटक बताया. पुलिस के मुताबिक गुहा ने माना था कि उसे ये पत्र सेन ने दिए थे जो जेल में बंद नक्सलियों के लिए अवैध पत्रवाहक का काम कर रहे हैं. मगर जैसे ही गुहा को मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया गया तो उसने और ही बात कही. उसने खुलासा किया कि असल में उसे एक मई को गिरफ्तार किया गया था और पांच दिन तक अवैध रूप से हिरासत में रखकर और यातनाएं देकर उससे एक खाली दस्तावेज पर हस्ताक्षर करा लिए गए.
इस तरह के हास्यास्पद सबूतों पर पुलिस ने सेन को भगोड़ा नक्सल नेता घोषित कर दिया. उस समय सेन अपनी बीमार मां को देखने कोलकाता गए हुए थे. स्थानीय मीडिया में ये खबरें छपीं. इसे सुनकर सेन भौचक रह गए. उन्हें विश्वास था कि पुलिस को जरूर कोई गलतफहमी हुई है. उन्हें भारत की संवैधानिक व्यवस्था पर पूरा भरोसा था. इसलिए शुभचिंतकों की राज्य में न जाने और अग्रिम जमानत लेने की सलाहों को उन्होंने दरकिनार कर दिया. अपने त्रुटिहीन रिकॉर्ड और बेकसूर होने को लेकर निश्चिंत सेन पुलिस की गलतफहमी दूर करने बिलासपुर पहुंचे. यहां पहुंचने पर पुलिस ने उनसे कहा कि उनका बयान लिया जाएगा और वो तारबहार थाने में रुक जाएं. सेन ने ऐसा ही किया और 14 मई 2007 को उन्हें छत्तीसगढ़ विशेष जन सुरक्षा कानून और गैरकानूनी गतिवधि (बचाव) एक्ट के तहत फौरन गिरफ्तार कर लिया गया. ये दोनों देश के सबसे कठोर कानूनों में से एक हैं जिनमें किसी चीज के लिए सोचना ही आपको जेल पहुंचा सकता है. जैसाकि किंजर कहते हैं, “मुझे पता था कि जज ज़मानत देने से इनकार कर देंगे. अगर आप पर इन कानूनों के तहत मामला दर्ज हुआ है तो समझिए आपका काम-तमाम हो गया. ये कानून जजों के मन में एक तरह का पूर्वाग्रह पैदा करने के लिए बनाए गए हैं.”
सेन के खिलाफ अभियोजन पक्ष के मुख्य आरोपों में एक ये है कि सेन जेल में बंद नक्सल नेता सान्याल से 33 बार मिले हैं. चलिए कुछ पल के लिए इस बात को छोड़ देते हैं कि सान्याल ने ऐसा क्यों किया, सान्याल का स्वास्थ्य, शल्यक्रिया, उनके मामले की जटिलताएं...सब छोड़ देते हैं. एक पल को ये भी मान लेते हैं कि बिनायक नक्सलियों से अप्रत्यक्ष सहानुभूति रखते हैं. मगर यहां तथ्य ये है कि इन सभी मुलाकातों की न सिर्फ कानूनी रूप से अनुमति ली गई थी बल्कि ये पूरी निगरानी में भी हुईं थीं. क्या सिर्फ इससे ही सरकार को किसी व्यक्ति की आजादी छीनने का अधिकार मिल जाता है? अभियोजन पक्ष का ये दावा है कि बिनायक ने खुद को सान्याल का रिश्तेदार बताकर अधिकारियों को धोखे में रखा. लेकिन उनकी पत्नी ने सूचना का अधिकार कानून के तहत वो पत्र निकाले जिनमें सेन ने जेल अधिकारियों से सान्याल से मिलने की अनुमति मांगी थी. पता चला कि वो सभी पीयूसीएल के आधिकारिक लेटरहेड पर लिखे गए थे जिनमें सेन ने महासचिव के रूप में हस्ताक्षर भी किए थे.
बिनायक सेन की गिरफ्तारी के बाद से ही पुलिस उनके खिलाफ हास्यास्पद सबूत ढूंढकर ला रही है. जैसे कि दो माओवादियों का एक दूसरे को लिखा गया प्रेमपत्र जिसमें बिनायक सेन का नाम है. इसके अलावा गोंदी में कथित रूप से एक मुठभेड़ स्थल पर मिला कागज का एक टुकड़ा जिसकी लिखावट शायद ही कोई पढ़ सके. पर पुलिस ने पाया है कि इसमें पीयूसीएल और छत्तीसगढ़ विशेष जन सुरक्षा कानून लिखा है. या फिर नक्सल नेता मदन बरकड़े द्वारा सेन को लिखी गई एक चिट्टी जिसमें जेल के हालात की शिकायत की गई है जिसे सेन ने मानवाधिकार संगठनों के पत्रों में प्रकाशित करवाया. हैरत है कि इन सबूतों में कुछ भी ऐसा नहीं जो साबित करे कि सेन को जमानत देना राष्ट्रीय सुरक्षा को खतरे में डालना होगा.
सवाल है कि फिर क्यों सरकार सेन को सलाखों के पीछे रखने पर तुली है? क्यों एक भले डॉक्टर को भयानक अपराधी की तरह पेश किया जा रहा है? क्यों सेन के खिलाफ सबूत बनाए जा रहे हैं? उदाहरण के लिए डीजीपी विश्व रंजन दावा करते हैं कि पीयुष गुहा, सेन के खिलाफ उनका मुख्य सबूत हैं. मगर गुहा की गिरफ्तारी के कई हफ्ते बाद पुलिस उसे चार जून 2007 को अचानक पुरुलिया ले गई और थाना बंडवाना में हुए एक पुराने बम धमाके के मामले में उसे आरोपी बना दिया. गौरतलब है कि डेढ़ साल पहले अक्टूबर 2005 में जब इस मामले की मूल एफआईआर दर्ज हुई थी तो उसमें गुहा का नाम तक नहीं था. तो क्या ये गुहा को भी एक अपराधी का जामा पहनाने के लिए किया गया था? आखिरकार सेन का दामन काला करने की ऐसी कोशिशें क्यूं? बिनायक सेन की गिरफ्तारी के बाद से ही पुलिस उनके खिलाफ हास्यास्पद सबूत ढूंढकर ला रही है. जैसे कि दो माओवादियों का एक दूसरे को लिखा गया प्रेमपत्र जिसमें बिनायक सेन का नाम है. इसके अलावा गोंदी में कथित रूप से एक मुठभेड़ स्थल पर मिला कागज का एक टुकड़ा जिसकी लिखावट शायद ही कोई पढ़ सके.
बिनायक सेन मामले की भयावहता को पूरी तरह से समझने और इस देश के लिए इसके मायने जानने के लिए आपको छत्तीसगढ़ पर गौर से निगाह डालनी होगी. बिनायक सेन की कहानी उनके जैसे सैकड़ों बेनाम लोगों की कहानी का एक उदाहरण मात्र है जो उस लड़ाई में फंस गए हैं जो सरकार ने अपने ही लोगों के खिलाफ छेड़ रखी है. उन तमाम लोगों की तरह ही सेन की व्यथा भी मानवाधिकारों के खुलेआम हनन की कहानी है. कई मामलों में छत्तीसगढ़ अब माओवादी विद्रोह का केंद्र बन गया है जिसकी जड़ें 13 राज्यों में फैली हैं. छत्तीसगढ़ में खुद सरकार का कहना है कि बस्तर और दंतेवाड़ा के ज्यादातर हिस्से उसके नियंत्रण से बाहर हैं. बिना शक ये गंभीर स्थिति है. हर साल पुलिस के सैकड़ों जवान, असहाय आदिवासी और पुल, जेल व टेलीफोन के खंभों जैसे सरकारी प्रतीक उग्रवादियों द्वारा उड़ा दिए जाते हैं. गृहमंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक साल 2007 में छत्तीसगढ़ में 311 लोगों की जानें गई. देश भर में ये आंकड़ा 571 रहा। माओवादियों से सहानुभूति रखने वाले आपको बताते हैं कि उन्हें स्थानीय लोगों का समर्थन है- ये समर्थन किस हद तक ऐच्छिक है और किस हद तक दबाव में, इसके बारे में कोई भी साफ-साफ नहीं बोलता। माओवादियों के बारे में जानकारी पाने का सिर्फ एक ही रास्ता है कि वो खुद आपको जंगलों में अपने कैंप तक ले जाएं. ज़ाहिर है ऐसे में वहां से आपको सिर्फ चुनिंदा सूचनाएं ही हासिल होंगी. ये बात भी साफ है कि जो इलाके माओवादियों के प्रभाव वाले हैं उनकी सरकारों ने पूरी तरह से अनदेखी की हुई है. स्कूल, प्राथमिक चिकित्सा, बिजली, आजीविका जैसी चीजें यहां कहीं नजर नहीं आतीं. कई जगह सरकार ऐसे विकास और औद्योगीकरण की हड़बड़ी में है जो कि स्थानीय लोगों की उम्मीदों और जरूरतों से मेल नहीं खाता.
अदूरदर्शिता के चलते भारत सरकार शिकायतों का इलाज हिंसा से और रोग का इलाज रोगी को मिटाकर कर रही है. कठोर क़ानून, अनगिनत अर्धसैनिक बल, पुलिस के आधुनिकीकरण के लिए हज़ारों करोड़ के पैकेज और नक्सल प्रभावित राज्यों के लिए विशेष पैकेज. यानी कि सरकारी जवाब हिंसा की एक प्रतिस्पर्धी ज़मीन तैयार करने जैसा है. इसका उदाहरण है छत्तीसगढ़ में 2005 में ही सरकार प्रायोजित नक्सल विरोधी अभियान, जो अब सल्वा जूडम के नाम से कुख्यात है. इसने एक ग्रामीण को दूसरे ग्रामीण पर गोलियां चलाने के लिए तैयार कर एक अघोषित गृहयुद्ध को बढ़ावा दिया. सरकार ने 644 गांवों को जबरन खाली करवा कर वहां के लोगों को अमानवीय अवस्था में तंबुओं में रहने को मजबूर कर दिया. सरकार का नारा है कि उनके समर्थन को ही खत्म कर दो. मानवाधिकार कार्यकर्ता आपको बताएंगे कि सरकार का असल निशाना माओवादी नहीं बल्कि जमीन के नीचे प्रचुर मात्रा में मौजूद लौह अयस्क है जिसे वे नंदीग्राम की तर्ज पर निजी कंपनियों को सौंपने के लिए तैयार है.
ये अफवाहें भी उड़ रही हैं कि अस्थाई शिविरों को राजस्व गांवों में तब्दील कर दिया जाएगा और आदिवासियों द्वारा छोड़ी ज़मीनों को सरकार अपने कब्ज़े में ले लेगी. ये सब अभी भले ही कयास हों लेकिन सल्वा जुडूम की अति एक हकीकत है.
इसी का विरोध करने के लिए बिनायक सेन राज्य सरकार की आंखों की किरकिरी बन गए. उनके द्वारा उठाए गए मामलों में नारायण सान्याल का मामला शायद सबसे कम विवादित है. संतोषपुर फर्जी मुठभेड़, गोलापल्ली फर्जी मुठभेड़, नारायण खेरवा फर्जी मुठभेड़, रायपुर फर्जी आत्मसमर्पण, राम कुमार ध्रुव की हिरासत में मौत, अंबिकापुर, लाकराकोना, बांदेथाना, कोइलीबेरा—ये सभी नाम भयावह सरकारी अत्याचारों के गवाह हैं. उन अत्याचारों के जिनका सच बिनायक सेन और दूसरे मानवाधिकार कार्यकर्ता सामने लाए जिससे सरकार को खासी शर्मिंदगी झेलनी पड़ी. दिसंबर 2005 में बिनायक सेन ने 15 लोगों के एक दल के साथ सल्वा जूडम पर करारी चोट करने वाली एक रिपोर्ट प्रकाशित की.
बिनायक सेन ने सरकार को एक बार नहीं बल्कि बार-बार आईना दिखाने का अपराध कर रहे थे और इसके एवज़ में सरकार कुछ भी करके उन्हें एक सबक सिखाना चाहती थी. बिनायक सेन की असल कहानी एक बुद्धिहीन और डरे हुए राज्य की अंधेरगर्दी की कहानी है. सरकार का रवैया जार्ज बुश जैसा ही है. जिसे उस जगह जनसंहार के हथियार नजर आ रहे हैं जहां असल में कुछ है ही नहीं. बिनायक सेन जैसे लोगों की छवि ओसामा बिन लादेन जैसी बनाई जा रही है. और ये सब किया जा रहा है राष्ट्रीय सुरक्षा की आड़ में.
एक हल्के-फुल्के क्षण में डीजीपी विश्व रंजन ये स्वीकार करते हैं कि सेन के साथ न्याय नहीं हुआ. वो कहते हैं, "अगर मेरे बस में होता तो मैं बिनायक सेन को निगरानी में रखता उन्हें गिरफ्तार नहीं करता." ये एक बड़ी स्वीकरोक्ति है. तुरंत ही संभलते हुए, उसी सांस में वो ये भी कह जाते हैं कि सेन के खिलाफ उनके पास सबूतों का पहाड़ है. ऐसे सबूत जिसे वे न तो आपको दिखा सकते हैं और न ही अदालत में ही पेश कर सकते हैं. जब तक सबूतों का असल जैसा पहाड़ खड़ा नहीं कर दिया जाता तब तक बिनायक सेन जेल में सड़ते रहेंगे. एक हल्के-फुल्के क्षण में डीजीपी विश्व रंजन ये स्वीकार करते हुए मिलते हैं कि सेन के साथ न्याय नहीं हुआ. वो कहते हैं, "अगर मेरे बस में होता तो मैं बिनायक सेन को निगरानी में रखता उन्हें गिरफ्तार नहीं करता." ये एक बड़ी स्वीकरोक्ति है.
2 फरवरी 2008 की सुबह, गिरफ्तारी के पूरे 9 महीने बाद, सेन के खिलाफ आरोप तय करने के लिए उन्हें रायपुर की सत्र अदालत में पेश किया गया. पुलिसवालों की भीड़ से घिरे शांतचित्त, आकर्षक बिनायक सेन पुलिस वैन से नीचे उतरते हैं. दृढ़ता से हाथ मिलाने के बाद कहते हैं, "यहां आने के लिए धन्यवाद", इसके बाद सारे लोग अदालत में चले जाते हैं. जज सलूजा थोड़ी असहजता के साथ आरोपों को सुनाते हैं. वो कुछ बेकार के आरोपों को खारिज कर सकते थे लेकिन ऐसा नहीं करते. बिनायक विटनेस बॉक्स में चुपचाप खड़े रहते हैं. और अंत में सारे आरोपों को मानने से इनकार कर देते हैं. इसके बाद वे अपनी पत्नी और वकील से मिलने के लिए कुछ समय मांगते हैं जो उन्हें दे दिया जाता है.
वहां हवाओं में एक अजीब सा डर साफ महसूस किया जा सकता है. तमाम डॉक्टर जो उनका साथ देने के लिए आए हैं, बात करने से भी झिझकते हैं. एक दिन पहले ही पूरे रायपुर में बड़े पैमाने पर गिरफ्तारियां हुई हैं- दो महिलाएं, एक ट्रैवेल एजेंसी का मालिक, एक पत्रकार...हर आदमी खुद को शिकार महसूस कर रहा है. झूठ और सच में फर्क करना मुश्किल है. यद्यपि बिनायक सेन इस सबसे विरक्त से प्रतीत होते हैं. जब पुलिस उनको वैन में धकेलती है तो वे लोहे की जालियों से मुंह सटाकर कहते हैं, "कुछ लोगों को जानबूझ कर विकास की प्रक्रिया से बाहर रखा जा रहा है. आप दो तरह के लोगों का वर्ग तैयार नहीं कर सकते. सबको इसके खिलाफ आवाज़ उठानी होगी वरना जल्द ही बहुत देर हो जाएगी." उनकी आवाज़ सलाखों के पीछे से भी सुनायी दे रही है "अगर ये लोग मुझ जैसे आदमी को गिरफ्तार करते हैं तो मानवाधिकार कार्यकर्ता असहाय हो जाएंगे. मैंने कभी भी माओवादी हिंसा का समर्थन नहीं किया. यह एक अवैध आंदोलन है जो ज़्यादा दिनों तक नहीं टिक पाएगा. सल्वा जूडम के साथ मिलकर इसने आदिवासी समुदायों में खतरनाक खाई पैदा कर दी है. लेकिन उनकी व्यथा वास्तविक है. ये इलाका इस समय अकाल से जूझ रहा है. लोगों के शरीर का वजन 18.5 से भी नीचे आ गया है, 40 फीसदी आबादी कुपोषण की शिकार है. दलितों और आदिवासियों में इसका स्तर 50 से 60 फीसदी तक है. हमें और ज्यादा भागीदारी सुनिश्चित करने वाले विकास की जरूरत है. आप लोगो की दो श्रेणियां नहीं बना सकते...."
बातचीत कहीं से भी उनके भारत को तोड़ने वाला होने का आभास नहीं देती. ये पूछने पर कि खुद को नक्सली घोषित कर चुके नारायण सान्याल का साथ आप ने क्यों दिया, बिनायक सेन का जवाब दुनिया भर में मानवाधिकारों की जरूरत को स्थापित करता है, "मुझे पता था मैं शेर के मुंह में घुस रहा था लेकिन अगर आप अपने कदम पीछे खींचने लगे तो फिर आप कहां जाकर रुकेंगे? आप भेद-भाव नहीं कर सकते. सबको क़ानूनी सहायता और चिकित्सा सेवा पाने का अधिकार है. ये संविधान में लिखा है. ये मानवाधिकारों का आधार है."
डीजीपी विश्व रंजन गुस्से से पूछते हैं, "वह माओवादियों से ज्यादा सल्वा जूडम की आलोचना क्यों करते हैं?" बिनायक का जवाब होता है कि संविधान और क़ानूनी मर्यादाओं से बंधे होने के कारण भारत सरकार की जिम्मेदारियां उन माओवादियों के बनिस्बत ज्यादा बड़ी हैं जिन्होंने राज्य को ही त्याग दिया है. लेकिन सरकार से ऊंचे मूल्यो वाली ये नैतिकता हज़म नहीं होती. इलिना सेन से ये पूछने पर कि आपको ये लड़ाई लड़ने का जज्बा कहां से मिला, जवाब मिलता है, "मुझे महसूस हुआ कि ये सिर्फ बिनायक और मेरे परिवार का ही मामला नहीं है. हम एक बहुत बड़ी लड़ाई का हिस्सा हैं. हम शांतिपूर्वक अपनी असहमति जताने के अधिकार की लड़ाई लड़ रहे हैं. इसके प्रति हमारा समर्पण मुझे ताकत देता है." ये एक और ऐसा नैतिक सदाचरण है जो सरकार के गले नहीं उतरता. मेधा पाटकर को ही लीजिए. 20 सालों का शांतिपूर्ण विरोध- नतीजा सिफर. शर्मिला इरोम को लीजिए- सात सालों का उपवास लेकिन कोई फल नहीं। बिनायक सेन को ही लें...
जल्द ही बिनायक सेन की सुनवाई शुरू होगी. इस दौरान उन्हें कैद रखने का मतलब होगा कि भारत में शांतिपूर्ण विरोधों के लिए कोई जगह नहीं. ये जनसंहार के हथियारों को खाद-पानी देने के जैसा है. ये अपनी बात रखने के लिए हिंसक तरीके अपनाने को प्रेरित करने जैसा है. ये पहले से ही ज़िम्मेदार लोगों द्वारा तार-तार किये जा चुके गांधीवाद की धज्जियां उड़ाने जैसा होगा.