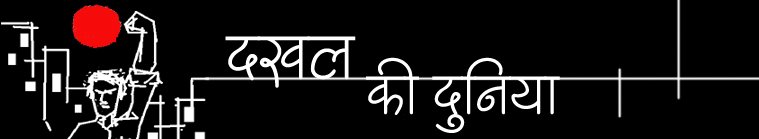-युग मोहित चौधरी*
युग मोहित चौधरी ने 9 फरवरी 2013 को दूसरे शाहिद आज़मी स्मृति व्याख्यान में जो भाषण दिया उसका ये संपादित रूप है। मृत्युदंड की अवधारणा पर करारा चोट करता यह भाषण उन सबके लिए हैं जो देश
को कम हिंसक और कम प्रतिक्रियावादी जगह के तौर पर देखना चाहते हैं। लेख लंबा है लेकिन किस्तों की बजाए एक बार में इसलिए छाप रहे हैं ताकि लयात्मकता बरकरार रहे। मूल रूप से अंग्रेज़ी में
दिए गए भाषण का लिप्यांतरण दीप्ती स्वामी, धीरज पांडेय और अनुराग सेठी ने किया।
(महताब आलम के लगातार आग्रह पर हिंदी अनुवाद : दिलीप ख़ान)
 |
| अधिवक्ता युग मोहित चौधरी |
फरमन वनाम जॉर्जिया (1972) केस में अमेरिका के उच्चतम न्यायालय ने मृत्युदंड की मुखालफत की। न्यायाधीश मार्शल ने कहा कि अगर नागरिकों को इस बात की पूरी जानकारी हो कि लोगों को किस तरह मृत्युदंड सुनाए जाते हैं तो उन्हें लगेगा कि मौत की सजा स्तब्धकारी, ग़लत और अस्वीकार्य है। हालांकि भारत में मृत्युदंड उन्मूलन अभियान में ऐसे शोध और लोगों के बीच जागरुकता अभियान जैसे काम को सर्वाधिक नज़रंदाज किया गया है। भारत में मृत्युदंड की संवैधानिकता को चुनौती देने वाले अंतिम तीन बिंदुओं को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया, क्योंकि उन्मूलन के दावों को समर्थन देने के लिए कोई अनुभवजन्य आंकड़ें (empirical data) नहीं थे। अफ़सोसजनक ये है कि परिस्थिति में अब भी कोई बदलाव नहीं आया है। अब भी इस मामले पर शायद ही कोई शोध हुआ है। इसलिए मृत्युदंड के ऊपर अनुभवजन्य शोध करना उन्मूलन अभियान की प्राथमिकता में शीर्ष पर होना चाहिए। हरेक प्रस्तावित मृत्युदंड को रोकने की हरसंभव कोशिश में विफल रहने के बाद हमें कम-से-कम राज्य को उस स्थिति तक पहुंचाना चाहिए कि अगले मामले में मृत्युदंड देना उसके लिए मुश्किल भरा काम बन जाए। इसके लिए हरसंभव क़ानूनी, राजनीतिक और सामाजिक तौर-तरीकों का इस्तेमाल करना चाहिए। मृत्युदंड का उन्मूलन कभी भी एक झटके में नहीं हुआ है और न ही ऐसा होगा। इस दिशा में होने वाली प्रगति की रफ़्तार सुस्त होगी और ये हम पर निर्भर करता है कि हम सरकार, अदालत, संसद और लोगों को ये समझा सके कि इससे हमें कुछ भी हासिल नहीं होता, अलबत्ता हमारे मानवीय स्तर को ये नीचे ज़रूर गिराता है।
आज मृत्युदंड का विरोध करने के अनेक कारण हैं। लोग यह आसानी से महसूस सकते हैं कि किसी को मारना नैतिक तौर पर ग़लत है, कि सजा के तौर पर एक हत्यारे की हत्या करना पाखंड है, कि आजीवन कारावास की बजाय मृत्युदंड देने से अपराध की मात्रा में कोई कमी नहीं आती। मृत्युदंड की मुख़ालफ़त के पीछे जो एक और कारण हैं वो ये कि इस सजा को वापस नहीं लिया जा सकता। ऐसे कई मामले हैं जब अदालती फ़ैसले ग़लत साबित हुए और जिन्हें दुरुस्त करने का कोई मौका नहीं बचा। एक बार जिसे मौत दे दी गई, उसे ठीक करने का कोई तरीका नहीं होता। मौत के घर से वापसी नहीं होती। चलिए हम तीन सामाजिक संस्थाओं के संदर्भ में मृत्युदंड की चर्चा करते हैं, ताकि इसके उन्मूलन के लिए तर्क निकल सके। ये तीन संस्थाएं हैं, पुलिस, जोकि सबूत इकट्ठा करने वाली इकाई है; अदालत, जोकि दोष तय करने और उपयुक्त सजा सुनाने वाली इकाई है और कार्यपालिका, जोकि क्षमा याचिका पर विचार करने वाली ईकाई है।
इस बात को बहुत ज़ोर देकर उभारने की ज़रूरत नहीं है कि हमारे यहां, भारत में, पुलिस बल बदमाश, भ्रष्ट, बेईमान और आपराधिक है। अदालत में जो सबूत पेश होते हैं उसे यही पुलिस जमा करती है। हम इन्हीं सबूतों के बिनाह पर ये तय करते हैं कि किसी को मौत की सजा सुनाई जाए या नहीं। यह अपने-आप में सोचने वाली बात है कि जिस पुलिस के बारे में हम जानते हैं कि वो भ्रष्ट और बेईमान है, उसके द्वारा पेश किए गए सबूतों के आधार पर सजा तय होती है। इसके मुतल्लिक मैं कुछ उदाहरण पेश करता हूं :- मुंबई में कुछ साल पहले एक आदमी को एक बच्चे की हत्या और बलात्कार के मामले में दोषी पाते हुए सजा सुनाई गई। अर्जी उच्च न्यायालय में अटकी थी और इसी दरम्यान पुलिस अधिकारियों को जांच-पड़ताल के बाद ये पता चला कि वो मामला आत्महत्या का है और पुलिस ने आत्महत्या नोट बरामद करते हुए माना कि उस आदमी को उन लोगों ने ख़ामख़्वाह पकड़ लिया था। अब रिकॉर्ड में जो सबूत हैं उसके आधार पर उस आदमी को निर्दोष नहीं माना जा सकता क्योंकि सबूत काफी मज़बूत थे। सुसाइड नोट सबूत का हिस्सा नहीं था और उसके बग़ैर वो आदमी मौत के पार पहुंच सकता था। बंबई उच्च न्यायालय ने अपारंपरिक तौर पर उस सुसाइड नोट पर ग़ौर करते हुए उस आदमी को बरी कर दिया। अगर मामला इस तरह हल नहीं हुआ होता तो कल्पना कीजिए क्या घटित हो चुका होता?
मैं आपको कुछ दूसरे उदाहरण दूंगा। जिन मामलों को शाहिद (शाहिद आज़मी**) देख रहे थे उन्हें आज-कल मैं देख रहा हूं। वो मामला है, 2006 का मालेगांव बम धमाका। शब-ए-बरात की पवित्र रात या बड़ी रात को मुस्लिम बाहुल्य शहर मालेगांव में मस्जिद के बाहर बम धमाके हुए। नौ लड़कों को इस मामले में पकड़ा गया और उनपर उन धमाकों के आरोप लगाए गए। नौ स्वीकृतियां (कनफेसन) रिकॉर्ड में दर्ज हैं। पुलिस का दावा है कि उसने उन लोगों के घर से आरडीएक्स सहित अन्य विस्फोटक सामग्रियां जब्त की। पुलिस ने ये भी दावा किया कि उन नौ में से एक लड़के का जमीर जाग गया और वो अपने सहयोगियों के ख़िलाफ़ राज्य के लिए गवाह बनने को तैयार हो गया। मामले में आरोप पत्र दायर किया गया। मुंबई में पूरे मामले पर गर्माहट के बाद केस सीबीआई को सौंप दिया गया। सीबीआई ने एक पूरक आरोप पत्र दायर किया जोकि मुंबई पुलिस द्वारा किए गए जांच-पड़ताल से संबंधित था। और फिर, एनआईए (राष्ट्रीय जांच एजेंसी), जोकि समझौता एक्सप्रेस धमाकों की जांच कर रही थी, उसने स्वामी असीमानंद को गिरफ़्तार किया। असीमानंद ने बाद में ये स्वीकारा कि उसने ही मालेगांव के तीन धमाकों को अंजाम दिया। उसने बताया कि उसके हिंदूवादी दक्षिणपंथी आतंकी समूह ने मालेगांव में धमाका किया है। तो, उन तमाम सबूतों का क्या हुआ, उन स्वीकृतियों का क्या हुआ और उस आरडीएक्स का? कहां से वो आरडीएक्स आया था और कहां ग़ायब हो गया?
अब आप खुद को वकील की जगह रखकर देखें, एक केस में पुलिस कोर्ट के सामने आरडीएक्स ये कहते हुए पेश कर रही है कि उसने आरोपियों के घर से उसे जब्त किया है। बचाव पक्ष का वकील कह रहा है कि सबूत गढ़ा गया है। जज पूछता है, "पुलिस ने इसे फिर कहां से बरामद किया?" आप इस सवाल का जवाब कैसे देंगे? जज अपने सामने पेश किए गए उस सबूत पर यकीन करेगा और ये मानेगा कि वाकई आरडीएक्स जब्त किया गया होगा क्योंकि लोगों के पास आखिरकार कहां से आरडीएक्स आएगा? सामान्य लोगों के पास आरडीएक्स नहीं होता। लेकिन स्वामी असीमानंद की स्वीकृति जाहिर होने से पहले इन नौ लोगों के सर पर तलवार लटकी थी। सबके ऊपर। ये कोई अलग-थलग मामला नहीं है।
11 जुलाई 2006 को आधे घंटे के दरम्यान मुंबई की ट्रेन में सात धमाके हुए। पुलिस ने सिमी (स्टूडेंट इस्लामिक मूवमेंट ऑफ इंडिया) के तेरह लड़कों को ये कहते हुए गिरफ़्तार किया कि उन्हीं लोगों ने इन धमाकों को अंजाम दिया है। गिरफ़्तारी के समय उनके मोबाइल फोन जब्त कर लिए गए। मजिस्ट्रेट के सामने रिमांड आवेदन पेश करते हुए पुलिस ने लिखित तौर पर कहा कि उनके मोबाइल फोन को फॉरेंसिक जांच के लिए भेजा गया है और मोबाइल सेवा प्रदाता से मिलकर उनकी कॉल का विवरण भी खंगाला जा रहा है। कॉल रिकॉर्ड के बिनाह पर पुलिस ने दावा किया कि षडयंत्र को तय करने की खातिर वो तेरहों लड़के आपस में संपर्क में थे। इसके अतिरिक्त पुलिस ने ये भी कहा कि उनका पाकिस्तान के लश्कर-ए-तैयबा से भी संपर्क था और वे लोग नौजवानों को आतंकवादी प्रशिक्षण के लिए सीमा पार पाकिस्तान भी भेजते थे। ये सब पुलिस ने महज रिमांड आवेदन में ही नहीं कहा बल्कि हफ़्तों तक बार-बार इस बात को दोहराते रहे ताकि उन लड़कों की बढ़ी हुई हिरासत अवधि को वैधता दे सके। 189 लोग उन धमाकों में मारे गए। कोई भी मजिस्ट्रेट या जज ऐसे मामलों में बेल नहीं देगा, ख़ासकर तब जब पुलिस इतने मज़बूत फॉरेंसिक सबूत पेश कर रही हो। लश्कर-ए-तैयबा के साथ संपर्क में रहना और आतंकवादी प्रशिक्षण के लिए लोगों को उनके पास भेजना बेहद गंभीर मामला है।
बहरहाल, कुछ समय बाद, मुंबई पुलिस की दूसरी शाखा ने कुछ अन्य लोगों को पकड़ा जो यह मान रहे थे कि उन्होंने मुंबई की रेलों में धमाके किए। उनके पास आत्मस्वीकृति के रिकॉर्ड थे। जब सिमी वाले मामले में आरोपपत्र दाखिल किए गए थे तो उन लड़कों ने अपने मोबाइल रिकॉर्ड की प्रतियां मांगी क्योंकि पुलिस ने आरोपपत्र के साथ उसे नत्थी नहीं किया था। यह बहुत अचंभित करने वाला तथ्य है कि पुलिस ने उन्हीं फोन रिकॉर्ड के आधार पर ये दावा किया था कि उन लड़कों का लश्कर के साथ ताल्लुक है और बाद में उन्हीं मोबाइल फोन रिकॉर्ड को सार्वजनिक नहीं कर रही! पुलिस ने आरोपपत्र के साथ उन रिकॉर्ड को नत्थी क्यों नहीं किया?
 |
| मौत के घर से वापसी नहीं होती। |
उन लड़कों ने हमेशा कहा कि अगर अदालत के सामने उन रिकॉर्ड को पेश किया जाता है तो घटना में उनकी निर्लिप्तता साबित हो जाएगी। लोग जान जाएंगे कि वे निर्दोष हैं। तथ्य ये है कि बम धमाकों के समय वे सब किसी दूसरी जगह पर मौजूद थे। (मोबाइल) टावर का लोकेशन ये साफ़ बता रहा था कि पुलिस के दावों के विपरीत वे चर्च गेट स्टेशन के पास नहीं थे। उनमें से एक तो मुंबई से बाहर बिहार में कहीं था। कुछ चर्च गेट स्टेशन से बिल्कुल उल्टे छोर पर उत्तरी मुंबई में थे। इसलिए उन लड़कों ने लगातार ये कहा कि उनके बचाव के लिए वो फोन रिकॉर्ड्स अहम दस्तावेज़ है। बचाव पक्ष के वकील द्वारा छह साल के भीतर उन रिकॉर्ड्स की प्रतिलिपि मांगने के लिए छह बार आवेदन दिया गया जिन्हें पुलिस ने (कथित तौर पर) अपने पास जमा रखा था। लेकिन पुलिस ये कहकर रिकॉर्ड्स देने से लगातार मना करती रही कि चूंकि आरोप पत्र में उन्होंने उन रिकॉर्ड्स को चस्पां नहीं किया है इसलिए आरोपित को दस्तावेज़ देने के लिए वो बाध्य नहीं है। लेकिन जैसा कि आतंकवाद से जुड़े मुक़दमें में ज़्यादातर होता है, चौतरफ़ा दबाव के चलते अभियोजन पक्ष द्वारा रखी गई दलीलों पर जज सिर्फ़ मुहर लगाता चलता है, उन फोन रिकॉर्ड्स के लिए छह साल में किए गए छह आवेदनों को जज ने खारिज कर दिया।
पुलिस लगातार उन रिकॉर्ड्स को देने से इनकार करती रही, लेकिन उस मामले के मुतल्लिक और कुछ भी कहने से बचती रही। आख़िरकार हमने उच्च न्यायालय का रुख किया और वहां उन रिकॉर्ड्स को मांगने के लिए अपील की। उच्च न्यायलय ने उन रिकॉर्ड्स को प्रासंगिक और ज़रूरी माना और पुलिस को निर्देश दिया कि वो दस्तावेज़ हमें सौंपे। छह साल बाद और आख़िरी बार जब पुलिस ने हमें रिकॉर्ड्स देने से मना किया था उसके तीन महीने बाद उच्च न्यायालय में पहली बार पुलिस ने मुंह खोला और कहा कि उसने उन रिकॉर्ड्स को नष्ट कर दिया है! जबकि पुलिस बीच-बीच में ये दावा कर रही थी कि उन दस्तावेज़ों के आधार पर कुछ आरोपितों को अभी पकड़ा जाना बाकी है, वो कैसे उन रिकॉर्ड्स को नष्ट कर सकती है?
सामान्य अपराध के मामलों में आत्म-स्वीकृति को बतौर सबूत मामूली भाव मिलता है, क्योंकि एक पुलिस अधिकारी की कही गई बातों पर कोई किस तरह भरोसा कर ले? न्यायिक सिद्धांत में इसी आधार पर आत्म-स्वीकृति को सबूत से अलग कर दिया गया। लेकिन, गंभीर अपराधों में आत्म-स्वीकृति को सबूत के तौर पर लिया जाता है। ये हैरतअंगेज़ व्यवस्था है। अगर आत्म-स्वीकृति को सामान्य अपराध में सबूत के तौर पर मान्य नहीं ठहराया जाता तो फिर गंभीर क़िस्म के अपराध में आरोपियों के ऊपर इसे क्यों लादा जाता है? लेकिन हमारे यहां क़ानूनन यह व्यवस्था है। आतंकवाद के मामले में यह विशेष व्यवस्था लागू होती है। इसलिए 2006 के मालेगांव मामले में पुलिस ने अदालत के सामने हमेशा नौ आत्म-स्वीकृतियों को सबूत के तौर पर पेश किया। हां, साथ में आरडीएक्स बरामदगी की मनगढंत कहानी ज़रूर चस्पां की। कोई भी वास्तविक सबूत नहीं पेश हुआ। एक आत्म-स्वीकृति को अपने मुताबिक ढालने में ज़्यादा मशक्कत नहीं करनी पड़ती जब उसका सत्यापन भी ख़ुद पुलिस अधिकारियों को ही करना हो!
इंदिरा गांधी हत्याकांड में उनके सुरक्षा दस्ते में से एक सुरक्षाकर्मी बलवंत सिंह को फौरन गिरफ़्तार कर लिया गया। हत्या के तुरंत बाद, ग़ैरक़ानूनी तरीके से। हालांकि उनकी गिरफ़्तारी को दिखाया नहीं गया लेकिन यमुना वेलोड्रम के छोर से ग़ैरक़ानूनी तरीके से उसको उठाकर कई दिनों तक रखा गया। उस दौरान हिरासत में उसको भीषण यातनाएं दी गईं और बाद में छोड़ दिया गया। उसके एक या दो दिन बाद जब वो आईएसबीटी में बस में चढ़ने जा रहा था तो उसकी गिरफ़्तारी गिखाई गई। पुलिस ने दावा किया कि उसकी जेब से चिट्ठी की शक्ल में पूरा का पूरा आत्म-स्वीकृति नोट बरामद हुआ है, जिसमें विस्तार से उसके बयान दर्ज़ थे। पुलिस के दावों पर यक़ीन करें तो वो अपनी जेब में आत्म-स्वीकृति नोट लेकर दिल्ली की सड़कों पर घूम रहा था! यह इंदिरा गांधी हत्याकांड का सच है! ट्रायल कोर्ट ने इस क़िस्से पर अपना भरोसा जताया और बलवंत सिंह को मौत की सजा सुना दी। हाई कोर्ट ने भी भरोसा का इजहार किया और बलवंत सिंह की मौत की सजा को बरकरार रखा।
इसलिए मैं वापस उसी सवाल पर आना चाहता हूं: क्या ऐसे सबूत के आधार पर लोगों को मौत की सजा सुनाना जायज है?
******************
मृत्युदंड में संलिप्त दूसरी संस्था है- न्यायपालिका, और न्यायपालिका की ग़लती करने की क्षमता उतनी ही है जितनी भारत में किसी दूसरी संस्था की। इसमें उसी तरह के लोग शामिल हैं जैसे समाज के अन्य दूसरी संस्थाओं में होते हैं। ग़लतियां लोगों से होनी अवश्यंभावी हैं। मृत्युदंड के संदर्भ में ख़ास तौर पर इसे परखा जाना चाहिए क्योंकि 'रेयरेस्ट ऑफ द रेयर' का समूचा मसला इतना व्यक्तिकेंद्रित होता है कि इसकी पड़ताल में नज़रियों का फर्क आसानी से पाया जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने बार-बार ये माना है कि मृत्युदंड के उसके फैसले भी चुनिंदा होते हैं और इसके नियम में कोई स्थिरता या फिर सामान्यता नहीं है। इस आधार पर देखें तो न्याय हासिल करने में समानता के अधिकार का लगातार उल्लंघन होता रहा है। बच्चन सिंह (1982) के मामले में सुप्रीम कोर्ट के पूर्व मुख्य न्यायाधीश जस्टिस भगवती ने कहा था कि सुप्रीम कोर्ट 'मनमौजी और सनकनपन' में मृत्युदंड सुनाता है। क्या वो ग़लत थे?
फरमन बनाम जॉर्जिया मामले में जस्टिस स्टीवर्ट ने कहा था कि मृत्युदंड मनमाने और क्रूर तरीके से सुनाया जाता है। किसी को पता नहीं होता कि अगली बारी किसकी है। जिसको सजा सुनाई गई, उसे उसका दुर्भाग्य ही समझा जाना चाहिए! हरबन सिंह (1982) के मामले में इसे हम स्पष्ट तौर पर देख सकते हैं। हत्या के एक ही तरह के तीन मामलों में तीन लोगों को मौत की सजा सुनाई गई और सुप्रीम कोर्ट की तीन अलग-अलग खंडपीठ ने उन मामलों पर नाटकीय तौर पर तीन अलग-अलग फैसले सुनाए। कश्मीरा के मृत्युदंड को आजीवन कारावास में तब्दील कर दिया गया, जीता की अपील ठुकरा दी गई और उसे फांसी हुई और हरबन को राष्ट्रपति के यहां से क्षमादान मिली, जबकि कोर्ट ने उसकी शुरुआती अपील और पुनर्विचार याचिका को खारिज कर दिया था।
मृत्युदंड के फैसले में ये उदाहरण 'भ्रम, विचलन और विरोधाभास' की तस्वीर पेश करते हैं। एकसमान मामलों पर अलग-अलग फैसले पर्याप्त संख्या में मौजूद है और ये चिंता का विषय है। इन मामलों में जिनको मौत मिली और जिनको आजीवन कारावास मिली उनके बीच सिवाय अलग खंडपीठ के और कोई बड़ा अंतर नहीं था। जहां न्यायमूर्ति बालाकृष्णन और सिन्हा ने बच्चों के बलात्कार और हत्या के सारे मामलों में मिले मृत्युदंड को आजीवन कारावास में तब्दील कर दिया, वहीं जस्टिस पसायत ने लगभग हर मामले में मृत्युदंड को या तो बरकरार रखा या फिर नए सिरे से यह सजा सुनाई, यहां तक कि उन मामलों में भी जिनमें निचली अदालतों ने आरोपी को मुक्त कर रखा था। मृत्युदंड ऐसे में इस पर निर्भर हो जाता है कि आख़िरकार उसको सुनाने वाला जज कौन है। यह ऐसा जुआ बन जाता है जिसमें यह देखना सबसे ज़्यादा दिलचस्प होता है कि किसी ख़ास जज की मौजूदगी से मृत्युदंड की सांख्यिकी में कितना सकारात्मक और कितना नकारात्मक फ़र्क़ पैदा होता है। यानी जीने और मरने की संभावना सबूतों की बजाय जज पर निर्भर करता है! तीन जजों की तुलना से यह साफ़ हो जाएगा कि किस तरह मृत्युदंड को लेकर जजों का निजी नजरिया फैसलों में जाहिर होता है।
क्रिकेट की छोटी शैली में इस्तेमाल होने वाली भाषा के सहारे कहें तो जस्टिस पसायत का "स्ट्राइक रेट" लगभग 73 फीसदी है, जोकि उनके कार्यकाल में रहने वाले बाकी सारे जजों के सम्मिलित स्ट्राइक रेट (19 फ़ीसदी) से काफ़ी ज़्यादा है। इस तरह जो मामला जस्टिस पसायत की खंडपीठ को नहीं सौंपा गया, उसमें मृत्युदंड से बचने की संभावना चौगुनी बढ़ जाती है। मृत्युदंड के एक मामले की सुनवाई जस्टिस पसायत और जस्टिस सिन्हा के पास होने की संभावना लगभग बराबर का है, लेकिन आरोपी के ज़िंदा रहने की संभावना 100 फ़ीसदी हो जाती है अगर वो केस जस्टिस सिन्हा के पास पहुंचा हो। एक कैदी के ज़िंदा रहने की संभावना 50 फ़ीसदी बढ़ जाती है अगर वो केस जस्टिस पसायत की खंडपीठ की बजाय जस्टिस बालाकृष्णन के पास पहुंचे। क्या मृत्युदंड की अपील करने वाले एक व्यक्ति को यह सवाल नहीं पूछना चाहिए, "मैं जिंदा रहूंगा या नहीं यह मेरे केस में मौजूद सबूत से तय होगा या फिर गठित होने वाली खंडपीठ से?" इससे भयावह नहीं तो कम से कम फैसलों में ऐसा ही अंतर ब्लैकशील्ड (1972-1976) के अध्ययन में भी जाहिर होता है। भगवती के इस बयान पर शक की कोई गुंजाइश नहीं रहनी चाहिए कि "कोई व्यक्ति जिएगा या मरेगा यह बहुत कुछ खंडपीठ में शामिल जजों के समिश्रण पर निर्भर करता है और यही बात मृत्युदंड को मनमाना मामला बना देता है"। जीवन की पवित्रता, बदतर अपराधियों के भीतर ‘पापमुक्ति’ की हमेशा मौजूद रहने वाली संभावना और मृत्युदंड की बर्बरता पर जस्टिस कृष्णा अय्यर की टिप्पणी के बाद इस पर कोई प्रमाण देने की ज़रूरत नहीं रह जाती। बच्चन सिंह के फैसले के बाद खेद जताते हुए कुछ जजों का ये सोचना था कि “दुर्भाग्य” से उस फैसले ने और अधिक मृत्युदंड देने से उन्हें रोक दिया!
 |
| जस्टिस पसायत को फांसी की सजा सुनाने में विशेषज्ञता हासिल है! |
भारत में मृत्युदंड की नींव बच्चन सिंह (के फ़ैसले) से रखी गई और उसके बाद के फ़ैसले से ये उम्मीद रखी गई कि वो उसके अनुरूप ही रहे। बच्चन सिंह मामले में ये साफ़ हो गया कि जजों को अपराध के जुड़ी परिस्थितियां और अपराधियों से जुड़ी परिस्थितियां, दोनों तरफ देखनी चाहिए। हालांकि कुछ जघन्य अपराधों और आतंकवाद के मामलों में न्यायिक सतर्कता थोड़ी दूसरी तरफ़ डिग जाती है जोकि अपराध से पैदा हुई तब्दीली के कारण ज़्यादा होती है। एक व्यक्ति रावजी ने अपने परिवार का क़त्ल किया क्योंकि उसे शक था कि उसकी पत्नी उसके प्रति वफ़ादार नहीं है और उसके बच्चे नाजायज़ हैं। अब इस मामले में वो अगर अपराध की परिस्थितियों को देखें तो निश्चित तौर पर अपराधी को फांसी की सजा सुना देंगे, लेकिन अगर अपराधी की परिस्थिति पर वो ग़ौर करें तो वो उसे शायद मानसिक तौर पर विक्षिप्त करार दें और उसके बाद बहुत संभव है कि उसे क्षमादान मिल जाए या फिर फांसी का फंदा। लेकिन अपराध इतना भयानक और स्तब्धकारी है कि इसे आगे घटित नहीं होना चाहिए! इसलिए एक क़ानून बना कि ऐसे जघन्य मामलों में अपराधियों से जुड़ी परिस्थितियों पर हमें विचार करने की ज़रूरत ही नहीं है। इन मामलों में सिर्फ़ अपराध के इर्द-गिर्द की परिस्थितियों को परखा जाना चाहिए! और इस तरह रावजी को फांसी के तख़्त पर भेज दिया गया।
बच्चन सिंह के मामले में तय किए गए सिद्धांत के मुताबिक़ क़ानून चलने लगा। इसी तरह सुरजा राम को फांसी हुई। और इसके अगले एक दशक में 12 लोगों को फांसी पर झुलाया गया। लगभग 15 लोगों को इस ग़लत सिद्धांत के आधार पर मौत की सजा मुकर्रर हुई। 2009 में सुप्रीम कोर्ट ने रावजी के अलावा सात और मामलों को ग़लत बताया और कहा कि इसमें क़ानूनी चूक हुई थी। इसके बाद दो और खंडपीठों ने यही निष्कर्ष निकाले। लेकिन तब तक फांसी के फंदे पर झूल चुके रावजी सहित बाकी कैदियों के लिए बहुत देर हो चुकी थी। उसके बाद एक क़ैदी को किशोर घोषित किया गया और बाक़ी चार के मृत्युदंड को सरकार ने माफ़ कर दिया। सात क़ैदी मृत्युदंड की कतार में खड़े रहे, इसके बावज़ूद कि सुप्रीम कोर्ट ने अलग-अलग मामलों में ये माना कि उनके फ़ैसलों में चूक हुई है।
जब उच्च और उच्चतम न्यायलय के 14 जजों ने राष्ट्रपति से लिखकर इन मृत्युदंडों को माफ़ करने की अपील की तो उसके बाद एक सघन अभियान चलाया गया। इनमें सायबाना का मामला भी शामिल था। गृह मंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति ने हाल ही में सायबाना की दया याचिका ख़ारिज कर दी है। सायबाना को अब कभी भी फांसी के तख़्ते पर भेजा जा सकता है। बाकी छह क़ैदियों की दया याचिका पर फैसले अभी लंबित हैं।
सायबाना केस के बारे में मैं कुछ जानकारी देता हूं। भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 303 में एक उपबंध हुआ करता था कि अगर आजीवन कारावास काट रहा कोई व्यक्ति उसी दौरान दूसरी हत्या करता है तो उसे निश्चित तौर पर मौत की सजा मिलेगी। यह अनिवार्य मृत्युदंड था। 1983 में क़ानून के इस खंड को असंवैधानिक घोषित कर दिया गया। क़ानून में इस संशोधन के 20 साल बाद सायबाना पर 303 के तहत आरोप लगाए गए। यानी जिस समय विधि संहिता से उस उपबंध को हटा दिया गया उसके बाद उस विलुप्त क़ानूनी धारा के तहत उसे 'अनिवार्य मृत्युदंड' सुनाया गया। उसके वकील ने ट्रायल कोर्ट में जज के सामने यह बात रखी कि उनके मुवक्किल को जिस सेक्शन के तहत मौत की सजा दी गई है वो क़ानून में मौजूद ही नहीं है। यहां अनिवार्य मृत्युदंड और विवेकाधीन मृत्युदंड में फर्क़ को समझना ज़रूरी हो जाता है। विवेकाधीन मृत्युदंड में आरोपी के पास ये अधिकार होता है कि वो कोर्ट के सामने उन परिस्थितियों को जाहिर करें जिनके तहत उसने घटना को अंजाम दिया। कोर्ट उस पर विचार करने के बाद ये तय करता है कि मामले में सही सजा क्या मुकर्रर की जाए, क्योंकि ग़ौरतलब है कि सुप्रीम कोर्ट ने यह कह रखा है कि सुनवाई के वक़्त अपराध और अपराधी दोनों की परिस्थितियों को संज्ञान में लिया जाना चाहिए। इसलिए ऐसे मौक़े पर यह सुनवाई निर्णायक हो जाती है।
सायबाना केस में चूंकि जज ने धारा 303 के तहत कार्यवाही की, जहां अनिवार्य मृत्युदंड का प्रावधान है, इसलिए वहां सजा सुनाने के बीच किसी भी तरह की सुनवाई का या फिर परिस्थितिजन्य सबूत पेश करने का कोई मौका ही नहीं था। इस तरह सायबाना पर आरोप तय हुए। मामला जब उच्च न्यायालय में पहुंचा तो ग़लती की पड़ताल हुई कि आरोपित को धारा 303 के तहत दोषी ठहराया गया। धारा 303 को विधि संहिता से हटाने के 23 साल बाद की ये घटना है। फिर मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा। सुप्रीम कोर्ट ने ये पाया कि ट्रायल कोर्ट ने सायबाना पर धारा 303 के तहत आरोप तय किया है और उच्च न्यायालय ने धारा 302 के तहत फ़ैसले को बरक़रार रखा है। मामले में चूंकि रिकॉर्ड पर शमन परिस्थितियां दर्ज़ नहीं थी इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने धारा 302 के तहत मृत्युदंड को बरकार रखा। केस में धारा 302 कहीं से भी परिदृश्य में नहीं था और रिकॉर्ड भी उतना ही साफ़ था। जब मामले की कोई सुनवाई ही नहीं हुई तो शमन परिस्थितियां कैसे मौजूद हो सकती है? इसके बावज़ूद कि सुप्रीम कोर्ट ने बाद में मामले को PER INCURIAM (यानी जिस मामले का कोई वैधानिक प्रावधान न हो और नही किसी पुराने फैसले से उसके तार जुड़ते हो) बताया और 14 जजों ने राष्ट्रपति से लिखकर क्षमादान का समर्थन किया, राष्ट्रपति ने उसकी क्षमाचायना को अस्वीकार कर दिया।
 |
| फांसी किसको मिलती है, ज़रा अमेरिका के आंकड़े देखिए। भारत के मामले में ब्लैक को दलित-अल्पसंख्यक- आदिवासी-ग़रीब पढ़िए |
अब राजीव गांधी हत्याकांड पर आते हैं। ट्रायल कोर्ट में 26 लोगों पर राजीव गांधी की हत्या का मुकदमा चला। सभी 26 लोगों को दोषी पाया गया और सबको मौत की सजा सुनाई गई। उनपर टाडा के तहत आरोप तय किए गए, जहां से हाई कोर्ट में अपील का कोई प्रावधान नहीं था क्योंकि वो फास्ट ट्रैक कोर्ट की तरह काम कर रहा था। इसलिए मामला सीधे सुप्रीम कोर्ट पहुंचा। सुप्रीम कोर्ट ने मृत्युदंड की सजा पाए 26 में से 19 लोगों को बरी कर दिया। पहले सुनाए गए फैसले और बाद में सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बीच के विशाल अंतर को देखिए! न्यायव्यवस्था में कुछ तो भयानक गड़बड़ी है कि पहले यह 26 लोगों के नाम मौत की सजा का फरमान जारी करती है और पहली चुनौती में ही 19 को दोषमुक्त बताती है। बचे हुए सात लोगों में से चार को सुप्रीम कोर्ट ने मृत्युदंड सुनाया। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के मुताबिक उनमें से एक लड़के का दोष महज इतना है कि उसने उन लोगों के लिए 14 वोल्ट की बैटरी लाने का काम किया जिन्होंने धानू में बम प्लांट किया था।
मैंने पहले ही ये कहा है कि सामान्य क़ानून के तहत आत्म-स्वीकृति को सबूत के तौर पर नहीं स्वीकारा जाता लेकिन टाडा जैसे विशेष क़ानून के तहत आरोपी की स्वीकृति को सबूत समझा जाता है। राजीव गांधी हत्या मामले में इन सात लोगों की आत्म-स्वीकृति को रिकॉर्ड किया गया, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इस दलील को माना कि वहां पर टाडा के तहत गिने जाने वाले अपराध को नहीं माना जाएगा। इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें टाडा से मुक्त कर दिया। अब अगर टाडा उन पर लागू ही नहीं होता तो उनकी आत्म-स्वीकृतियों को भी बतौर सबूत ख़ारिज कर दिया जाना चाहिए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा 'नहीं'। सुप्रीम कोर्ट का कहना था कि चूंकि उन्हें टाडा के तहत पकड़ा गया है और टाडा यह कहता है कि आत्म-स्वीकृति को दोष साबित करने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है इसलिए उसे पूरी तरह ख़ारिज नहीं किया जा सकता। तो कल को आप एक ऐसे चोर को टाडा के तहत दोषी मानते हुए पकड़ते हैं, जिनपर और कोई दूसरे आरोप न हो, तो टाडा के अलावा चोरी के तहत दोषी पाए जाने पर उनका क्या करेंगे? इस तरह के जजों की तर्क पद्धति यही है कि उन्हें आतंकवाद के मामलों से तो बरी कर दिया जाए लेकिन चोरी की सजा मिले!
मनमाना होने के अलावा मृत्युदंड भेदभाव से भी भरा हुआ है। जस्टिस कृष्णा ने राजेंद्र प्रसाद के मामले में ये महसूस किया कि मृत्युदंड में वर्गीय नज़रिया शामिल था। जिन 12 निर्दोष क़ैदियो को फांसी हुईं उनमें से 12 का मुकदमा सरकारी ख़र्चे पर लड़ा जा रहा था। आम तौर पर मृत्युदंड वाला मामला 6-9 महीनें तक खिंचता है। ज़्यादातर जगहों पर सरकारी वक़ीलों को एक मृत्युदंड के मामले में 500 से 2000 रुपए भुगतान किए जाते हैं, ट्रायल और हाई कोर्ट में यही दर है। सुप्रीम कोर्ट में अपील जाने पर उन्हें 4000 रुपए दिए जाते हैं। दशकों से यह फीस यहीं पर अटकी हुई है और इसमें आने-जाने और विविध मदों में होने वाले ख़र्चों को शामिल नहीं किया जाता। क़ानूनी सहायता के नियम के मुताबिक़ मृत्युदंड के हर मामले में किसी वरिष्ठ वकील को केस लड़ने का प्रावधान है, लेकिन विरले ही ऐसा हो पाता है। नए अनुभवहीन रण बांकुड़ों को केस की लगाम थमाकर अनुभवी अहाते से बाहर खड़े रहते हैं। इसमें कोई हैरत की बात नहीं कि जिस कोर्ट में अपील होती है वो ज़्यादातर ऐसे मामलों को वापस ट्रायल कोर्ट में भेज देती है, क्योंकि वहां पर क़ैदी का ठीक तरीके से बचाव ही नहीं होकर आता। लेकिन इनमें से ज़्यादातर मामलों में जहां-तहां दरार पड़ी होती है। इसलिए ये चौंकाने वाला तथ्य नहीं है कि फैसलों में लापरवाही, ग़लत तरीके से आरोप तय करने से लेकर फ़ांसी तक की सजा को (सरकारी) क़ानूनी सहायता से नहीं लड़ा जा सकता। मृत्युदंड के ऐसे क़ैदी जो ग़रीबी की मार झेल रहे हो उन्हें मामूली सरकारी चंदे वाली क़ानूनी सहायता देकर फिर से उस चक्र में झोंक दिया जाता है।
संविधान में हरेक नागरिक को क़ानून से सामने समानता का अधिकार हासिल है, जिसका मतलब है कि किसी की वित्तीय क्षमता को ध्यान में रखे बग़ैर मुकदमा में सबको समान फ़ैसला मिलेगा। अदालत को इस वायदे का निर्वाह करना चाहिए क्योंकि न्यायिक वैधानिकता की वो जड़ है। चूंकि मृत्युदंड में अब तक ऐसी समानता, स्थिरता और साफ़गोई देखने को नहीं मिली है, इसलिए इसका उन्मूलन होना चाहिए। नहीं तो, ईर्ष्या के एवज में हुई हत्या और न्यायिक हत्या में क्या फ़र्क रह जाएगा?
***************
अब तीसरे भाग की तरफ़ चलते हैं। फांसी देने के तरीकों पर बात करते हैं। ऐतिहासिक तौर पर क्षमादान की शक्ति प्रभु वर्ग के हाथ में निहित है। इस शक्ति को बनाए रखने का यह बेहतर तरीका है। ये एक जरिया है ताकि न्यायिक प्रशासन की ग़लतियों को भी दुरुस्त किया जा सके। ग़ुस्सैल फ़ैसले पर ठंडा पानी छिड़कने के लिए यह प्रावधान है। न्याय के अर्थ का दायरा जिस हद तक व्यापक है वहां तक क़ानून नहीं पहुंच सकता। इसलिए इस शक्ति को बनाए रखना ज़रूरी भी है। यही वजह है कि लगभग सारे देशों के पास क्षमादान की व्यवस्था है। लेकिन अगर क्षमादान की शक्ति के इस्तेमाल के तौर-तरीकों पर नज़र दौड़ाएं तो आप पाएंगे कि सरकार के लिए अलग-अलग तात्कालिक मुद्दों से मुंह चुराने के लिए यह हथकंडे के तौर पर उभरी है। आप अजमल कसाब की फांसी के समय को देखिए। आप सिर्फ़ समय को देखते रहिए। अजमल, अफ़जल सबके समय को। 2001 में संसद पर हुआ, 2005 में सुप्रीम कोर्ट ने फ़ैसला सुनाया, 2013 में अफ़जल को फांसी पर लटकाया गया। आठ साल बाद और संयोग से आज ही (9 फरवरी)। मैं यह कह सकता हूं कि संसद भवन पर हमले के जुर्म में उसे फांसी नहीं दी गई है। आठ साल से क्षमा चायिका को लंबित रखा गया और आज उस समय, जब यूपीए सरकार को राष्ट्रीय सुरक्षा, अपराध सहित कई मोर्चों पर बीजेपी पीछे धकेल रही है, अचानक उसे फांसी चढ़ा दी गई। संसद का सत्र इस बार भी जल्द ही शुरू होने वाला है, ठीक वैसे ही जैसे कसाब की फांसी के बाद हुआ था।
 |
| मृत्युदंड-विरोधी आंदोलन दुनिया के कई देशों में लंबे समय से चल रहा है। |
फांसी के तरीकों और निहितार्थ पर सवाल ज़रूर उठने चाहिए। संविधान की धारा 21 अपरिहार्य रूप से सारे मनुष्य पर लागू होती है, उन पर भी जो भारत का नागरिक नहीं है। अनुच्छेद 21 कहता है कि क़ानूनी रूप से स्थापित प्रक्रियाओं के अलावा किसी भी व्यक्ति को उसकी ज़िंदगी और निजी आज़ादी से बेदख़ल नहीं किया जा सकता। और सुप्रीम कोर्ट के मुताबिक़ वो क़ानूनी प्रक्रिया निष्पक्ष, उचित और तर्कसंगत होनी चाहिए। अगर आप किसी व्यक्ति की ज़िंदगी लेने जा रहे हैं तो आप इन क़ानूनी प्रक्रियाओं के तहत ही ऐसा कर सकते हैं। क़ानूनी तौर पर ये प्रक्रिया क्या है? इस मुद्दे पर सरकारी नियम कहता है कि जब कोई क्षमा याचिका दायर की जाती है तो उस याचिका को ख़ारिज करने के बाद उस व्यक्ति को सूचित किया जाना चाहिए जिसने वो याचिका दायर की है। क़ैदी और परिवार के सदस्यो को याचिका ख़ारिज किए जाने और फांसी की तारीख़ के बारे में पहले से सूचित किया जाना चाहिए।
कसाब के मामले में जब याचिका ख़ारिज की गई तो एक पत्रकार ने इस मामले पर आरटीआई किया और ख़ारिज किए जाने के एक दिन बाद उन्हें लिखित में जवाब आया कि वो मामला अभी भी लंबित है! ऐसे झूठ बोलने की ज़रूरत क्यों है? एक सरकार को झूठ नहीं बोलना चाहिए। ख़ुद सरकार द्वारा तय की गई प्रक्रिया का उल्लंघन करने की ज़रूरत क्यों आन पड़ती है? सरकार के पास पहले से जब कसाब को फांसी देने के न्यायिक वारंट मौजूद है तो बिना उसके परिवार को इत्तला किए और दुनिया को अंधेरे में रखकर वो क्यों फांसी दे रही है? उसके पास उसके परिवार का पता मौजूद है। बड़ी तादाद में लोगों ने कसाब के लिए क्षमादान की याचिका लगाई। उन्हें इस बात की कोई भनक तक नहीं है कि उनकी याचिका ख़ारिज की जा चुकी है। नियम के मुताबिक़ याचिकाकर्ता को ये सूचना अनिवार्य तौर पर दी जानी चाहिए। नियम ऐसा क्यों कहता है? क्योंकि अंतिम सांस तक किसी व्यक्ति को न्यायिक उपचार का अधिकार हासिल है और सुप्रीम कोर्ट के मुताबिक़ अगर दया याचिका को ख़ारिज किए जाने में लंबा वक़्त लगता है तो वह फिर से सुप्रीम कोर्ट जाकर अपने मृत्युदंड को माफ़ करने के लिए अर्जी लगा सकता है। अगर अधिकार मौजूद है तो उसका इस्तेमाल होने देना चाहिए। इसलिए याचिका ख़ारिज किए जाने और फांसी की तारीख़ के बीच के खंड में आरोपी इस अधिकार का इस्तेमाल करता है। लेकिन अजमल कसाब और अफ़जल गुरु, दोनों को यह मौका नहीं दिया गया। कसाब की फांसी के बाद केंद्रीय गृह मंत्री और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री ने आधिकारिक तौर पर ये कहा कि उन्होंने कसाब को गुपचुप फांसी इसलिए दी क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि लोग कोर्ट का रुख करे।
अफ़जल गुरु की फांसी के बाद गृह मंत्री ने इसे फिर दोहराया। लोकतंत्र के लिए यह एक हैरतअंगेज़ कथन है। देश के गृह मंत्री द्वारा विधि सम्मत नियम की यह बेशर्म उपेक्षा है। क्या हम पुलिस राज्य में नहीं तब्दील होते जा रहे हैं? अफ़जल गुरु के पास पत्नी थी, परिवार था और वो भी दिल्ली से बहुत दूर नहीं। विधि संहिता द्वारा एक क़ैदी को उनसे मिलने का जो अधिकार प्राप्त है उससे उनको वंचित नहीं किया जाना चाहिए। पहले कसाब के साथ उन्होंने ऐसा किया और अब अफज़ल गुरु के साथ।
हाल ही में ये दिखाने के लिए कि वो महिला अधिकार को लेकर कितने सचेत और अपराध पर कितने अड़ियल है, भूतपूर्व सब इंस्पेक्टर और हमारे मौजूदा गृहमंत्री ने गौरवान्वित भाव से ये कहा कि वे किसी भी बलात्कारी के मृत्युदंड की क्षमा चायिका को कभी भी स्वीकार नहीं करेंगे। जाहिर है, इससे महिलाओं के लिए सड़कें ज़्यादा महफ़ूज हो जाएंगी, ठीक वैसे ही जैसे कसाब को फांसी चढ़ाने से भारत पर आतंकवादी हमले बंद हो गए और जिस तरह सायबाना और दास को फांसी चढ़ाने से दोहरी हत्याकांड देश से विलुप्त हो जाएंगी! फांसी और इसके समर्थन में उठी आवाज़ें राजनेताओं के लिए रंगमंच की सामग्री का काम करती है और इस बिनाह पर वो दावा करते हैं कि अपराध पर वो बेहद सख़्त हैं। अपराध के कारणों की तह तक पहुंचने और भविष्य में किसी भी तरह के हमलों से बचने के लिए सुरक्षा के जो अनिवार्य, लेकिन मुश्किल और जटिल, तरीके हो सकते हैं उनपर तवज्जों देने और उसे सुलझाने के बजाए एक व्यक्ति के जीवन का दांव लगाकर बेहद आसान और सस्ते तरीके से लोगों के ग़ुस्से को ये कहकर शांत कर दिया जाता है कि इन समस्याओं से निजात दिलाने के लिए ऐसे कदम की सरकार को दरकार है!
वास्तव में मृत्युदंड ध्यान भटकाव का एक ठोस तरीका है ताकि सरकार ऐसे मुद्दों से लोगों का ध्यान हटा सके जिनपर चर्चा सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। यह लोगों के भीतर अपनी सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए जो ख़ून की भूख उठती है उसे तुष्ट करने का जरिया है। लेकिन जैसा कि हम जानते हैं कि एक व्यक्ति की मौत से मौजूदा समस्या शांत नहीं होती और न ही स्थाई तौर पर किसी भी मामले का निदान होता है, अलबत्ता इससे मामला ढंक-छिप ज़रूर जाता है। राज्य-समर्थित फांसी विपत्ति के समय ख़ून की हमारी प्यास को बुझाने के अलावा और कुछ नहीं करती। ख़ून के इस प्यास को बुझाने की कवायद और राज्य द्वारा किसी अपराधी को बधिया करने जैसे सजा के नए ख़यालात हमारे समाज से हिंसा ख़त्म करने की बजाए हमें और ज़्यादा हिंसक समाज में तब्दील कर देगा। अगर हमें नैतिक और करुणादायक समाज के रूप में ख़ुद को विकसित करना है और अपने बच्चों के सामने कम हिंस्र समाज का मॉडल ले जाना है तो हमें अपने भीतर से ऐसे ख़ूनी प्रतिकार के भाव को तजना होगा।
एक फांसी के पीछे के सच हैं: न्यायिक चूक, मनगढ़ंत सबूत और कार्यान्वयन में हेरा-फेरी। इन्हीं तीन के मिश्रण से फांसी संपन्न होती है। मौत की सजा आम तौर पर रहस्यमयी क़ानूनी जिरह के बाद मटमैले कोर्टरूम में सुनाई जाती है जिन्हें समझना आम आदमी के लिए बेहद मुश्किल है। फिर ऊंची दीवारों से घिरे जेल परिसर में इसे अंजाम दिया जाता है। हालांकि व्यक्ति को मारकर सजा देने के राज्य के अधिकार पर ख़ूब चर्चा हुई हैं, लेकिन क़ैदी को जेल की खोली से फांसी के चबूतरे तक ले जाने की प्रक्रिया अभी भी गुप्त है। चूंकि हमारे नाम पर फांसी दी जाती है, इसलिए इसे जानने और अपनी पसंद तय करने का हमें पूरा हक़ है
*युग मोहित चौधरी मुंबई उच्छ न्यायालय में अधिवक्ता हैं और भारत में मृत्युदंड के ख़िलाफ़ सक्रिय तौर पर अभियान चलाने वाले गिने-चुने लोगों में शुमार हैं।
**शाहिद आज़मी की 11 फरवरी 2010 को 32 साल की उम्र में उसके दफ़्तर के बाहर गोली मारकर हत्या कर दी गई। उस वक़्त शाहिद आतंकवाद से जुड़े मसलों का केस लड़ रहे थे, जिनमें मालेगांव धमाकों में झूठे आरोप लगाकर पकड़े गए और 26/11 मुंबई हमलों के आरोप में गिरफ़्तार किए गए लोगों के मामले शामिल थे।