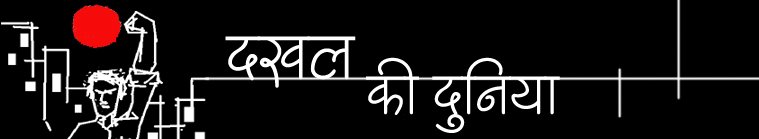राजा
की मौतें कई बार हुई और राजशाही धीरे-धीरे
मरी. राजा
को कभी मरना नहीं था. उसे
जिंदा रहना था. वह
ईश्वर का दूत था, वह
उसका अवतार और उसका पुत्र था. ईश्वर
के बच्चे की मौत जब हुई तो यह तयशुदा माना गया कि ईश्वर भी मर सकता है. सैद्धांतिक
तौर पर ईश्वर की मौत राजा की मौत के साथ हो गई. यह
दो सौ बरस से भी पहले की बात है. यह
तब की बात है जब रेलगाड़ी का पहला इंजन पटरियों पर नहीं आया था. यह
तब की बात भी है जब इंसान थोड़ा मजबूत हो रहा था और ईश्वर थोड़ा कमजोर. ये
पारस्परिक संबंध थे इन्हें इसी तरह विकसित होना था. एक
की मजबूती दूसरे की कमजोरी बननी थी. दुनिया
में इसके पहले के यकीन और आस्थाएं भिन्न थे. इस
आस्था और यकीन की मौत के पहले यह जरूरी था कि दूसरे यकीन और आस्थाएं बनाई जाएं. ऐसी
यकीन और आस्थाएं जो प्रचलन में लाई जा सकें. अदृश्य
सत्ताओं के सवालों के जवाब अबूझ और अदृश्य ही हुआ करते थे. राजशाही
जिन मूल्यों पर खड़ी थी वह विघटित हो गई. वर्तमान
में संचालित व्यवस्थाएं इसी विघटन की उपज रहीं. एक
नई व्यवस्था और नए मूल्यों में यकीन की प्रक्रियाएं शुरू हुई. सत्ता
के ढांचे एकहद तक बदल गए पर इस बदलाव में जो नही बदला वह सत्ता पर कब्जेदारी वाला वर्ग. प्रत्यक्ष
राजनैतिक सत्ता के अलावा हर समाज में एक ऐसा वर्ग बना रहा जो सामाजिक हैसियत को विभिन्न रूपों में कायम रखते हुए वर्चस्व बनाए रहा. समाज
पहले भी सोपानों में थे और समता, समानता
बंधुत्व के नारे के दो सौ साल बाद भी ये सोपानों में ही रह गए. यह
एक खोखला नारा साबित हुआ. यह
नीचे के सोपानों से ऊपर के सोपानों को वैद्यता हासिल करने का तरीका भर था. ऐसे
नारे उस समय की जरूरत थे और ये आज भी जरूरत बने हुए हैं. जो
सामाजिक हैसियत और वर्चस्व को कायम रखने में कारगर हुए. राजा, उप-राजा
या जमीदार, सेनापति, सिपाही का जैसा सोपान था यदि गौर करें तो लोकतांत्रिक पद्धति में यही बदलाव आया कि इसकी प्रक्रिया बदल गई. ऐसा
ही एक नया ढांचा सत्ता ने दूसरी प्रक्रिया के जरिए तलाश लिया. लोगों
की भागीदारी ही एक बड़ी गुमराही बनी. यहां
फिर से यह कहना जरूरी है कि सामाजिक परिवर्तन की स्थिति में सत्ताएं मोहलत देती हैं. वे
टूटती हैं और एक नए रूप में खुद को मजबूत करती हैं. किसी
व्यवस्था को टूटने की जरूरत उसके आंतरिक संरचनाओं में निहित होती है. ऐसी
कोई भी सत्ता संरचना विवादहीन नहीं हो सकती जिसके भीतर असमानताओं की उपज लगातार बनी हुई हो. इन्हीं
असमानताओं, द्वयम
व्यवहारों की खि़लाफत भिन्न-भिन्न
रूपों में उपजती थी/है
और उपजती रहेगी. ऐसे
में पैदा हुए क्षोभ, उत्पीड़न
और आक्रोश लंबे समय तक दबाए जा सकते हैं पर उन्हें खत्म नहीं किया जा सकता. जब
तक कि उसके कारण को न खत्म
किया जाए. कारणों
के विश्लेषण बेहद अहम होते हैं. इन्हें
कई-कई
रूपों में प्रस्तुत किया जा सकता है. जैसे
गरीब होने को काम न करने
के साथ जोड़ दिया जाए. जैसे
भुखमरी के कारण को कम उपज बता दिया जाए. जैसे
तूफान, भूकम्प, बाढ़ को महज प्राकृतिक आपदा बता दिया जाए. प्राकृतिक
आपदाओं के वैज्ञानिक कारणों पर चर्चाएं की जाएं पर चर्चाओं को वैज्ञानिक प्रक्रियाओं तक समझाने के लिए ही रखा जाए. जबकि
बड़े पैमाने पर दुनिया की व्यवस्थागत उत्पादन और प्रक्रियाएं प्राकृतिक आपदाओं का कारण बन रहे हैं. व्यवस्था
जनित आपदाओं के चेहरे बदल दिए जाते हैं. इसके
स्वरूप यदि बदल दिए जाएं तो यह गुमराही जरूर पैदा कर सकता है. लोग
अपने जीवन में कुछ बदलने का इंतजार करते हैं. वे
लंबे समय तक सब्र रखते हैं, फिर
वे आक्रोशित भी होते हैं और उन्मादित भी. यदि
परिस्थितियां समग्रता में राजनैतिक समझ बनाती हैं तो समाज का संक्रमण की स्थिति में जाना संभव बनता है. इसलिए
संक्रमण के दौर परिवर्तनकारी भी होते हैं और फासीवादी भी होने की संभावनाएं बनी रहती हैं. परिवर्तन
की जरूरत और मसक्कत वही करते हैं जो स्थितियों की विद्रूपताओं में फंसे होते हैं. ऐसे
में सत्ता अपनी संभावनाओं के नए गलियारे तलाशती है. वह
थोड़ा सा बदलाव करती है और लोगों के आक्रोश से उसे मोहलत मिलती है. सत्ताओं
ने असमानता से उपजे आक्रोशों में हमेशा एक मोहलत को तलाशा है.
वर्तमान
में भारतीय राजनीति इन्हीं स्थितियों से गुजर रही है. पूरे
देश में छोटे-छोटे
आंदोलनो के उभार और आक्रोश हैं. पूरा
का पूरा पेड़ सूखते हुए पीलेपन की तरफ बढ़ रहा है. जबकि
पूरी चर्चाएं पेड़ के अलग-अलग
पत्तों के सूखने और पीले हो जाने पर भिन्न-भिन्न
स्वरों में उठ रही हैं और उठाई जा रही हैं. समस्याओं
को जब इस तरह से उठाया जाता है तो वह पेड़ को बचा लेने की गुंजाइश का एक हिस्सा होता है. यह
बहुत चालाक किस्म से किया जा रहा प्रयोग है जिसमे जड़ों की तरफ बात करना फलदायी नही है. इन
वक्तों में बस शब्दों में कुछ नए अर्थ भर दिए जाते हैं और कुछ नए शब्द प्रचलित कर दिए जाते हैं. पूजी
केन्द्रित जरूरतों, उसकी
पूर्ति के लिए किए जाने वाले तमाम प्रयासों और पूजी जनित विद्रूपताओं को ‘भ्रष्टाचार’ कह दिया जाता है. फिलवक्त
यह एक ऐसा शब्द है जो राजनीति में अवमूल्य बना हुआ है. जिसके
बरक्स ईमानदारी को एक मूल्य के रूप में खड़ा किया जा रहा है. इस
शब्द के तहत एक नया मूल्य इस तरह गढ़ दिया गया है मानो यही एक खामी है जो हमारी विकट स्थितियों का कारण बनी हुई है. वर्गीय
असमानताओं से जो एक खाई बनी थी उसमे आम आदमी दमित हो चुका था और है. तब
एक नई पार्टी ही उसके नाम से खड़ी कर दी जाती है. अब
आम आदमी, उससे
जुड़े सवाल और उससे जुड़े सरोकार की जो सामाजिक स्मृति बनी थी उस पर एक पार्टी की पैठ हो जाती है. देश
में आम आदमी पर बात करना एक जुमला बन जाता है.
पुरानी
बहसें भुला दी जाती हैं और सत्ता हमे नई बहसों में गुमराह कर देती है. पुरानी
बहसें वह थी जब पानी जैसे प्राकृतिक संपदाओं पर सबके अधिकार की बहस हो रही थी, वह
नदी पर सबके बराबर हक़ की बहस थी और अब यह पानी के दाम कम कर दिए जाने या आधे कर दिए जाने तक आ पहुंची
है. जब
पानी के साथ खरीदने और बेचने के सरोकार सामाजिक स्मृतियों में बस जाएंगे तो प्राकृतिक संसाधनों के साथ एक नए तरह की बहस शुरू हो जाएगी. यह
धीरे-धीरे
एक ऐसे रास्ते पर जाना है जहां पुरानी स्मृतियां विलुप्त होती जाएंगी. समाज
नई समस्याओं से घिर रहा है और सत्ता के संस्थानों में नए रंगरूट कड़े नियम बनाने की दुहाई दे रहे हैं. उन
समस्याओं के समाधान नियमों और कानूनों के जरिए हल किए जा रहे हैं जिनकी जड़ें सांस्कृतिक हैं. कड़े
नियम बनने का आशय है कि हम सबको और बांधा जाएगा. समस्याओं
के समाधान हम अपनी बंदिशों के रूप में पाएंगे. जहां
व्यवस्था से उपजी बीमारियों के इलाज का खर्च हम नई बंदिशों और दमनकारी कानूनों के तहत अदा करेंगे. एक
बेहतर व्यवस्था में हमे एक ऐसे समाज की तरफ बढ़ना था जहां किसी भी सत्ता की ताकत से ज्यादा हम खुद को मुक्त कर पाते जबकि यह उस तरफ बढ़ना है जहां हम और भी बंधनों में घिर रहे हैं और घेरे जा रहे हैं.