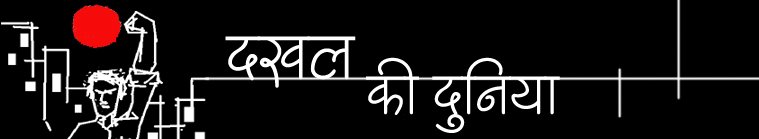अवनीश, अम्बाला से (संपर्क- 256avani@gmail.com)
उत्तर प्रदेश व बिहार के प्रवासी श्रमिकोंं के साथ दुव्र्यवहार का सिलसिला रुकने का नाम नहीं ले रहा है। कभी उन्हें असम के चरमपंथी गुटों की राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं का शिकार होना पड़ रहा है तो कभी शिवसेना और महाराष्ट्र नवनिर्माणसेना जैसे लम्पट समूहों के हाथों लुटना-पिटना पड़ रहा है। विभेद और अलोकतांत्रिकता की इस कड़ी में अब जालंधर (पंजाब) स्थित यूनियन बैंक ऑफ इंडिया की बस्ती नौ शाखा का नाम भी जुड़ गया है। इस शाखा ने हाल ही में पंजाब में काम कर रहे प्रवासी श्रामिकों को लेन-देन का काम करने के लिए सप्ताह में एक दिन ‘गुरुवार’ मुकर्रर करके रंगभेद की एक नई प्रथा शुरू करने का प्रयास किया है। गत दिनों इस बैक के ब्रांच मैनेजर ने उत्तर प्रदेश और बिहार के श्रमिकों को यह कहकर बैंक आने से मना कर दिया कि वे देखने में गंदे और जाहिल लगते हैं। उन्हें बैंक के कामों के बारे में जानकारी नहीं है और उनके कारण स्टाफ को परेशानी होती है। इस तैश में ही उस मैनेजर ने यह इलहाम भी कर दिया कि जलंधर की बस्ती नौ शाखामें उत्तर प्रदेश और बिहार के श्रमिकों का लेन-देन का काम केवल गुरुवार को किया जाएगा। इसलिए सप्ताह के अन्य दिनों में ये श्रमिक बैंक ना आएं। अब यह निर्णय बैंक मैनेजर की अपनी विवेकशीलता थी या प्रवासी श्रामिकों को लेकर बैंक की नीतियों में आए बदलाव का संकेत, यह कह पाना मुश्किल है।
घटनाक्रम के अनुसार गत २० दिसंबर को जलंधर के बस्ती दानिशमंदा इलाके की एक फैक्ट्री में काम करने वाला श्रमिक उदयवीर कोरबैंकिंग के जरिए अपने पैसे घर भेजने के लिए नजदीक की यूनियन बैंक की शाखा में पहुंचा। यह श्रमिक देवरिया जिले का रहने वाला है और इस बैंक से ही वह पहले भी अपने पैसे भेजता रहा है। लेकिन उस दिन बैंक कांउटर पर बैठे क्लर्क ने यह कहकर कि बाहरी लोगों के काम केवल गुरुवार को होंगे, उसके पैसे लेने से मना कर दिया । श्रमिक ने पैसे जमा करने की लिए मिन्नतें की लेकिन बात नहीं बनी। इसलिए वह वापस लौट गया और अपने फैक्ट्री मालिक को साथ दोबारा आया। उसने सोचा की शायद स्थानीय व्यक्ति के साथ होने पर उसके पैसे जमा कर लिए जाएं। लेकिन इस बार भी ऐसा नहीं हुआ । क्लर्क ही नहीं बैंक मैनेजर तरसेम जैन ने भी बाहरी लोगों के पैसे केवल गुरुवार को जमा करने की बात दोहराई। श्रमिक और फैक्ट्री मालिक ने जब मैनेजर से पूृछा कि बाहरी लोगों के पैसे गुरुवार को ही जमा होंगे इस बाबत आपने नोटिस कहां लगाई है ? इस पर मैनेजर उखड़ गया और उन दोनों बैंक से बाहर चले जाने को कहा। मैनेजर के इस रवैये से बैंक में हंगामा खड़ा हो गया। पैसा जमा न होते देख फै क्ट्री मालिक और श्रमिक दोंनो वापस लौट आए। वापस आकर फैक्ट्री मालिक ने पैसे जमा करने के लिए अपने छोटे भाई को भेजा और दिलचस्प यह रहा कि इस बार पैसे जमा कर लिए गए।
प्रवासी श्रमिक के साथ हुए इस दुव्र्यवहार के खबर सामने आते ही बैंक की इस शाखा की पंजाब में औद्योगिक, राजनीतिक और सरकारी स्तर पर जबर्दस्त आलोचना हुई, जिसके बाद यूनियन बैंक आफ इंडिया के उच्च पदाधिकारियों को माफी मांगनी पड़ी। बैैंक प्रबंधन ने ब्रांच मैनेजर का तबादला कर दिया और प्रेस विज्ञप्ति जारी करके कहा कि बैंक की सभी शाखाएं सभी ग्राहकों को सभी दिन सुचारु रूप से बैंकिंग सुविधाएं प्रदान कर रही हैं। इस संबध में यदि किसी ग्राहक या किसी व्यक्ति को असुविधा हुई तो इसके लिए खेद है। हालंाकि इस आपातकालीन कार्रवाई के बावजूद विरोध थमने का नाम नहीं ले रहा है और कई संगठनों ने बैंक प्रबंधन द्वारा सार्वजनिक रूप से माफी मांगने की अपील की है। इस मामले में अप्रवासी श्रमिक बोर्ड के चेयरमैन आरसी यादव ने जालंधर के पुलिस कमिश्रर गौरव यादव से मिलकर बैंक मैनेजर के खिलाफ कार्रवाई किए जाने की मांग की है। पंजाब में सक्रिय प्रवासी श्रमिकों के संगठन पूर्वांचल विकास महासभा ने रिजर्व बैंक आफ इंडिया के पास शिकायत दर्ज कराई है कि राज्य के कई बैंक प्रवासी मजदूरों के साथ भेदभावपूर्ण व्यवहार कर रहे हैं। सभा के अनुसार बैंको ने प्रवासी मजदूरों के लिए अलग कांउटर बना रखे हैं और उनको लेनदेन जैसे काम करने के लिए सप्ताह में एक दिन मुकर्रर किर दिया है। ऐसा करने की वजह बैंक में आने वाले सभं्रात ग्राहकों को होने वाली परेशानी बताई जा रही है। इस मामले में एक दिलचस्प बात यह सामने आई है कि प्रवासियों के लिए अलग दिन तय करने अथवा अलग काउंटर बनाने के निर्णय को बैंको ने ‘प्रिविलेज बैंकिं ग’ का नाम दिया है यानी एक ऐसी सुविधा जो केवल प्रवासी श्रमिकों को उपलब्ध कराई गई है। बैंकों के अनुसार इस विशेष सुविधा की वजह निरक्षर श्रमिकों को बैंको के कामकाज में आने वाली परेशानी है। इस सुविधा के जरिए उन्हें सप्ताह में एक दिन बुलाकर उनका कामकाज आसानी से निपटाया जा सकता है। यूनियन बैंक आफ इंडिया के प्रबंधन ने कहा कि ऐसा करने की वजह प्रवासी मजदूरों को सुविधाजनक बैंकिंग सेवाएं उपलब्ध करवाना है। प्रवासी श्रमिक किसी भी दिन आकर बैंक में लेनदेन का काम कर सकते हैं लेकिन गुरुवार के दिन जलंधर की सभी फैक्ट्रियों में अवकाश रहता है इसलिए इस दिन उनके लिए अलग से एक काउंटर खोल दिया जाता है।
अलग दिन और अलग काउंटर खोले जाने के बारे में बैंक जो भी वजह बताते हों लेकिन प्रवासी श्रमिकों के संगठनों ने इसे भेदभाव भरा कदम ही बताया है । प्रवासी श्रमिक संगठनों द्वारा ऐसा कहे जाने की वजह भी है। दरअसल पंजाब में प्रवासियों के साथ भेदभाव व शोषण नई बात नहीं है। पूर्वंचल विकास सभा के प्रवक्ता एके मिश्रा ने बताया कि पंजाब के बैंक मे भेदभाव की घटना पहली बार नहीं घटी है । इसके पहले लुधियाना में पंजाब नेशनल बैंक की गिल रोड स्थित शाखा में भी ऐसी ही वाकया हो चुका है। बैंक के अलावा आम जीवन में भी प्रवासी श्रमिकों को अक्सर भेदभाव का सामना करना पड़ता है। जालंधर में काम कर रहे पत्रकार चंदन मिश्रा ने बताया कि पंजाब में प्रवासी मजदूरों के साथ रेलवे टिकट काउंटर पर, डाक खाने में , स्कूलों में बच्चों का दाखिला करते समय अक्सर भेदभाव की घटनाएं होती हैं। रेलवे टिकट काउंटरों पर तो कई बार बाहरी मजदूरों को टिकट देने से भी मना कर दिया जाता है।
एक अनुमान के मुताबिक पंजाब में लगभग ४० लाख प्रवासी श्रमिक काम करते हैं, इनमें से अधिकतर उत्तर प्रदेश और बिहार के ग्रामीण क्षेत्रों से आते हैं। इन श्रमिकों ने पंजाब की अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण योगदान भी दिया। इसका अंदाजा बैंको में बचत के रूप में हर महीनें जमा होने वाली करोंड़़ों की रकम से लगाया जा सकता है। एक मजदूर अपनी रोजमर्रा की अर्थिक गतिविधियों द्वारा भी राज्य की अर्थव्यवस्था को मजबूत करता है। पंजाब में कई विधान सभा सीटों में भी प्रवासी मजदूर राजनीतिक रूप से सशक्त हैं, इसलिए राजनीतिक दल इनका इस्तेमाल वोट बैंक के रूप में भी खूब करते हैं। इन सबके बावजूद पंजाब सरकार ने कभी भी इनके लिए किसी प्रकार की सामाजिक सुरक्षा योजना या इनके हितों की रक्षा की लिए कोई कानून लाने की नहीं सोची। जबकि भारत के ही एक राज्य केरल में इस तरह के कानून भी है और योजनाएं भी। इस राज्य ने मई महीने में प्रवासी मजदूरों के कल्याण के लिए ‘प्रवासी मजदृूर कल्याण योजना’ भी लागू की है । इस योजना के तहत पंजीयन कराने के बाद हर प्रवासी मजदूर सलाना २५००० रुपए तक की चिकित्सा सहायता व बच्चों को पढऩे के लिए हर महीने ३००० रुपए का शैक्षणक भत्ता दिया जाता है। किसी दुर्घटना में श्रमिक की मृत्यु होने की स्थिति में उसके संबधियों को ५०००० रुपए की सहायता दी जाती है । इस योजना के तहत एक निर्धारित समय तक केरल में में काम करने के बाद राज्य छोडऩे की स्थति में २५००० रुपए का आर्थिक लाभ दिया जाता है। केरल मे भी अनुमानत: ३० लाख उत्तर भारतीय मजदूर काम करते हैं। केरल में इन मजदूरों की स्थिति स्थानापन्न मजदूरों जैसी है क्योंकि केरल की अधिकांश श्रामिक आबादी खाड़ी देशों में काम करती है। पंजाब में भी श्रमिक मजदूरों की स्थिति स्थानापन्न मजदूरों जैसी ही है। इस राज्य के भी अधिकांश श्रामिक अधिक पैसे और बेहतर अवसर की तलाश में विदेशों की ओर रुख कर चुके हैं। इस आबादी द्वारा पैदा की गई जगह को ही प्रवासी श्रामिकों ने भरा है। इसलिए ऐसा भी नहीं कि यहांं श्रमिकों की आबादी बहुत है और उनके पलायन की स्थिति में पंजाब अपनी अर्थव्यवस्था सम्हाल पाएगा! मनरेगा की सफलता के बाद पंजाब में प्रवासी कृषि मजदूरों की संख्या में आई कमी के बाइ यह बात जाहिर भी हो चुकी है। इस योजना के बाद पंजाब में मजदूरों की कमी के कारण ‘१०० रुपए पर भारी, एक बिहारी’ का जुमला आम तौर पर सुना जाता है।
श्रमिकों की पंजाब सरकार द्वारा की जा रही अनदेखी के बावजूद उतर प्रदेश और बिहार में प्रवासन एक ऐसी समस्या है जिसका हल निकाला जाना जरूरी है। पिछले ६० वर्षों में देश में जिस प्रकार असंतुलित और विसंगतिपूर्ण विकास हुआ है, उसके बाद आंतरिक प्रवासन एक सामान्य परिघटना हो चुकी है। ७० के दशक में हुई हरित क्रांति के बाद पंजाब में बहुपरतीय आर्थिक प्रगति हुई है। राज्य में कृषि क्षेत्र में अतिरेक के बाद कुटिर व लघुस्तर के उद्योगों का भी विस्तार हुआ। वैज्ञानिक व कृषि यंत्रों, होम आप्लयसेंज और स्पोर्टस के सामन बनाने के उद्योग पंजाब में पिछले तीन दशकों में खूब फले- फूले हैं। इसके परिणामस्वरूप यहां रोजगार के अवसर पैदा हुए हैं और गरीबी में जबर्दस्त कमी आई । जबकि इस दौर में उत्तर प्रदेश और बिहार में रोजगार का पहिया बिलकुल ही थमा रहा। केन्द्र सरकार ने उत्तर प्रदेश व बिहार की आर्थिेक प्रगतिके के लिए कभी कोई ठोस कार्यक्रम लागू करने का प्रयास नहीं किया। इन राज्यों की सरकारें भी कभी विकास की बाबत बहुत गंभीर नहीं रहीं। कृषि उत्तर प्रदेश और बिहार में रोजगार का अहम जरिया रही है। लेकिन पिछले दो दशकों में अर्थिक नीतियों में आए बदलाव के कारण इन राज्यों में खेती -बारी चौपट होती चली गई। जिसके परिणामस्वरूप जहां इन राज्यों में बेरोजगारी बढ़ी वहीं गरीबी और अपराध ने भी यहां अपनी जडेें़ जमा लीं। खेती -बारी के नष्ट होने का दुष्प्रभाव कस्बों और छोटे शहरों पर भी पड़ा। उत्तर प्रदेश और बिहार में कस्बे और छोटे शहर ग्रामीण आबादी की वाणिज्यिक गतिविधियों को प्रमुख केन्द्र रहे हैं । यहां मौजूद लाखों खुदरा दुकानों की जीवन रेखा इन क्षेत्रों की कृषि का अतिरेक ही रहा है। लेकिन खेतीबारी का खत्म होना कस्बों और छोटे शहरों के लिए प्राणघातक साबित हुआ। इन क्षेत्रों में रोजी रोटी के अवसर अब बिलकुल ही खत्म हो गए हैं और यहां कि श्रामिक आबादी पंजाब व हरियाणा जैसे संपन्न राज्यों की ओर रुख करने लगी है। आंकड़ों पर गौर करें तो २००४-०५ में पंजाब के ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी रेखा के नीेचे मात्र ९.०२ प्रतिशत आबदी रहती थी, जबकि उत्तर प्रदेश और बिहार में यह आबादी क्रमश:४२.१ और ३३.४ प्रतिशत थी। गरीबी रेखा के नीचे रह रही आबादी का यह अंतर उत्तरप्रदेश और बिहार की दुर्दशा की कहानी खुद बयां कर रहा है।
असंतुलित विकास के कारण हो रहे प्रवासन ने राजनीतिक समस्या का रूप भी ले लिया है। रोजगार के अवसर कम होने की स्थिति में मजदूरों पर क्या गुजरती है इसके उदाहरण महाराष्ट्र और असोम जैसे राज्यों में अक्सर ही देखने को मिलते रहते हैं। इन राज्यों में राजनीतिक दल इनके हितों को ही इंधन बनाकर अपनी रोटी सेंकते हैं और अपनी ताकत का मुजाहिरा करने के लिए इन श्रमिकों को ही अपना शिकार भी बनाते हैं । दरअसल प्रवासन में तेजी भी पिछले दो दशकों में ही आई है। पंजाब में ही गौर करें तो १९८१ की जनगणना में यहां उत्तर प्रदेश और बिहार के मजदूरों की संख्या क्रमश:२२०२१६ और ५८२३५ थी वहीं १९९१ में बढक़र संख्या २८०३५० और ९०७३२ हो गई। २००१ की जनगणना में ये संख्या ५१७३५१ और २६७४०९ हो गई। २००१ की जनगणना में पंजाब में प्रवासी मजदूरों में उत्तर प्रदेश और बिहार के श्रमिकों का प्रतिशत क्रमश: ३२.९२ और १७ .०१ हो गया । पंजाब में २००१ में प्रवासी श्रमिकों के बीच आधी आबादी उत्तर प्रदेश और बिहार के श्रमिकों की थी। जबकि इसी दौर में हिमांचल, हरियाणा और राजस्थान से पंजाब आए श्रमिकों की संख्या में कमी आई थी। ये आंकड़े भी दरअसल पिछले दो दशकों में हुए असंतुलित आर्थिक विकास की ओर ही संकेत कर रहे हैं। इसलिए आवश्यकता इस बात की है इन क्षेत्रीय विसंगतियों को समाप्त किया जाए और रोजगार के अवसर स्थानीय स्तर पर उपलब्ध कराने के प्रयास किए जाएं। लोकतंत्र होने के नाते सभी नागरिकों देश में कहीं भी काम करने की आजादी है , इसलिए आर्थिक संस्थाओं की भी जिम्मेदारी बनती है कि वे लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा के लिए प्रयास करें। बैंंको और व्यापारिक संगठनों से तो यह कतई अपेक्षा नहीं की जा सकती कि वे भेद भाव की प्रथा के पैरोकार बनेगें। इसलिए पंजाब में हुई घटना दोहराई नहीं जाएगी, इसकी उम्मीद की जानी चाहिए।