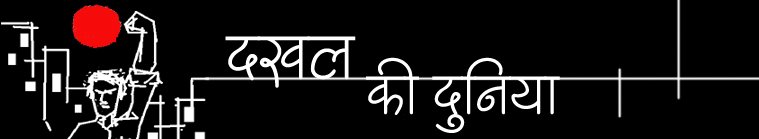दिलीप ख़ान
दादरी के बिसाड़ा गांव में 28 सितंबर की रात उन्मादी लोगों के एक समूह ने अख़लाक़ की गोमांस खाने की अफ़वाह के आधार पर हत्या कर दी। बिहार में चुनाव के मद्देनज़र उसी वक़्त से ये कयास लगाए जा रहे थे कि राजनीतिक फ़ायदा उठाने की कोशिश के चलते पश्चिमी उत्तर प्रदेश के एक छोटे से कस्बे की घटना बिहार की ज़मीन तक खींच लाई जाएगी। हफ़्ते भर चली तीखी बहस के बाद राष्ट्रीय स्तर पर इस घटना पर कई पक्ष उभरकर सामने आए। फ़िलहाल उन तमाम दलीलों, बहसों को स्थगित करते हुए अगर बिहार के सियासी रण में इस घटना के जुड़े तार पर नज़र दौड़ाएं तो ये साफ़ हो चला कि बीजेपी इस घटना को बिहार में भी बड़े मुद्दे के तौर पर उछाल रही है। घटना की आंच को बिहार में हिंदूवादी रंग में रंगने की कोशिश को बीजेपी इस तरह देख रही है कि धार्मिक गोलबंदी के ज़रिए जातिवादी खांचे में बंटे हिंदू समाज वो एक अस्मिता के तौर पर बांध लेगी।
पहले छिटपुट आरोप-प्रत्यारोपों का दौर चला और बाद में जब आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव ने ये बयान दिया कि हिंदुओं का भी एक तबका बीफ़ खाता है तो पूरे मामले ने बिहार में तूल पकड़ लिया। बीजेपी इसी तरह के बयान के फ़िराक में थी और 5 अक्टूबर को राज्य के पूर्व उपमुख्यमंत्री और बीजेपी नेता सुशील कुमार मोदी ने बाक़ायदा इस पर लंबा बयान देकर जनता को ये संदेश दिया कि महागठबंधन के नेता बीफ़ खाने की तरफ़दारी कर रहे हैं। सुशील मोदी ने कहा, “जहां नरेन्द्र मोदी ने बांग्लादेश सीमा पर चौकसी बढ़ाकर हज़ारों गायों को कटने से रोक दिया है, वहीं लालू-नीतीश और सोनिया गांधी गोमांस खाने की बात कर रहे हैं।” हालांकि ना तो सोनिया गांधी और ना ही नीतीश कुमार ने इस पर कोई बयान जारी किया, लेकिन बीजेपी ने समूचे महागठबंधन को इस राजनीति की आंच में एक कड़ाही में बंद कर दिया।
इसके बाद मीडिया ने जब इसको लपका तो लालू प्रसाद यादव को पीछे हटते हुए सफ़ाई देनी पड़ी कि वो पुश्तैनी तौर पर गाय पालते रहे हैं और गोरक्षा को लेकर उन्हें किसी भी तरह के स्पष्टीकरण की दरकार नहीं है क्योंकि नरेन्द्र मोदी और अमित शाह के मुक़ाबले गाय के प्रति उनका प्यार सार्वजनिक है। लालू प्रसाद शायद इस बयान में अपनी जातिगत पृष्ठभूमि को जाहिर करते हुए यादव और पशुपालन के संबंधों को रेखांकित करना चाह रहे थे। हालांकि वो सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायधीश मार्कंडेय काट्जू और सिने अभिनेता ऋषि कपूर के उदाहरण के ज़रिए इस बात पर भी अड़े रहे कि हिंदुओं का एक तबका बीफ़ खाता है और ये देश की हक़ीकत है।
बिहार के चुनाव को इस बार देश की राजनीति के लिए अहम बताया जा रहा है और इसके बाद पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश और केरल में होने वाले चुनाव के लिहाज से बीजेपी के लिए ये अहम पड़ाव है। लिहाजा, बिहार में बीजेपी ने इसे साख का सवाल बना लिया है और महागठबंधन की पार्टियों के लिए भी ये समीक्षा के आख़िरी मौक़ों में से एक है कि जिस राजनीति के आधार पर उन्होंने एकजुट होने का फ़ैसला लिया और “जनता दल’ का प्रयोग आख़िरी मौक़े पर समाजवादी पार्टी के अलग होने से बिखर गया, उसकी राह आने वाले दिनों में कहां तक पहुंच पाएगी?
अब दो प्रमुख मुद्दे उभरते हैं एक तो बिहार की राजनीति में बीफ़ पॉलिटिक्स की दरकार और दूसरा बीफ़ को लेकर प्रचलित मान्यताओं की हक़ीक़त। बढ़ती महंगाई से लेकर बेरोज़गारी, पलायन और बुनियादी सुविधाओं के अभाव से जूझते बिहार में विकास की बात हर पार्टी कर रही है और हर पार्टी का दावा है कि उनके लिए यही सबसे बड़ा एजेंडा है, लेकिन इन बयानों के समानांतर ये भी साफ़ हो चला है कि पहले के मुक़ाबले कहीं ज़्यादा गहरे स्तर तक ये चुनाव जातिगत और धार्मिक आधार पर लड़ा जा रहा है। महागठबंधन के भीतर जहां आरजेडी मंडल-2 की बात उछालकर सामाजिक न्याय और सोशल इंजीनियरिंग को अपना प्रमुख एजेंडा बनाकर प्रचार कर रही है, वहीं दूसरी तरफ़ उसकी सहयोगी जेडीयू अपने प्रचार में विकास और नीतीश सरकार के काम-काज को रैलियों में तरजीह दे रही है। यानी दोनों पार्टियों ने रणनीतिक तौर पर मतदाताओं के लिए मुद्दे बांट लिए हैं। लालू प्रसाद यादव को तो अगड़े-पिछड़े पर दिए गए एक बयान के बाद चुनाव आयोग ने नोटिस भी भेज दिया।
जातिगत समीकरण के लिहाज से बीजेपी के लिए इस चुनाव को मुफ़ीद नहीं माना जा रहा है, लिहाजा उसके लिए जातिगत अस्मिता को धार्मिक अस्मिता के लबादे से ढंकना फ़ायदे का सौदा है। बीफ़ एक ऐसा शब्द है जो राजनीतिक तौर पर हिंदू पहचान को समेटने की कोशिश में क़ामयाबी देने का माद्दा रखता है। ये अलग बात है कि ऐतिहासिक तौर पर और इस वक़्त भी हिंदुओं का एक तबका बीफ़ खाता ज़रूर है लेकिन राजनीतिक माहौल में बीफ़ को धार्मिक पहचान का मुद्दा मानते हुए वो लकीर के एक तरफ़ खड़ा हो सकता है।
इस पूरे मामले में ग़ौरतलब बात ये है कि बिहार में जातीय पहचान को दरकिनार करने की दो कोशिशें हुईं और दोनों बीजेपी के चलते। एक कोशिश बीफ़ की और दूसरी बिहारी उपराष्ट्रवाद की। नरेन्द्र मोदी ने बिहार में मुज़फ़्फ़रपुर की पहली चुनावी रैली में जब नीतीश कुमार को लेकर डीएनए वाला बयान दिया तो महागठबंधन ने इसे 180 डिग्री मोड़ते हुए बिहारी अस्मिता पर चोट करार दिया। डीएनए जांच करने के लिए कैंप लगाने की राजनीतिक नौटंकी हुई और मामला कुल ऐसा बना कि बिहारी नाम की कोई एक पहचान बिहार के भीतर रह रहा है जिसको अपमानित किया गया। शैवाल गुप्ता ने इसे बिहार के सुसुप्त राष्ट्रवाद को उछालने का मामला बताया। यानी, जिस तरह तमिलनाडु में तमिल अस्मिता, पश्चिम बंगाल में बांग्ला अस्मिता भारतीय राष्ट्रवाद के समानांतर चलती रहती है उस तर्ज पर उत्तर भारत में कभी भी उपराष्ट्रवाद सतह पर नज़र नहीं आया।
डीएनए और स्पेशल पैकेज देने के वक़्त नरेन्द्र मोदी की भंगिमा को जिस तरह महागठबंधन ने बिहारी अस्मिता से जोड़ा वो इस चुनाव में पहली बार बिहारियों को एक ठोस आइडेंटिटी के नीचे खड़ा कर दिया। दूसरी तरफ़ बीजेपी ने बीफ़ को हिंदू अस्मिता के साथ जोड़ते हुए जातीय पहचान को पाटने की कोशिश की। बड़ा सवाल तो ये है कि दोनों गठबंधनों के बीच जिस चुनाव को सीधा मुक़ाबला माना जा रहा है, क्या उसमें जातियों के चक्रव्यूह को भेदने की कोशिश में दोनों आश्वस्त नहीं है?
तीसरा मामला ये है कि बीफ़ को लेकर जिस तरह की अफ़वाह दादरी से लेकर बिहार के मैदान तक फैलाई गई, उसकी सच्चाई क्या है? राजनीतिक बिसात पर बीफ़ का उदय हाल के दिनों में नरेन्द्र मोदी की देन है, जब लोक सभा चुनाव प्रचार के दौरान उन्होंने कई रैलियों में ‘पिंक रिवोल्यूशन’ का मुद्दा उठाया। ज़्यादा विस्तार में ना जाते हुए दो-तीन बातों का ज़िक्र करना ज़रूरी है। पहली, भारत गोमांस का निर्यात नहीं करता। दूसरी, बीफ़ की अंतरराष्ट्रीय श्रेणी में गाय के अलावा भैंसे का भी मांस आता है और साल भर पहले तक भारत बीफ़ (यानी भैंसे का मांस) निर्यात में दूसरे नंबर पर था और नरेन्द्र मोदी के प्रधानमंत्री बनने के बाद नंबर वन बन गया। तीसरी, देश के कई राज्यों में गोमांस खाना बूचड़खानों में गाय काटना भी क़ानूनी है और जम्मू-कश्मीर और महाराष्ट्र के अलावा किसी भी राज्य में बीजेपी सरकार ने इस पर पाबंदी लगाने की कोई कोशिश नहीं की।
इन तमाम तथ्यों का बिहार से सीधे तौर पर लेना-देना नहीं है, लेकिन चुनावी बयार में बीफ़ को लेकर चुनिंदा तथ्यों को जिस तरह राजनेता पेश कर रहे हैं उसमें इस लिहाज से ये ज़रूरी है कि अचानक राजनीति में बीफ़ के उदय को मतदाता किस तरह देखें। बिहार अगले एक महीने तक ऐसे कई मुद्दों से होकर गुजरेगा जो वहां के स्थानीय लोगों के लिए कतई मुद्दा नहीं है। ऐसे आसमानी मुद्दे कई दफ़ा वास्तविक मुद्दों को पीछे धकेलने में क़ामयाब हो जाती है। लिहाजा इस क़ामयाबी को असफ़ल करने का पूरा दारोमदार उस समूह पर है, जिसे लोकतंत्र में मतदाता के नाम से बुलाया जाता है।
जो बिहार मानव विकास सूचकांक पर निचले पायदानों पर लगातार अपनी मौजूदगी दर्ज करता रहा है, उसके लिए बीफ़ मतदान का बड़ा मुद्दा नहीं हो सकता। लेकिन, दादरी में बीजेपी कार्यकर्ताओं द्वारा अंजाम दी गई घटना को बिहार में राजनीतिक बढ़त के लिए इस्तेमाल करने की पूरी कोशिश इसी दिशा में आगे बढ़ती दिख रही है। इस मामले के बाद बीफ़ को लेकर सच्चाई बयान करने का जोखिम भी विपक्ष नहीं उठा सकता, क्योंकि अगर ये मुद्दा लंबा खिंचा तो सबसे ज़्यादा फ़ायदा बीजेपी को होगा। तो, बिहार में जातीय पहचान को ओवरलैप करने की दो कोशिशों (बिहारी उपराष्ट्रवाद के ज़रिए और धार्मिक पहचान के ज़रिए) का अंजाम क्या होना है? क्या विकास की बात करने वाली तमाम पार्टियां हमेशा इस फिराक में रहती हैं कि विकास को आगे कर जनता की संवेदनशील नस को किन मुद्दों के ज़रिए छुएं? चुनाव के बीच में दशहरा और मुहर्रम दोनों होने हैं और बीफ़ जैसे संवेदनशील मुद्दे बिहार की राजनीति को ग़लत दिशा में मोड़ सकते हैं।
फ़िलहाल बिहार के अलावा पूरे देश में जिस तरह की राजनीति इस मसले पर चल रही है उस लिहाज से सभी पार्टियों को समाज के व्यापक हित में इसे बंद कर बिहार की बुनियादी सुविधाओं की बात करनी चाहिए और ये दिखाना चाहिए कि किसके पास बिहार को बेहतर बनाने का अच्छा मॉडल है। एनडीए की मुश्किल ये है कि विकास और तरक्की की बात करेगी तो महंगाई समेत कई मुद्दों पर वो ख़ुद घिर जाएगी क्योंकि केंद्र में वो सत्ता में है और महागठबंधन की मुश्किल ये है कि विकास की बात करते ही बिहार के पिछड़ेपन के लिए नीतीश और पूर्ववर्ती लालू सरकार पर ही प्रश्नचिह्न लग जाएगा।
(ये भी पढ़ें - बीफ़=गोमांस में अफ़वाहों का संचारशास्त्रीय अध्ययन)
 |
| राजनीति की धुरी |
पहले छिटपुट आरोप-प्रत्यारोपों का दौर चला और बाद में जब आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव ने ये बयान दिया कि हिंदुओं का भी एक तबका बीफ़ खाता है तो पूरे मामले ने बिहार में तूल पकड़ लिया। बीजेपी इसी तरह के बयान के फ़िराक में थी और 5 अक्टूबर को राज्य के पूर्व उपमुख्यमंत्री और बीजेपी नेता सुशील कुमार मोदी ने बाक़ायदा इस पर लंबा बयान देकर जनता को ये संदेश दिया कि महागठबंधन के नेता बीफ़ खाने की तरफ़दारी कर रहे हैं। सुशील मोदी ने कहा, “जहां नरेन्द्र मोदी ने बांग्लादेश सीमा पर चौकसी बढ़ाकर हज़ारों गायों को कटने से रोक दिया है, वहीं लालू-नीतीश और सोनिया गांधी गोमांस खाने की बात कर रहे हैं।” हालांकि ना तो सोनिया गांधी और ना ही नीतीश कुमार ने इस पर कोई बयान जारी किया, लेकिन बीजेपी ने समूचे महागठबंधन को इस राजनीति की आंच में एक कड़ाही में बंद कर दिया।
इसके बाद मीडिया ने जब इसको लपका तो लालू प्रसाद यादव को पीछे हटते हुए सफ़ाई देनी पड़ी कि वो पुश्तैनी तौर पर गाय पालते रहे हैं और गोरक्षा को लेकर उन्हें किसी भी तरह के स्पष्टीकरण की दरकार नहीं है क्योंकि नरेन्द्र मोदी और अमित शाह के मुक़ाबले गाय के प्रति उनका प्यार सार्वजनिक है। लालू प्रसाद शायद इस बयान में अपनी जातिगत पृष्ठभूमि को जाहिर करते हुए यादव और पशुपालन के संबंधों को रेखांकित करना चाह रहे थे। हालांकि वो सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायधीश मार्कंडेय काट्जू और सिने अभिनेता ऋषि कपूर के उदाहरण के ज़रिए इस बात पर भी अड़े रहे कि हिंदुओं का एक तबका बीफ़ खाता है और ये देश की हक़ीकत है।
 |
| पशु से मैय्या तक |
अब दो प्रमुख मुद्दे उभरते हैं एक तो बिहार की राजनीति में बीफ़ पॉलिटिक्स की दरकार और दूसरा बीफ़ को लेकर प्रचलित मान्यताओं की हक़ीक़त। बढ़ती महंगाई से लेकर बेरोज़गारी, पलायन और बुनियादी सुविधाओं के अभाव से जूझते बिहार में विकास की बात हर पार्टी कर रही है और हर पार्टी का दावा है कि उनके लिए यही सबसे बड़ा एजेंडा है, लेकिन इन बयानों के समानांतर ये भी साफ़ हो चला है कि पहले के मुक़ाबले कहीं ज़्यादा गहरे स्तर तक ये चुनाव जातिगत और धार्मिक आधार पर लड़ा जा रहा है। महागठबंधन के भीतर जहां आरजेडी मंडल-2 की बात उछालकर सामाजिक न्याय और सोशल इंजीनियरिंग को अपना प्रमुख एजेंडा बनाकर प्रचार कर रही है, वहीं दूसरी तरफ़ उसकी सहयोगी जेडीयू अपने प्रचार में विकास और नीतीश सरकार के काम-काज को रैलियों में तरजीह दे रही है। यानी दोनों पार्टियों ने रणनीतिक तौर पर मतदाताओं के लिए मुद्दे बांट लिए हैं। लालू प्रसाद यादव को तो अगड़े-पिछड़े पर दिए गए एक बयान के बाद चुनाव आयोग ने नोटिस भी भेज दिया।
जातिगत समीकरण के लिहाज से बीजेपी के लिए इस चुनाव को मुफ़ीद नहीं माना जा रहा है, लिहाजा उसके लिए जातिगत अस्मिता को धार्मिक अस्मिता के लबादे से ढंकना फ़ायदे का सौदा है। बीफ़ एक ऐसा शब्द है जो राजनीतिक तौर पर हिंदू पहचान को समेटने की कोशिश में क़ामयाबी देने का माद्दा रखता है। ये अलग बात है कि ऐतिहासिक तौर पर और इस वक़्त भी हिंदुओं का एक तबका बीफ़ खाता ज़रूर है लेकिन राजनीतिक माहौल में बीफ़ को धार्मिक पहचान का मुद्दा मानते हुए वो लकीर के एक तरफ़ खड़ा हो सकता है।
इस पूरे मामले में ग़ौरतलब बात ये है कि बिहार में जातीय पहचान को दरकिनार करने की दो कोशिशें हुईं और दोनों बीजेपी के चलते। एक कोशिश बीफ़ की और दूसरी बिहारी उपराष्ट्रवाद की। नरेन्द्र मोदी ने बिहार में मुज़फ़्फ़रपुर की पहली चुनावी रैली में जब नीतीश कुमार को लेकर डीएनए वाला बयान दिया तो महागठबंधन ने इसे 180 डिग्री मोड़ते हुए बिहारी अस्मिता पर चोट करार दिया। डीएनए जांच करने के लिए कैंप लगाने की राजनीतिक नौटंकी हुई और मामला कुल ऐसा बना कि बिहारी नाम की कोई एक पहचान बिहार के भीतर रह रहा है जिसको अपमानित किया गया। शैवाल गुप्ता ने इसे बिहार के सुसुप्त राष्ट्रवाद को उछालने का मामला बताया। यानी, जिस तरह तमिलनाडु में तमिल अस्मिता, पश्चिम बंगाल में बांग्ला अस्मिता भारतीय राष्ट्रवाद के समानांतर चलती रहती है उस तर्ज पर उत्तर भारत में कभी भी उपराष्ट्रवाद सतह पर नज़र नहीं आया।
डीएनए और स्पेशल पैकेज देने के वक़्त नरेन्द्र मोदी की भंगिमा को जिस तरह महागठबंधन ने बिहारी अस्मिता से जोड़ा वो इस चुनाव में पहली बार बिहारियों को एक ठोस आइडेंटिटी के नीचे खड़ा कर दिया। दूसरी तरफ़ बीजेपी ने बीफ़ को हिंदू अस्मिता के साथ जोड़ते हुए जातीय पहचान को पाटने की कोशिश की। बड़ा सवाल तो ये है कि दोनों गठबंधनों के बीच जिस चुनाव को सीधा मुक़ाबला माना जा रहा है, क्या उसमें जातियों के चक्रव्यूह को भेदने की कोशिश में दोनों आश्वस्त नहीं है?
तीसरा मामला ये है कि बीफ़ को लेकर जिस तरह की अफ़वाह दादरी से लेकर बिहार के मैदान तक फैलाई गई, उसकी सच्चाई क्या है? राजनीतिक बिसात पर बीफ़ का उदय हाल के दिनों में नरेन्द्र मोदी की देन है, जब लोक सभा चुनाव प्रचार के दौरान उन्होंने कई रैलियों में ‘पिंक रिवोल्यूशन’ का मुद्दा उठाया। ज़्यादा विस्तार में ना जाते हुए दो-तीन बातों का ज़िक्र करना ज़रूरी है। पहली, भारत गोमांस का निर्यात नहीं करता। दूसरी, बीफ़ की अंतरराष्ट्रीय श्रेणी में गाय के अलावा भैंसे का भी मांस आता है और साल भर पहले तक भारत बीफ़ (यानी भैंसे का मांस) निर्यात में दूसरे नंबर पर था और नरेन्द्र मोदी के प्रधानमंत्री बनने के बाद नंबर वन बन गया। तीसरी, देश के कई राज्यों में गोमांस खाना बूचड़खानों में गाय काटना भी क़ानूनी है और जम्मू-कश्मीर और महाराष्ट्र के अलावा किसी भी राज्य में बीजेपी सरकार ने इस पर पाबंदी लगाने की कोई कोशिश नहीं की।
 |
| बिहार में गाय की राजनीति को हवा |
जो बिहार मानव विकास सूचकांक पर निचले पायदानों पर लगातार अपनी मौजूदगी दर्ज करता रहा है, उसके लिए बीफ़ मतदान का बड़ा मुद्दा नहीं हो सकता। लेकिन, दादरी में बीजेपी कार्यकर्ताओं द्वारा अंजाम दी गई घटना को बिहार में राजनीतिक बढ़त के लिए इस्तेमाल करने की पूरी कोशिश इसी दिशा में आगे बढ़ती दिख रही है। इस मामले के बाद बीफ़ को लेकर सच्चाई बयान करने का जोखिम भी विपक्ष नहीं उठा सकता, क्योंकि अगर ये मुद्दा लंबा खिंचा तो सबसे ज़्यादा फ़ायदा बीजेपी को होगा। तो, बिहार में जातीय पहचान को ओवरलैप करने की दो कोशिशों (बिहारी उपराष्ट्रवाद के ज़रिए और धार्मिक पहचान के ज़रिए) का अंजाम क्या होना है? क्या विकास की बात करने वाली तमाम पार्टियां हमेशा इस फिराक में रहती हैं कि विकास को आगे कर जनता की संवेदनशील नस को किन मुद्दों के ज़रिए छुएं? चुनाव के बीच में दशहरा और मुहर्रम दोनों होने हैं और बीफ़ जैसे संवेदनशील मुद्दे बिहार की राजनीति को ग़लत दिशा में मोड़ सकते हैं।
फ़िलहाल बिहार के अलावा पूरे देश में जिस तरह की राजनीति इस मसले पर चल रही है उस लिहाज से सभी पार्टियों को समाज के व्यापक हित में इसे बंद कर बिहार की बुनियादी सुविधाओं की बात करनी चाहिए और ये दिखाना चाहिए कि किसके पास बिहार को बेहतर बनाने का अच्छा मॉडल है। एनडीए की मुश्किल ये है कि विकास और तरक्की की बात करेगी तो महंगाई समेत कई मुद्दों पर वो ख़ुद घिर जाएगी क्योंकि केंद्र में वो सत्ता में है और महागठबंधन की मुश्किल ये है कि विकास की बात करते ही बिहार के पिछड़ेपन के लिए नीतीश और पूर्ववर्ती लालू सरकार पर ही प्रश्नचिह्न लग जाएगा।
(ये भी पढ़ें - बीफ़=गोमांस में अफ़वाहों का संचारशास्त्रीय अध्ययन)